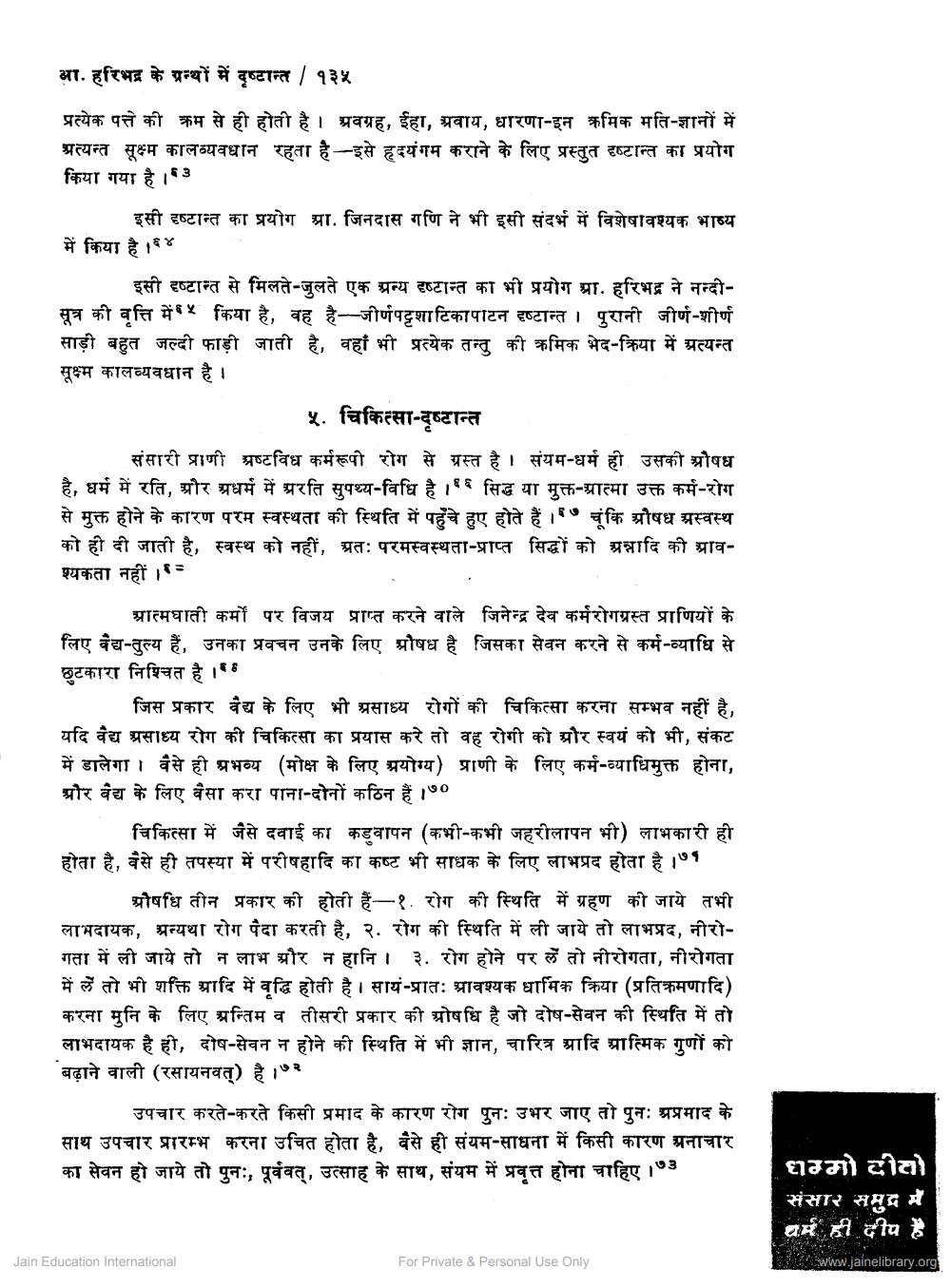Book Title: Haribhadra ke Grantho me Drushtant va Nyaya Author(s): Damodar Shastri Publisher: Z_Umravkunvarji_Diksha_Swarna_Jayanti_Smruti_Granth_012035.pdf View full book textPage 8
________________ आ. हरिभद्र के ग्रन्थों में दृष्टान्त / १३५ प्रत्येक पत्ते की क्रम से ही होती है। प्रवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा-इन क्रमिक मति-ज्ञानों में अत्यन्त सूक्ष्म कालव्यवधान रहता है-इसे हृदयंगम कराने के लिए प्रस्तुत दृष्टान्त का प्रयोग किया गया है। इसी दृष्टान्त का प्रयोग प्रा. जिनदास गणि ने भी इसी संदर्भ में विशेषावश्यक भाष्य में किया है।६४ इसी दृष्टान्त से मिलते-जुलते एक अन्य दृष्टान्त का भी प्रयोग प्रा. हरिभद्र ने नन्दीसूत्र की वृत्ति में ५ किया है, वह है-जीर्णपट्टशाटिकापाटन दृष्टान्त । पुरानी जीर्ण-शीर्ण साड़ी बहुत जल्दी फाड़ी जाती है, वहाँ भी प्रत्येक तन्तु की क्रमिक भेद-क्रिया में अत्यन्त सूक्ष्म कालव्यवधान है। ५. चिकित्सा-दृष्टान्त संसारी प्राणी अष्टविध कर्मरूपी रोग से ग्रस्त है। संयम-धर्म ही उसकी औषध है, धर्म में रति, और अधर्म में परति सुपथ्य-विधि है । ६६ सिद्ध या मुक्त-आत्मा उक्त कर्म-रोग से मुक्त होने के कारण परम स्वस्थता की स्थिति में पहुंचे हुए होते हैं। चूंकि औषध अस्वस्थ को ही दी जाती है, स्वस्थ को नहीं, अतः परमस्वस्थता-प्राप्त सिद्धों को अन्नादि की पावश्यकता नहीं। आत्मघाती कर्मों पर विजय प्राप्त करने वाले जिनेन्द्र देव कर्मरोगग्रस्त प्राणियों के लिए वैद्य-तुल्य हैं, उनका प्रवचन उनके लिए प्रौषध है जिसका सेवन करने से कर्म-व्याधि से छुटकारा निश्चित है।" जिस प्रकार वैद्य के लिए भी असाध्य रोगों की चिकित्सा करना सम्भव नहीं है, यदि वैद्य असाध्य रोग की चिकित्सा का प्रयास करे तो वह रोगी को और स्वयं को भी, संकट में डालेगा। वैसे ही प्रभव्य (मोक्ष के लिए अयोग्य) प्राणी के लिए कर्म-व्याधिमुक्त होना, और वैद्य के लिए वैसा करा पाना-दोनों कठिन हैं।७० चिकित्सा में जैसे दवाई का कड़वापन (कभी-कभी जहरीलापन भी) लाभकारी ही होता है, वैसे ही तपस्या में परीषहादि का कष्ट भी साधक के लिए लाभप्रद होता है।" औषधि तीन प्रकार की होती हैं-१. रोग की स्थिति में ग्रहण की जाये तभी लाभदायक, अन्यथा रोग पैदा करती है, २. रोग की स्थिति में ली जाये तो लाभप्रद, नीरोगता में ली जाये तो न लाभ और न हानि। ३. रोग होने पर लें तो नीरोगता, नीरोगता में लें तो भी शक्ति आदि में वृद्धि होती है। सायं-प्रातः आवश्यक धार्मिक क्रिया (प्रतिक्रमणादि) करना मुनि के लिए अन्तिम व तीसरी प्रकार की ओषधि है जो दोष-सेवन की स्थिति में तो लाभदायक है ही, दोष-सेवन न होने की स्थिति में भी ज्ञान, चारित्र आदि आत्मिक गुणों को बढ़ाने वाली (रसायनवत्) है। उपचार करते-करते किसी प्रमाद के कारण रोग पुनः उभर जाए तो पुनः अप्रमाद के साथ उपचार प्रारम्भ करना उचित होता है, वैसे ही संयम-साधना में किसी कारण अनाचार का सेवन हो जाये तो पुनः, पूर्ववत्, उत्साह के साथ, संयम में प्रवृत्त होना चाहिए।७३ धम्मो दीयो संसार समुद्र में धर्म ही दीय है www.jainelibrary.org. Jain Education International For Private & Personal Use OnlyPage Navigation
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15