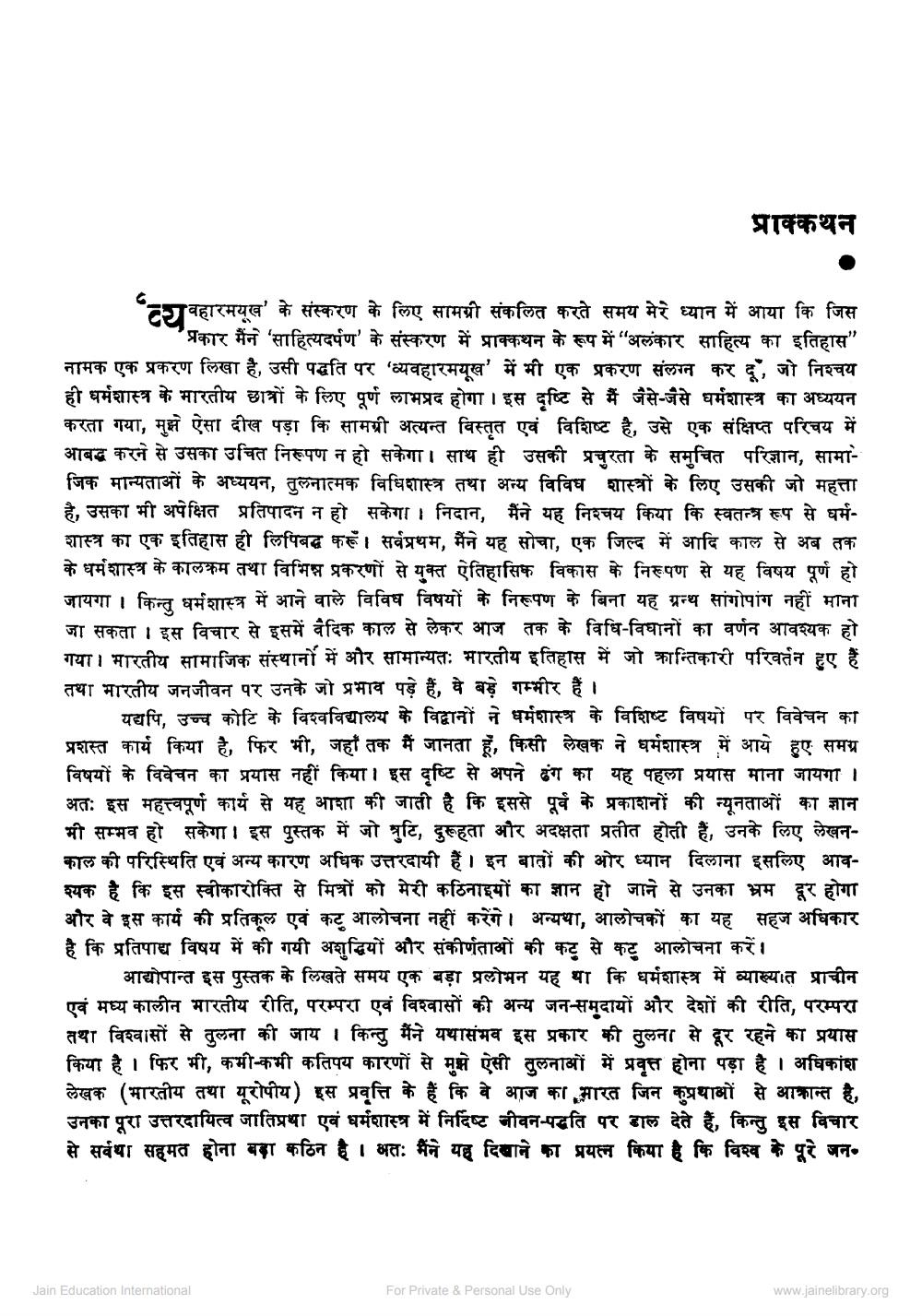Book Title: Dharmshastra ka Itihas Part 5 Author(s): Pandurang V Kane Publisher: Hindi Bhavan Lakhnou View full book textPage 6
________________ 'व्यवहारमयूख' के संस्करण के लिए सामग्री संकलित करते समय मेरे ध्यान में आया कि जिस 'प्रकार मैंने 'साहित्यदर्पण' के संस्करण में प्राक्कथन के रूप में "अलंकार साहित्य का इतिहास" नामक एक प्रकरण लिखा है, उसी पद्धति पर 'व्यवहारमयूख' में भी एक प्रकरण संलग्न कर दूँ, जो निश्चय ही धर्मशास्त्र के भारतीय छात्रों के लिए पूर्ण लाभप्रद होगा । इस दृष्टि से मैं जैसे-जैसे धर्मशास्त्र का अध्ययन करता गया, मुझे ऐसा दीख पड़ा कि सामग्री अत्यन्त विस्तृत एवं विशिष्ट है, उसे एक संक्षिप्त परिचय में आबद्ध करने से उसका उचित निरूपण न हो सकेगा । साथ ही उसकी प्रचुरता के समुचित परिज्ञान, सामाजिक मान्यताओं के अध्ययन, तुलनात्मक विधिशास्त्र तथा अन्य विविध शास्त्रों के लिए उसकी जो महत्ता है, उसका भी अपेक्षित प्रतिपादन न हो सकेगा । निदान, मैंने यह निश्चय किया कि स्वतन्त्र रूप से धर्मशास्त्र का एक इतिहास ही लिपिबद्ध करूँ । सर्वप्रथम, मैंने यह सोचा, एक जिल्द में आदि काल से अब तक के धर्मशास्त्र के कालक्रम तथा विभिन्न प्रकरणों से युक्त ऐतिहासिक विकास के निरूपण से यह विषय पूर्ण हो जायगा । किन्तु धर्मशास्त्र में आने वाले विविध विषयों के निरूपण के बिना यह ग्रन्थ सांगोपांग नहीं माना जा सकता । इस विचार से इसमें वैदिक काल से लेकर आज तक के विधि-विधानों का वर्णन आवश्यक हो गया। भारतीय सामाजिक संस्थानों में और सामान्यतः भारतीय इतिहास में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं तथा भारतीय जनजीवन पर उनके जो प्रभाव पड़े हैं, वे बड़े गम्भीर I यद्यपि, उच्च कोटि के विश्वविद्यालय के विद्वानों ने धर्मशास्त्र के विशिष्ट विषयों पर विवेचन का प्रशस्त कार्य किया है, फिर भी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसी लेखक ने धर्मशास्त्र आये हुए समग्र विषयों के विवेचन का प्रयास नहीं किया। इस दृष्टि से अपने ढंग का यह पहला प्रयास माना जायगा । अतः इस महत्त्वपूर्ण कार्य से यह आशा की जाती है कि इससे पूर्व के प्रकाशनों की न्यूनताओं का ज्ञान भी सम्भव हो सकेगा। इस पुस्तक में जो त्रुटि, दुरूहता और अदक्षता प्रतीत होती हैं, उनके लिए लेखनकाल की परिस्थिति एवं अन्य कारण अधिक उत्तरदायी हैं। इन बातों की ओर ध्यान दिलाना इसलिए आवश्यक है कि इस स्वीकारोक्ति से मित्रों को मेरी कठिनाइयों का ज्ञान हो जाने से उनका भ्रम दूर होगा और वे इस कार्य की प्रतिकूल एवं कटु आलोचना नहीं करेंगे । अन्यथा, आलोचकों का यह सहज अधिकार है कि प्रतिपाद्य विषय में की गयी अशुद्धियों और संकीर्णताओं की कटु से कटु आलोचना करें । आद्योपान्त इस पुस्तक के लिखते समय एक बड़ा प्रलोभन यह था कि धर्मशास्त्र में व्याख्यात प्राचीन एवं मध्य कालीन भारतीय रीति, परम्परा एवं विश्वासों की अन्य जन समुदायों और देशों की रीति, परम्परा तथा विश्वासों से तुलना की जाय । किन्तु मैंने यथासंभव इस प्रकार की तुलना से दूर रहने का प्रयास किया है । फिर भी, कभी-कभी कतिपय कारणों से मुझे ऐसी तुलनाओं में प्रवृत्त होना पड़ा है । अधिकांश लेखक ( भारतीय तथा यूरोपीय ) इस प्रवृत्ति के हैं कि वे आज का भारत जिन कुप्रथाओं से आक्रान्त है, उनका पूरा उत्तरदायित्व जातिप्रथा एवं धर्मशास्त्र में निर्दिष्ट जीवन-पद्धति पर डाल देते हैं, किन्तु इस विचार से सर्वथा सहमत होना बड़ा कठिन है । अतः मैंने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि विश्व के पूरे जन• Jain Education International प्राक्कथन For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 452