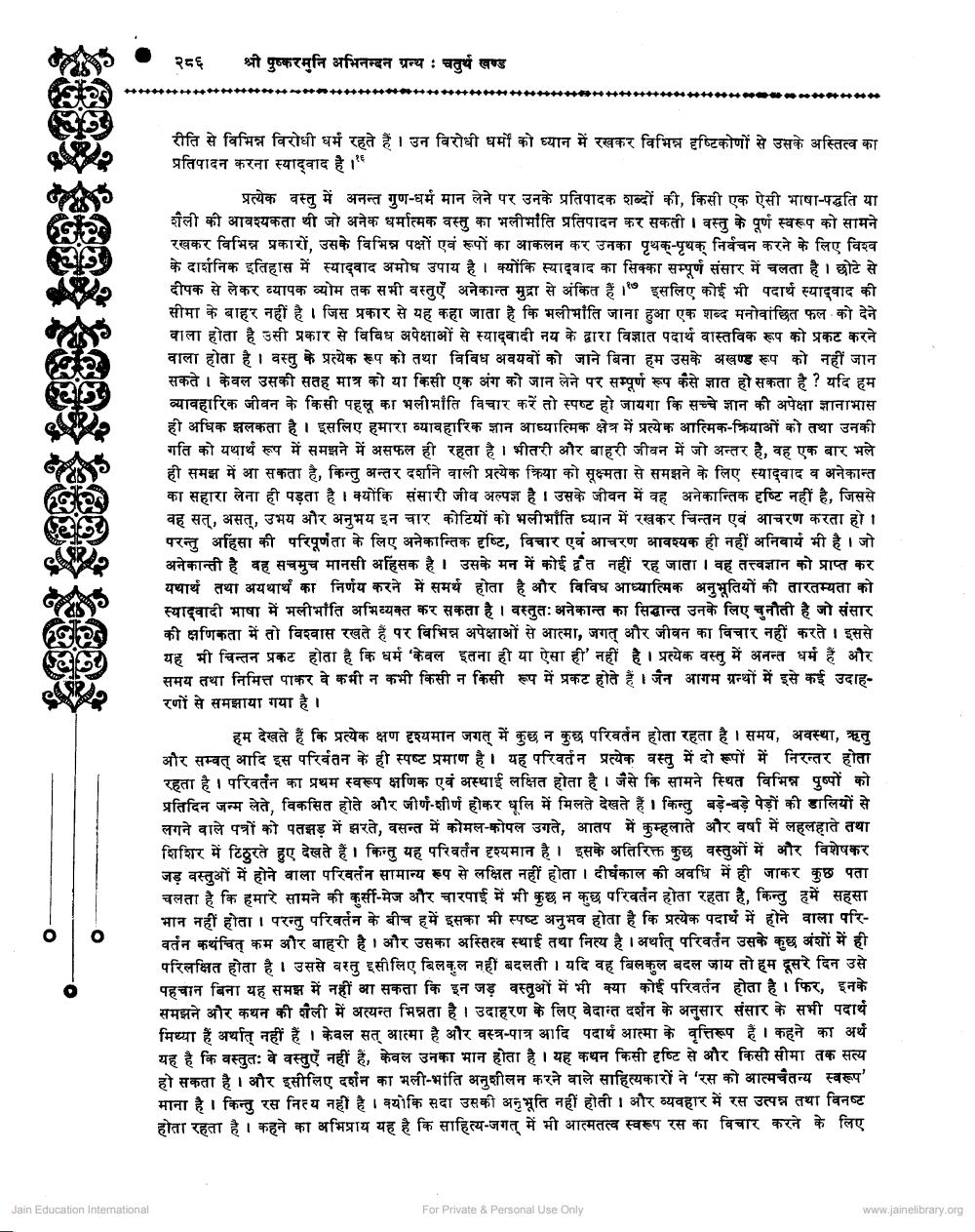Book Title: Bhartiya Darshanik Parampara aur Syadwad Author(s): Devendra Kumar Jain Publisher: Z_Pushkarmuni_Abhinandan_Granth_012012.pdf View full book textPage 4
________________ २८६ श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ : चतुर्थ खण्ड -rrrrrrrrrrrrrrr--immmmmmmmmmmmm.------------ रीति से विभिन्न विरोधी धर्म रहते हैं। उन विरोधी धर्मों को ध्यान में रखकर विभिन्न दृष्टिकोणों से उसके अस्तित्व का प्रतिपादन करना स्याद्वाद है।६ प्रत्येक वस्तु में अनन्त गुण-धर्म मान लेने पर उनके प्रतिपादक शब्दों की, किसी एक ऐसी भाषा-पद्धति या शैली की आवश्यकता थी जो अनेक धर्मात्मक वस्तु का भलीभांति प्रतिपादन कर सकती । वस्तु के पूर्ण स्वरूप को सामने रखकर विभिन्न प्रकारों, उसके विभिन्न पक्षों एवं रूपों का आकलन कर उनका पृथक्-पृथक् निर्वचन करने के लिए विश्व के दार्शनिक इतिहास में स्याद्वाद अमोघ उपाय है । क्योंकि स्यावाद का सिक्का सम्पूर्ण संसार में चलता है। छोटे से दीपक से लेकर व्यापक व्योम तक सभी वस्तुएँ अनेकान्त मुद्रा से अंकित हैं। इसलिए कोई भी पदार्थ स्याद्वाद की सीमा के बाहर नहीं है । जिस प्रकार से यह कहा जाता है कि भलीभांति जाना हुआ एक शब्द मनोवांछित फल को देने वाला होता है उसी प्रकार से विविध अपेक्षाओं से स्याद्वादी नय के द्वारा विज्ञात पदार्थ वास्तविक रूप को प्रकट करने वाला होता है । वस्तु के प्रत्येक रूप को तथा विविध अवयवों को जाने बिना हम उसके अखण्ड रूप को नहीं जान सकते। केवल उसकी सतह मात्र को या किसी एक अंग को जान लेने पर सम्पूर्ण रूप कसे ज्ञात हो सकता है ? यदि हम व्यावहारिक जीवन के किसी पहलू का भलीभाँति विचार करें तो स्पष्ट हो जायगा कि सच्चे ज्ञान की अपेक्षा ज्ञानाभास ही अधिक झलकता है। इसलिए हमारा व्यावहारिक ज्ञान आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रत्येक आत्मिक-क्रियाओं को तथा उनकी गति को यथार्थ रूप में समझने में असफल ही रहता है । भीतरी और बाहरी जीवन में जो अन्तर है, वह एक बार भले ही समझ में आ सकता है, किन्तु अन्तर दर्शाने वाली प्रत्येक क्रिया को सूक्ष्मता से समझने के लिए स्याद्वाद व अनेकान्त का सहारा लेना ही पड़ता है । क्योंकि संसारी जीव अल्पज्ञ है । उसके जीवन में वह अनेकान्तिक दृष्टि नहीं है, जिससे वह सत्, असत्, उभय और अनुभय इन चार कोटियों को भलीभाँति ध्यान में रखकर चिन्तन एवं आचरण करता हो। परन्तु अहिंसा की परिपूर्णता के लिए अनेकान्तिक दृष्टि, विचार एवं आचरण आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है । जो अनेकान्ती है वह सचमुच मानसी अहिंसक है। उसके मन में कोई दंत नहीं रह जाता । वह तत्त्वज्ञान को प्राप्त कर यथार्थ तथा अयथार्थ का निर्णय करने में समर्थ होता है और विविध आध्यात्मिक अनुभूतियों की तारतम्यता को स्याद्वादी भाषा में भलीभांति अभिव्यक्त कर सकता है । वस्तुतः अनेकान्त का सिद्धान्त उनके लिए चुनौती है जो संसार की क्षणिकता में तो विश्वास रखते हैं पर विभिन्न अपेक्षाओं से आत्मा, जगत् और जीवन का विचार नहीं करते । इससे यह भी चिन्तन प्रकट होता है कि धर्म 'केवल इतना ही या ऐसा ही नहीं है। प्रत्येक वस्तु में अनन्त धर्म हैं और समय तथा निमित्त पाकर वे कभी न कभी किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। जैन आगम ग्रन्थों में इसे कई उदाहरणों से समझाया गया है। हम देखते हैं कि प्रत्येक क्षण दृश्यमान जगत् में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है । समय, अवस्था, ऋतु और सम्वत् आदि इस परिर्वतन के ही स्पष्ट प्रमाण है। यह परिवर्तन प्रत्येक वस्तु में दो रूपों में निरन्तर होता रहता है । परिवर्तन का प्रथम स्वरूप क्षणिक एवं अस्थाई लक्षित होता है । जैसे कि सामने स्थित विभिन्न पुष्पों को प्रतिदिन जन्म लेते, विकसित होते और जीर्ण-शीर्ण होकर धूलि में मिलते देखते हैं। किन्तु बड़े-बड़े पेड़ों की डालियों से लगने वाले पत्रों को पतझड़ में झरते, वसन्त में कोमल-कोपल उगते, आतप में कुम्हलाते और वर्षा में लहलहाते तथा शिशिर में टिठुरते हुए देखते हैं। किन्तु यह परिवर्तन दृश्यमान है। इसके अतिरिक्त कुछ वस्तुओं में और विशेषकर जड़ वस्तुओं में होने वाला परिवर्तन सामान्य रूप से लक्षित नहीं होता । दीर्घकाल की अवधि में ही जाकर कुछ पता चलता है कि हमारे सामने की कुर्सी-मेज और चारपाई में भी कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, किन्तु हमें सहसा भान नहीं होता। परन्तु परिवर्तन के बीच हमें इसका भी स्पष्ट अनुभव होता है कि प्रत्येक पदार्थ में होने वाला परिवर्तन कथंचित् कम और बाहरी है । और उसका अस्तित्व स्थाई तथा नित्य है । अर्थात् परिवर्तन उसके कुछ अंशों में ही परिलक्षित होता है। उससे वस्तु इसीलिए बिलकुल नहीं बदलती। यदि वह बिलकुल बदल जाय तो हम दूसरे दिन उसे पहचान बिना यह समझ में नहीं आ सकता कि इन जड़ वस्तुओं में भी क्या कोई परिवर्तन होता है । फिर, इनके समझने और कथन की शैली में अत्यन्त भिन्नता है। उदाहरण के लिए वेदान्त दर्शन के अनुसार संसार के सभी पदार्थ मिथ्या हैं अर्थात् नहीं हैं । केवल सत् आत्मा है और वस्त्र-पात्र आदि पदार्थ आत्मा के वृत्तिरूप हैं । कहने का अर्थ यह है कि वस्तुत: वे वस्तुएँ नहीं हैं, केवल उनका भान होता है । यह कथन किसी दृष्टि से और किसी सीमा तक सत्य हो सकता है। और इसीलिए दर्शन का भली-भांति अनुशीलन करने वाले साहित्यकारों ने 'रस को आत्मचैतन्य स्वरूप' माना है। किन्तु रस नित्य नहीं है । क्योकि सदा उसकी अनुभूति नहीं होती। और व्यवहार में रस उत्पन्न तथा विनष्ट होता रहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि साहित्य-जगत् में भी आत्मतत्व स्वरूप रस का विचार करने के लिए Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7