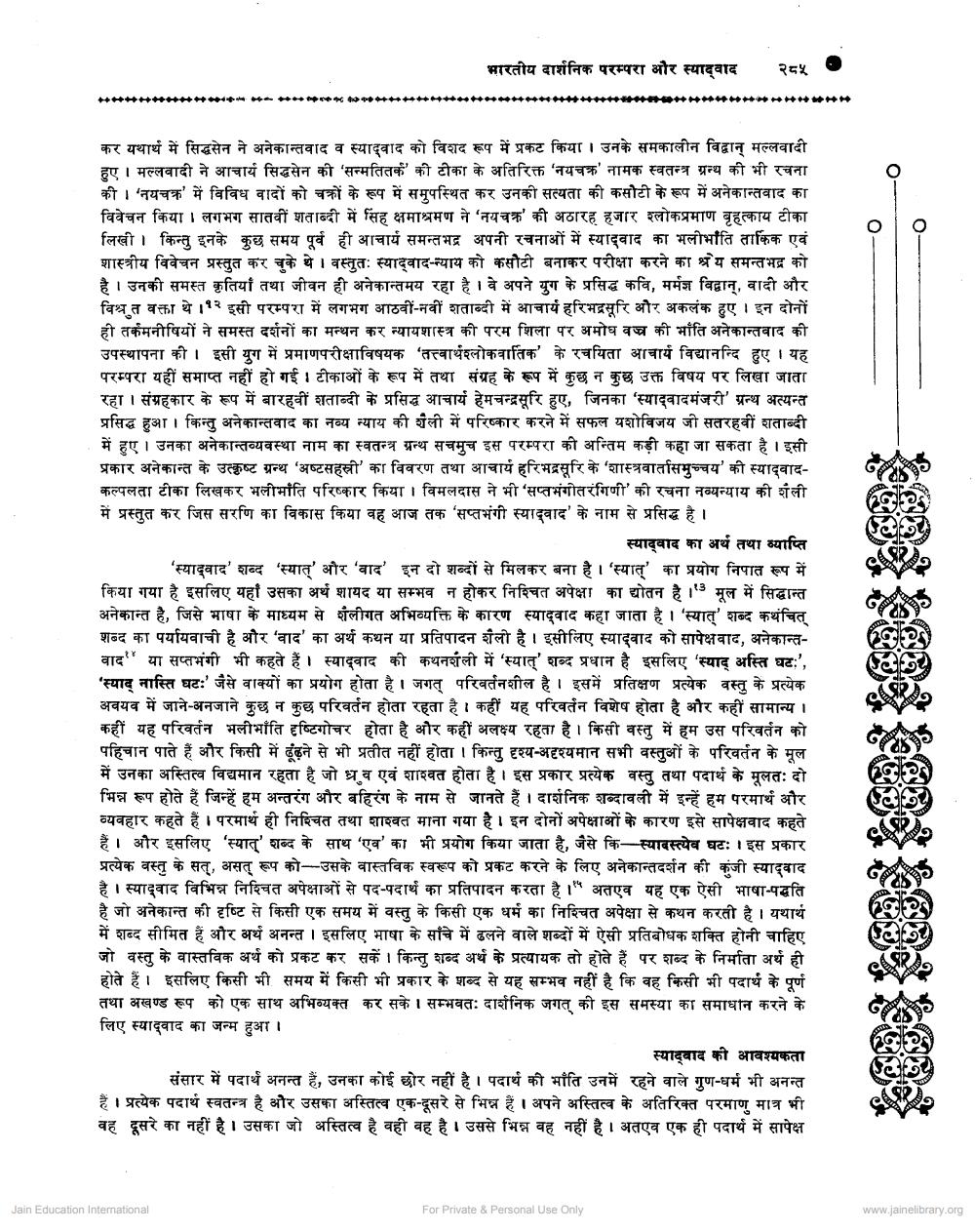Book Title: Bhartiya Darshanik Parampara aur Syadwad Author(s): Devendra Kumar Jain Publisher: Z_Pushkarmuni_Abhinandan_Granth_012012.pdf View full book textPage 3
________________ भारतीय दार्शनिक परम्परा और स्याद्वाद २८५ कर यथार्थ में सिद्धसेन ने अनेकान्तवाद व स्याद्वाद को विशद रूप में प्रकट किया। उनके समकालीन विद्वान् मल्लवादी हुए । मल्लवादी ने आचार्य सिद्धसेन की 'सन्मतितर्क' की टीका के अतिरिक्त 'नयचक्र' नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ की भी रचना की । 'नयचक्र' में विविध वादों को चक्रों के रूप में समुपस्थित कर उनकी सत्यता की कसौटी के रूप में अनेकान्तवाद का विवेचन किया । लगभग सातवीं शताब्दी में सिंह क्षमाश्रमण ने 'नयचक्र' की अठारह हजार श्लोकप्रमाण बृहत्काय टीका लिखी । किन्तु इनके कुछ समय पूर्व ही आचार्य समन्तभद्र अपनी रचनाओं में स्याद्वाद का भलीभाँति तार्किक एवं शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत कर चुके थे । वस्तुतः स्याद्वाद - न्याय को कसौटी बनाकर परीक्षा करने का श्र ेय समन्तभद्र को है । उनकी समस्त कृतियाँ तथा जीवन ही अनेकान्तमय रहा है । वे अपने युग के प्रसिद्ध कवि, मर्मज्ञ विद्वान्, वादी और विश्रुत वक्ता थे ।१२ इसी परम्परा में लगभग आठवीं-नवीं शताब्दी में आचार्य हरिभद्रसूरि और अकलंक हुए । इन दोनों ही तर्कमनीषियों ने समस्त दर्शनों का मन्थन कर न्यायशास्त्र की परम शिला पर अमोघ वस्त्र की भाँति अनेकान्तवाद की उपस्थापना की । इसी युग में प्रमाणपरीक्षाविषयक तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक' के रचयिता आचार्य विद्यानन्दि हुए । यह परम्परा यहीं समाप्त नहीं हो गई। टीकाओं के रूप में तथा संग्रह के रूप में कुछ न कुछ उक्त विषय पर लिखा जाता रहा । संग्रहकार के रूप में बारहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध आचार्य हेमचन्द्रसूरि हुए, जिनका 'स्याद्वादमंजरी' ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ । किन्तु अनेकान्तवाद का नव्य न्याय की शैली में परिष्कार करने में सफल यशोविजय जी सतरहवीं शताब्दी में हुए । उनका अनेकान्तव्यवस्था नाम का स्वतन्त्र ग्रन्थ सचमुच इस परम्परा की अन्तिम कड़ी कहा जा सकता है । इसी प्रकार अनेकान्त के उत्कृष्ट ग्रन्थ 'अष्टसहस्री' का विवरण तथा आचार्य हरिभद्रसूरि के 'शास्त्रवार्तासमुच्चय' की स्यादवादकल्पलता टीका लिखकर भलीभांति परिष्कार किया । विमलदास ने भी 'सप्तभंगीतरंगिणी' की रचना नव्यन्याय की शैली में प्रस्तुत कर जिस सरणि का विकास किया वह आज तक 'सप्तभंगी स्याद्वाद' के नाम से प्रसिद्ध है । स्याद्वाद का अर्थ तथा व्याप्ति 'स्याद्वाद' शब्द 'स्यात्' और 'वाद' इन दो शब्दों से मिलकर बना है । 'स्यात्' का प्रयोग निपात रूप में किया गया है इसलिए यहाँ उसका अर्थ शायद या सम्भव न होकर निश्चित अपेक्षा का द्योतन है। मूल में सिद्धान्त अनेकान्त है, जिसे भाषा के माध्यम से शैलीगत अभिव्यक्ति के कारण स्याद्वाद कहा जाता है। 'स्यात्' शब्द कथंचित् शब्द का पर्यायवाची है और 'वाद' का अर्थ कथन या प्रतिपादन शैली है । इसीलिए स्याद्वाद को सापेक्षवाद, अनेकान्तवाद" या सप्तभंगी भी कहते हैं । स्याद्वाद की कथनशैली में 'स्यात्' शब्द प्रधान है इसलिए 'स्याद् अस्ति घट:', 'स्याद् नास्ति घट:' जैसे वाक्यों का प्रयोग होता है । जगत् परिवर्तनशील है । इसमें प्रतिक्षण प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक अवयव में जाने-अनजाने कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है । कहीं यह परिवर्तन विशेष होता है और कहीं सामान्य । कहीं यह परिवर्तन भलीभाँति दृष्टिगोचर होता है और कहीं अलक्ष्य रहता है। किसी वस्तु में हम उस परिवर्तन को पहिचान पाते हैं और किसी में ढूंढने से भी प्रतीत नहीं होता किन्तु दृश्य-अदृश्यमान सभी वस्तुओंों के परिवर्तन के मूल में उनका अस्तित्व विद्यमान रहता है जो ध्रुव एवं शाश्वत होता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु तथा पदार्थ के मूलतः दो भिन्न रूप होते हैं जिन्हें हम अन्तरंग और बहिरंग के नाम से जानते हैं । दार्शनिक शब्दावली में इन्हें हम परमार्थ और व्यवहार कहते हैं । परमार्थ ही निश्चित तथा शाश्वत माना गया है । इन दोनों अपेक्षाओं के कारण इसे सापेक्षवाद कहते हैं । और इसलिए 'स्यात्' शब्द के साथ 'एव' का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि –—स्यावस्त्येव घटः । इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के सत् असत् रूप को उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने के लिए अनेकान्तदर्शन की कुंजी स्याद्वाद है । स्यादवाद विभिन्न निश्चित अपेक्षाओं से पद-पदार्थ का प्रतिपादन करता है ।" अतएव यह एक ऐसी भाषा-पद्धति है जो अनेकान्त की दृष्टि से किसी एक समय में वस्तु के किसी एक धर्म का निश्चित अपेक्षा से कथन करती है । यथार्थ में शब्द सीमित हैं और अर्थ अनन्त । इसलिए भाषा के सांचे में ढलने वाले शब्दों में ऐसी प्रतिबोधक शक्ति होनी चाहिए जो वस्तु के वास्तविक अर्थ को प्रकट कर सकें । किन्तु शब्द अर्थ के प्रत्यायक तो होते हैं पर शब्द के निर्माता अर्थ ही होते हैं । इसलिए किसी भी समय में किसी भी प्रकार के शब्द से यह सम्भव नहीं है कि वह किसी भी पदार्थ के पूर्ण तथा अखण्ड रूप को एक साथ अभिव्यक्त कर सके । सम्भवतः दार्शनिक जगत् की इस समस्या का समाधान करने के लिए स्याद्वाद का जन्म हुआ । Jain Education International स्याद्वाद की आवश्यकता संसार में पदार्थ अनन्त हैं, उनका कोई छोर नहीं है । पदार्थ की भाँति उनमें रहने वाले गुण-धर्म भी अनन्त हैं । प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र है और उसका अस्तित्व एक-दूसरे से भिन्न हैं । अपने अस्तित्व के अतिरिक्त परमाणु मात्र भी वह दूसरे का नहीं है । उसका जो अस्तित्व है वही वह है । उससे भिन्न वह नहीं है । अतएव एक ही पदार्थ में सापेक्ष For Private & Personal Use Only *+++ www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7