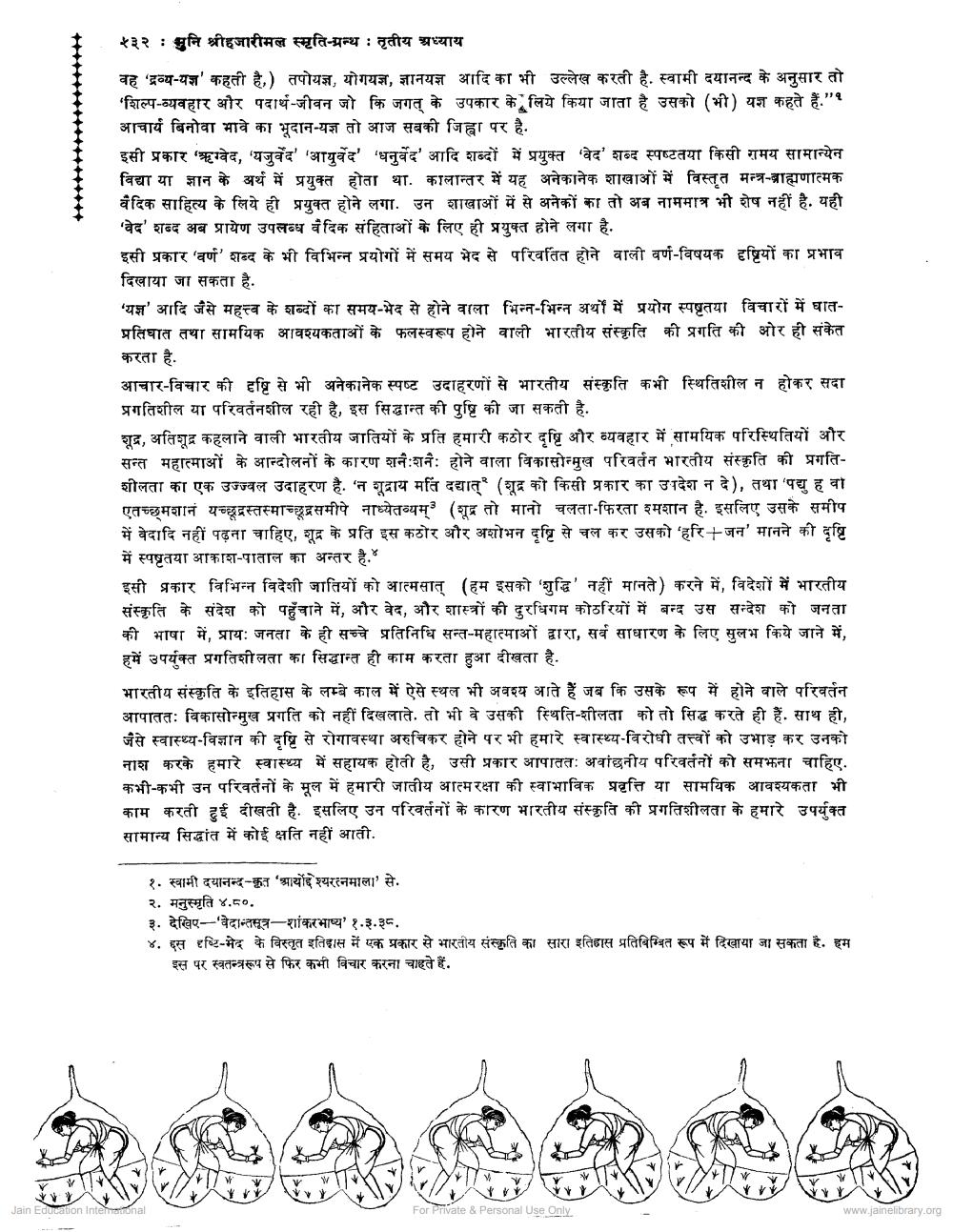Book Title: Bharatiya Sanskruti ka Vastavik Drushtikon Author(s): Mangaldev Shastri Publisher: Z_Hajarimalmuni_Smruti_Granth_012040.pdf View full book textPage 2
________________ ५३२ : मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रन्थ : तृतीय अध्याय वह 'द्रव्य-यज्ञ' कहती है,) तपोयज्ञ, योगयज्ञ, ज्ञानयज्ञ आदि का भी उल्लेख करती है. स्वामी दयानन्द के अनुसार तो 'शिल्प-व्यवहार और पदार्थ-जीवन जो कि जगत् के उपकार के लिये किया जाता है उसको (भी) यज्ञ कहते हैं." आचार्य बिनोवा भावे का भूदान-यज्ञ तो आज सबकी जिह्वा पर है. इसी प्रकार 'ऋग्वेद, यजुर्वेद' 'आयुर्वेद' 'धनुर्वेद' आदि शब्दों में प्रयुक्त 'वेद' शब्द स्पष्टतया किसी समय सामान्येन विद्या या ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होता था. कालान्तर में यह अनेकानेक शाखाओं में विस्तृत मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वैदिक साहित्य के लिये ही प्रयुक्त होने लगा. उन शाखाओं में से अनेकों का तो अब नाममात्र भी शेष नहीं है. यही 'वेद' शब्द अब प्रायेण उपलब्ध वैदिक संहिताओं के लिए ही प्रयुक्त होने लगा है. इसी प्रकार 'वर्ण' शब्द के भी विभिन्न प्रयोगों में समय भेद से परिवर्तित होने वाली वर्ण-विषयक दृष्टियों का प्रभाव दिखाया जा सकता है. 'यज्ञ' आदि जैसे महत्त्व के शब्दों का समय-भेद से होने वाला भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयोग स्पष्टतया विचारों में घातप्रतिघात तथा सामयिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप होने वाली भारतीय संस्कृति की प्रगति की ओर ही संकेत करता है. आचार-विचार की दृष्टि से भी अनेकानेक स्पष्ट उदाहरणों से भारतीय संस्कृति कभी स्थितिशील न होकर सदा प्रगतिशील या परिवर्तनशील रही है, इस सिद्धान्त की पुष्टि की जा सकती है. शूद्र, अतिशूद्र कहलाने वाली भारतीय जातियों के प्रति हमारी कठोर दृष्टि और व्यवहार में सामयिक परिस्थितियों और सन्त महात्माओं के आन्दोलनों के कारण शनैःशनैः होने वाला विकासोन्मुख परिवर्तन भारतीय संस्कृति की प्रगतिशीलता का एक उज्ज्वल उदाहरण है. 'न शूद्राय मतिं दद्यात् (शूद्र को किसी प्रकार का उपदेश न दे), तथा पधु ह वो एतच्छ्मशानं यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतव्यम् (शूद्र तो मानो चलता-फिरता श्मशान है. इसलिए उसके समीप में वेदादि नहीं पढ़ना चाहिए, शूद्र के प्रति इस कठोर और अशोभन दृष्टि से चल कर उसको 'हरिजन' मानने की दृष्टि में स्पष्टतया आकाश-पाताल का अन्तर है.४ इसी प्रकार विभिन्न विदेशी जातियों को आत्मसात् (हम इसको 'शुद्धि' नहीं मानते) करने में, विदेशों में भारतीय संस्कृति के संदेश को पहुँचाने में, और वेद, और शास्त्रों की दुरधिगम कोठरियों में बन्द उस सन्देश को जनता की भाषा में, प्रायः जनता के ही सच्चे प्रतिनिधि सन्त-महात्माओं द्वारा, सर्व साधारण के लिए सुलभ किये जाने में, हमें उपर्युक्त प्रगतिशीलता का सिद्धान्त ही काम करता हुआ दीखता है. भारतीय संस्कृति के इतिहास के लम्बे काल में ऐसे स्थल भी अवश्य आते हैं जब कि उसके रूप में होने वाले परिवर्तन आपाततः विकासोन्मुख प्रगति को नहीं दिखलाते. तो भी वे उसकी स्थिति-शीलता को तो सिद्ध करते ही हैं. साथ ही, जैसे स्वास्थ्य-विज्ञान की दृष्टि से रोगावस्था अरुचिकर होने पर भी हमारे स्वास्थ्य-विरोधी तत्त्वों को उभाड़ कर उनको नाश करके हमारे स्वास्थ्य में सहायक होती है, उसी प्रकार आपाततः अवांछनीय परिवर्तनों को समझना चाहिए. कभी-कभी उन परिवर्तनों के मूल में हमारी जातीय आत्मरक्षा की स्वाभाविक प्रवृत्ति या सामयिक आवश्यकता भी काम करती हुई दीखती है. इसलिए उन परिवर्तनों के कारण भारतीय संस्कृति की प्रगतिशीलता के हमारे उपर्युक्त सामान्य सिद्धांत में कोई क्षति नहीं आती. १. स्वामी दयानन्द-कृत 'आर्योद्देश्यरत्नमाला' से. २. मनुस्मृति ४.८०. ३. देखिए-'वेदान्तसूत्र-शांकरभाष्य' १.३.३८. ४. इस दृष्टि-भेद के विस्तृत इतिहास में एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का सारा इतिहास प्रतिबिम्बित रूप में दिखाया जा सकता है. हम इस पर स्वतन्त्ररूप से फिर कभी विचार करना चाहते हैं. Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8