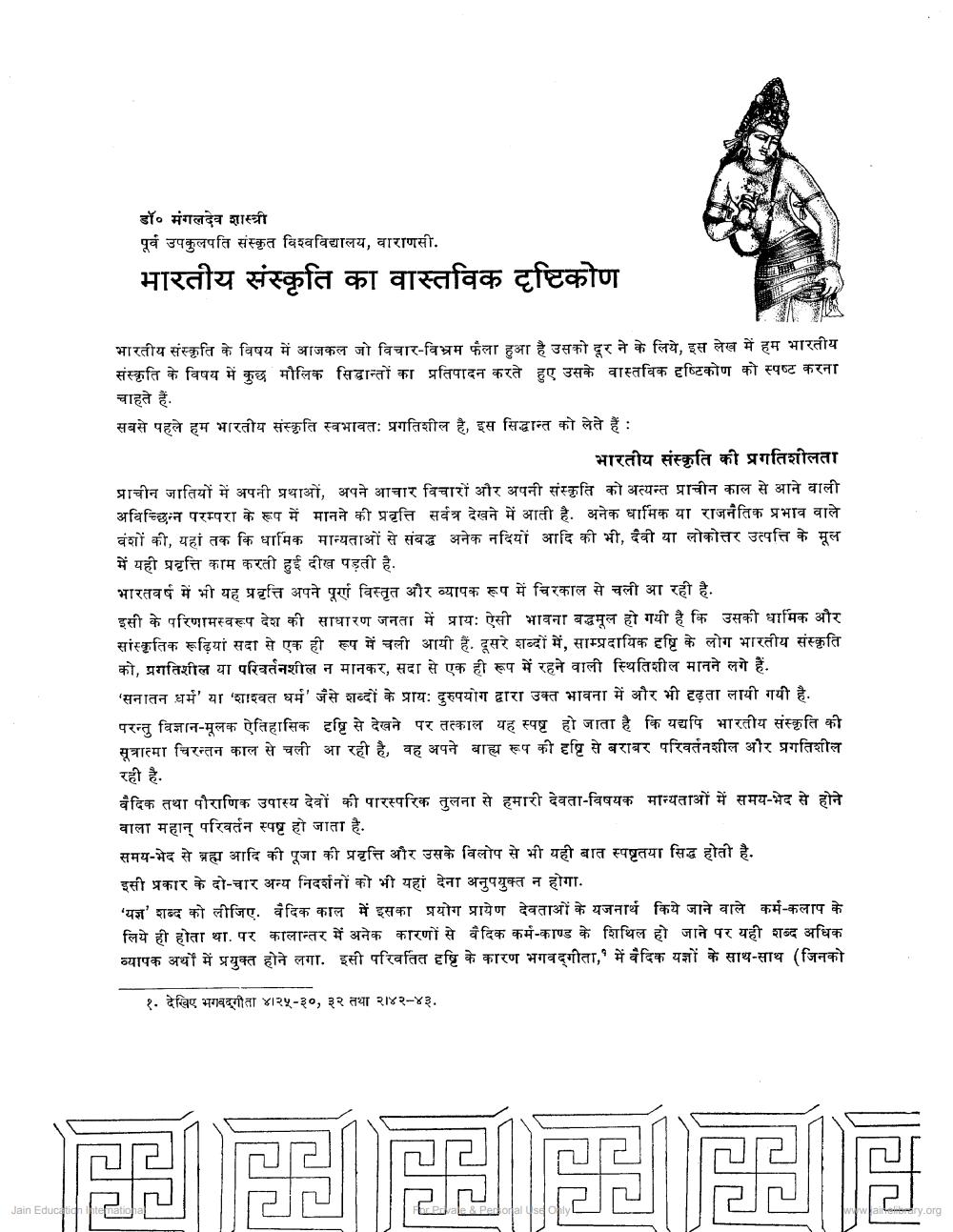Book Title: Bharatiya Sanskruti ka Vastavik Drushtikon Author(s): Mangaldev Shastri Publisher: Z_Hajarimalmuni_Smruti_Granth_012040.pdf View full book textPage 1
________________ डॉ० मंगलदेव शास्त्री पूर्व उपकुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी. भारतीय संस्कृति का वास्तविक दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति के विषय में आजकल जो विचार-विभ्रम फैला हुआ है उसको दूर ने के लिये, इस लेख में हम भारतीय संस्कृति के विषय में कुछ मौलिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए उसके वास्तविक दृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहते हैं. सबसे पहले हम भारतीय संस्कृति स्वभावतः प्रगतिशील है, इस सिद्धान्त को लेते हैं : भारतीय संस्कृति की प्रगतिशीलता प्राचीन जातियों में अपनी प्रथाओं, अपने आचार विचारों और अपनी संस्कृति को अत्यन्त प्राचीन काल से आने वाली अविच्छिन्न परम्परा के रूप में मानने की प्रवृत्ति सर्वत्र देखने में आती है. अनेक धार्मिक या राजनैतिक प्रभाव वाले वंशों की, यहां तक कि धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध अनेक नदियों आदि की भी, दैवी या लोकोत्तर उत्पत्ति के मूल में यही प्रवृत्ति काम करती हुई दीख पड़ती है. भारतवर्ष में भी यह प्रवृत्ति अपने पूर्ण विस्तृत और व्यापक रूप में चिरकाल से चली आ रही है. इसी के परिणामस्वरूप देश की साधारण जनता में प्रायः ऐसी भावना बद्धमूल हो गयी है कि उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक रूढ़ियां सदा से एक ही रूप में चली आयी हैं. दूसरे शब्दों में, साम्प्रदायिक दृष्टि के लोग भारतीय संस्कृति को, प्रगतिशील या परिवर्तनशील न मानकर, सदा से एक ही रूप में रहने वाली स्थितिशील मानने लगे हैं. 'सनातन धर्म' या 'शाश्वत धर्म' जैसे शब्दों के प्रायः दुरुपयोग द्वारा उक्त भावना में और भी दृढ़ता लायी गयी है. परन्तु विज्ञान-मूलक ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर तत्काल यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि भारतीय संस्कृति की सूत्रात्मा चिरन्तन काल से चली आ रही है, वह अपने बाह्य रूप की दृष्टि से बराबर परिवर्तनशील और प्रगतिशील रही है. वैदिक तथा पौराणिक उपास्य देवों की पारस्परिक तुलना से हमारी देवता-विषयक मान्यताओं में समय-भेद से होने वाला महान् परिवर्तन स्पष्ट हो जाता है. समय-भेद से ब्रह्म आदि की पूजा की प्रवृत्ति और उसके विलोप से भी यही बात स्पष्टतया सिद्ध होती है. इसी प्रकार के दो-चार अन्य निदर्शनों को भी यहां देना अनुपयुक्त न होगा. 'यज्ञ' शब्द को लीजिए. वैदिक काल में इसका प्रयोग प्रायेण देवताओं के यजनार्थ किये जाने वाले कर्म-कलाप के लिये ही होता था. पर कालान्तर में अनेक कारणों से वैदिक कर्म-काण्ड के शिथिल हो जाने पर यही शब्द अधिक व्यापक अर्थों में प्रयुक्त होने लगा. इसी परिवर्तित दृष्टि के कारण भगवद्गीता,' में वैदिक यज्ञों के साथ-साथ (जिनको १. देखिए भगवद्गीता ४।२५-३०, ३२ तथा २०४२-४३. Jain Educatie mati ale & Pedofalu Oy emandry.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8