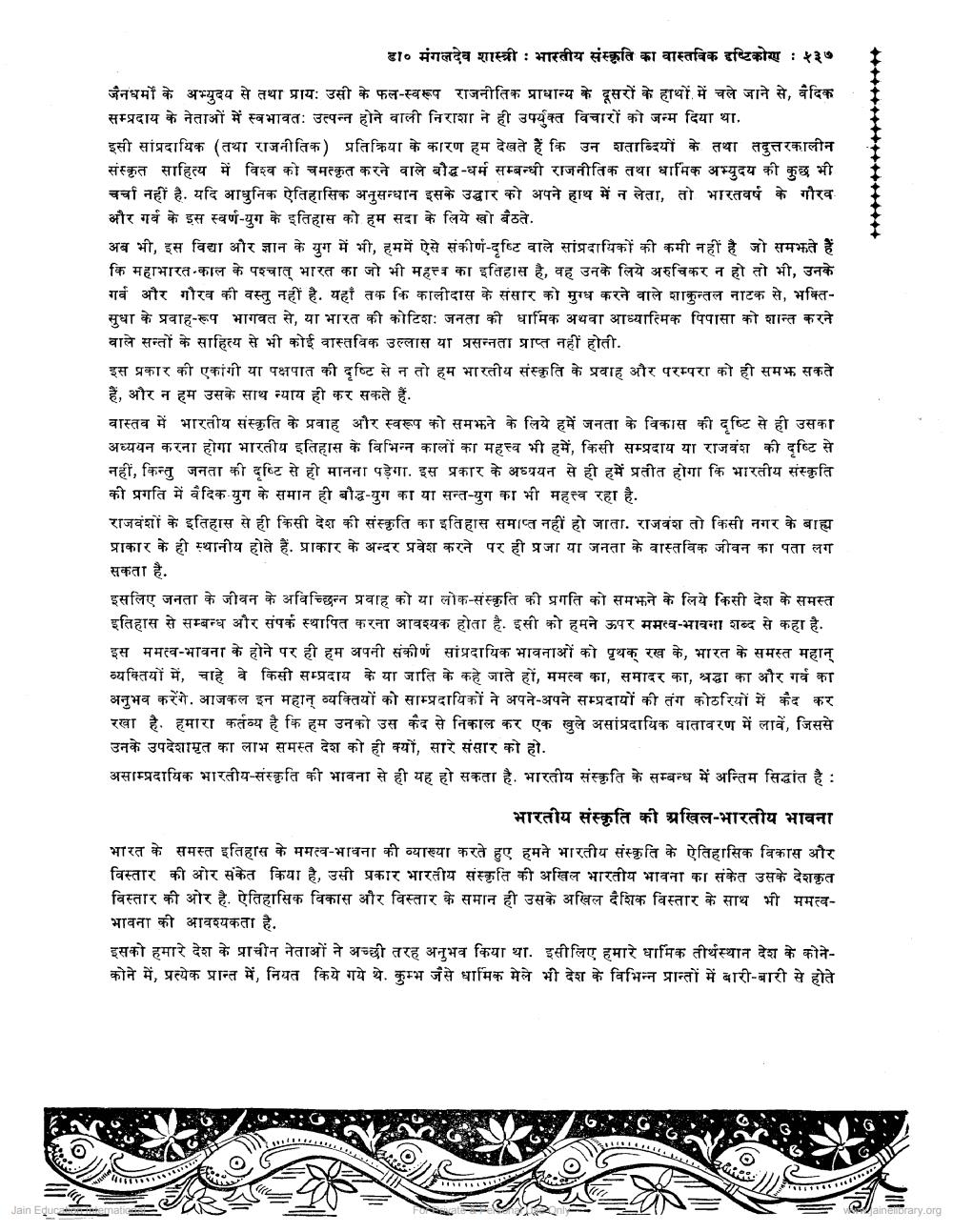Book Title: Bharatiya Sanskruti ka Vastavik Drushtikon Author(s): Mangaldev Shastri Publisher: Z_Hajarimalmuni_Smruti_Granth_012040.pdf View full book textPage 7
________________ डा. मंगलदेव शास्त्री : भारतीय संस्कृति का वास्तविक दृष्टिकोण : ५३७ जैनधों के अभ्युदय से तथा प्रायः उसी के फल-स्वरूप राजनीतिक प्राधान्य के दूसरों के हाथों में चले जाने से, वैदिक सम्प्रदाय के नेताओं में स्वभावतः उत्पन्न होने वाली निराशा ने ही उपर्युक्त विचारों को जन्म दिया था, इसी सांप्रदायिक (तथा राजनीतिक) प्रतिक्रिया के कारण हम देखते हैं कि उन शताब्दियों के तथा तदुत्तरकालीन संस्कृत साहित्य में विश्व को चमत्कृत करने वाले बौद्ध-धर्म सम्बन्धी राजनीतिक तथा धार्मिक अभ्युदय की कुछ भी चर्चा नहीं है. यदि आधुनिक ऐतिहासिक अनुसन्धान इसके उद्धार को अपने हाथ में न लेता, तो भारतवर्ष के गौरव और गर्व के इस स्वर्ण-युग के इतिहास को हम सदा के लिये खो बैठते. अब भी, इस विद्या और ज्ञान के युग में भी, हम में ऐसे संकीर्ण-दृष्टि वाले सांप्रदायिकों की कमी नहीं है जो समझते हैं कि महाभारत काल के पश्चात् भारत का जो भी महत्त्व का इतिहास है, वह उनके लिये अरुचिकर न हो तो भी, उनके गर्व और गौरव की वस्तु नहीं है. यहाँ तक कि कालीदास के संसार को मुग्ध करने वाले शाकुन्तल नाटक से, भक्तिसुधा के प्रवाह-रूप भागवत से, या भारत की कोटिशः जनता की धार्मिक अथवा आध्यात्मिक पिपासा को शान्त करने वाले सन्तों के साहित्य से भी कोई वास्तविक उल्लास या प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती. इस प्रकार की एकांगी या पक्षपात की दृष्टि से न तो हम भारतीय संस्कृति के प्रवाह और परम्परा को ही समझ सकते हैं, और न हम उसके साथ न्याय ही कर सकते हैं. वास्तव में भारतीय संस्कृति के प्रवाह और स्वरूप को समझने के लिये हमें जनता के विकास की दृष्टि से ही उसका अध्ययन करना होगा भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों का महत्त्व भी हमें, किसी सम्प्रदाय या राजवंश की दृष्टि से नहीं, किन्तु जनता की दृष्टि से ही मानना पड़ेगा. इस प्रकार के अध्ययन से ही हमें प्रतीत होगा कि भारतीय संस्कृति की प्रगति में वैदिक युग के समान ही बौद्ध-युग का या सन्त-युग का भी महत्त्व रहा है. राजवंशों के इतिहास से ही किसी देश की संस्कृति का इतिहास समाप्त नहीं हो जाता. राजवंश तो किसी नगर के बाह्य प्राकार के ही स्थानीय होते हैं. प्राकार के अन्दर प्रवेश करने पर ही प्रजा या जनता के वास्तविक जीवन का पता लग सकता है. इसलिए जनता के जीवन के अविच्छिन्न प्रवाह को या लोक-संस्कृति की प्रगति को समझने के लिये किसी देश के समस्त इतिहास से सम्बन्ध और संपर्क स्थापित करना आवश्यक होता है. इसी को हमने ऊपर ममत्व-भावना शब्द से कहा है. इस ममत्व-भावना के होने पर ही हम अपनी संकीर्ण सांप्रदायिक भावनाओं को पृथक् रख के, भारत के समस्त महान् व्यक्तियों में, चाहे वे किसी सम्प्रदाय के या जाति के कहे जाते हों, ममत्व का, समादर का, श्रद्धा का और गर्व का अनुभव करेंगे. आजकल इन महान् व्यक्तियों को साम्प्रदायिकों ने अपने-अपने सम्प्रदायों की तंग कोठरियों में कैद कर रखा है. हमारा कर्तव्य है कि हम उनको उस कैद से निकाल कर एक खुले असांप्रदायिक वातावरण में लावें, जिससे उनके उपदेशामृत का लाभ समस्त देश को ही क्यों, सारे संसार को हो. असाम्प्रदायिक भारतीय-संस्कृति की भावना से ही यह हो सकता है. भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में अन्तिम सिद्धांत है : भारतीय संस्कृति की अखिल-भारतीय भावना भारत के समस्त इतिहास के ममत्व-भावना की व्याख्या करते हुए हमने भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक विकास और विस्तार की ओर संकेत किया है, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति की अखिल भारतीय भावना का संकेत उसके देशकृत विस्तार की ओर है. ऐतिहासिक विकास और विस्तार के समान ही उसके अखिल दैशिक विस्तार के साथ भी ममत्वभावना की आवश्यकता है. इसको हमारे देश के प्राचीन नेताओं ने अच्छी तरह अनुभव किया था. इसीलिए हमारे धार्मिक तीर्थस्थान देश के कोनेकोने में, प्रत्येक प्रान्त में, नियत किये गये थे. कुम्भ जैसे धार्मिक मेले भी देश के विभिन्न प्रान्तों में बारी-बारी से होते C ainelorary.orgPage Navigation
1 ... 5 6 7 8