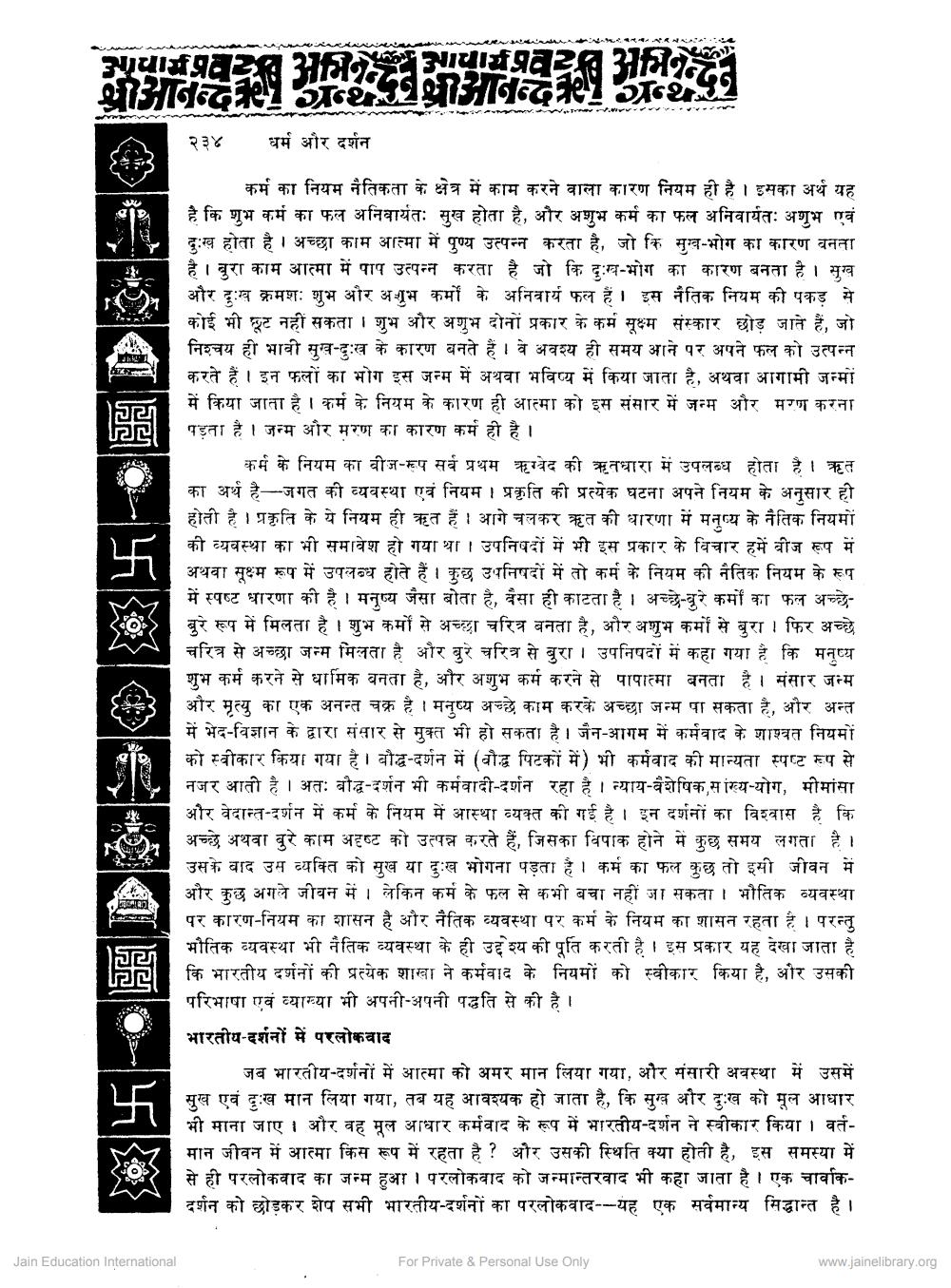Book Title: Bharatiya Darshan ke Samanya Siddhant Author(s): Vijay Muni Publisher: Z_Anandrushi_Abhinandan_Granth_012013.pdf View full book textPage 6
________________ आचार्य प्रद अभिनन्दन आआनन्द अन्थ आयायप्रवर अभिनंदन श्री आनन्दाय Jain Education International २३४ धर्म और दर्शन कर्म का नियम नैतिकता के क्षेत्र में काम करने वाला कारण नियम ही है। इसका अर्थ यह है कि शुभ कर्म का फल अनिवार्यतः सुख होता है, और अशुभ कर्म का फल अनिवार्यतः अशुभ एवं दुःख होता है । अच्छा काम आत्मा में पुण्य उत्पन्न करता है, जो कि सुख भोग का कारण बनता है बुरा काम आत्मा में पाप उत्पन्न करता है जो कि दुःख भोग का कारण बनता है। सुख और दुःख क्रमश: शुभ और अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल हैं। इस नैतिक नियम की पकड़ से कोई भी छूट नहीं सकता। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म सूक्ष्म संस्कार छोड़ जाते हैं, जो निश्चय ही भावी सुख-दुःख के कारण बनते हैं । वे अवश्य ही समय आने पर अपने फल को उत्पन्न करते हैं । इन फलों का भोग इस जन्म में अथवा भविष्य में किया जाता है, अथवा आगामी जन्मों में किया जाता है। कर्म के नियम के कारण ही आत्मा को इस संसार में जन्म और मरण करना पड़ता है । जन्म और मरण का कारण कर्म ही है । 1 कर्म के नियम का बीज रूप सर्व प्रथम ऋग्वेद की ऋतधारा में उपलब्ध होता है । ऋत का अर्थ है-जगत की व्यवस्था एवं नियम प्रकृति की प्रत्येक घटना अपने नियम के अनुसार ही होती है। प्रकृति के ये नियम ही ऋत हैं। आगे चलकर ऋत की धारणा में मनुष्य के नैतिक नियमों की व्यवस्था का भी समावेश हो गया था। उपनिषदों में भी इस प्रकार के विचार हमें बीज रूप में अथवा सूक्ष्म रूप में उपलब्ध होते हैं । कुछ उपनिषदों में तो कर्म के नियम की नैतिक नियम के रूप में स्पष्ट धारणा की है । मनुष्य जैसा बोता है, वैसा ही काटता है। अच्छे-बुरे कर्मों का फल अच्छेबुरे रूप में मिलता है। शुभ रूमों से अच्छा चरित्र बनता है, और अशुभ कर्मों से बुरा। फिर अच्छे चरित्र से अच्छा जन्म मिलता है और बुरे चरित्र से बुरा उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य शुभ कर्म करने से धार्मिक बनता है, और अशुभ कर्म करने से पापात्मा बनता है। संसार जन्म और मृत्यु का एक अनन्त चक्र है । मनुष्य अच्छे काम करके अच्छा जन्म पा सकता है, और अन्त में भेद - विज्ञान के द्वारा संसार से मुक्त भी हो सकता है। जैन आगम में कर्मवाद के शाश्वत नियमों को स्वीकार किया गया है बौद्ध दर्शन में (बौद्ध पिटकों में भी कर्मवाद की मान्यता स्पष्ट रूप से नजर आती है। अतः बौद्ध दर्शन भी कर्मवादी दर्शन रहा है। न्याय-वैशेषिक, सांख्ययोग, मीमांसा और वेदान्त दर्शन में कर्म के नियम में आस्था व्यक्त की गई है। इन दर्शनों का विश्वास है कि अच्छे अथवा बुरे काम अदृष्ट को उत्पन्न करते हैं, जिसका विपाक होने में कुछ समय लगता है। उसके बाद उस व्यक्ति को सुख या दुःख भोगना पड़ता है। कर्म का फल कुछ तो इसी जीवन में और कुछ अगले जीवन में। लेकिन कर्म के फल से कभी बचा नहीं जा सकता। भौतिक व्यवस्था पर कारण नियम का शासन है और नैतिक व्यवस्था पर कर्म के नियम का शासन रहता है । परन्तु मौतिक व्यवस्था भी नैतिक व्यवस्था के ही उद्देश्य की पूर्ति करती है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि भारतीय दर्शनों की प्रत्येक शाखा ने कर्मवाद के नियमों को स्वीकार किया है, और उसकी परिभाषा एवं स्याम्या भी अपनी-अपनी पद्धति से की है। भारतीय दर्शनों में परलोकवाद जब भारतीय दर्शनों में आत्मा को अमर मान लिया गया, और संसारी अवस्था में उसमें सुख एवं दुःख मान लिया गया, तब यह आवश्यक हो जाता है, कि सुख और दुःख को मूल आधार भी माना जाए और वह मूल आधार कर्मवाद के रूप में भारतीय दर्शन ने स्वीकार किया। वर्त मान जीवन में आत्मा किस रूप में रहता है? और उसकी स्थिति क्या होती है, इस समस्या में से ही परलोकवाद का जन्म हुआ । परलोकवाद को जन्मान्तरवाद भी कहा जाता है। एक चार्वाकदर्शन को छोड़कर शेष सभी भारतीय दर्शनों का परलोकवाद --- यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है । For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10