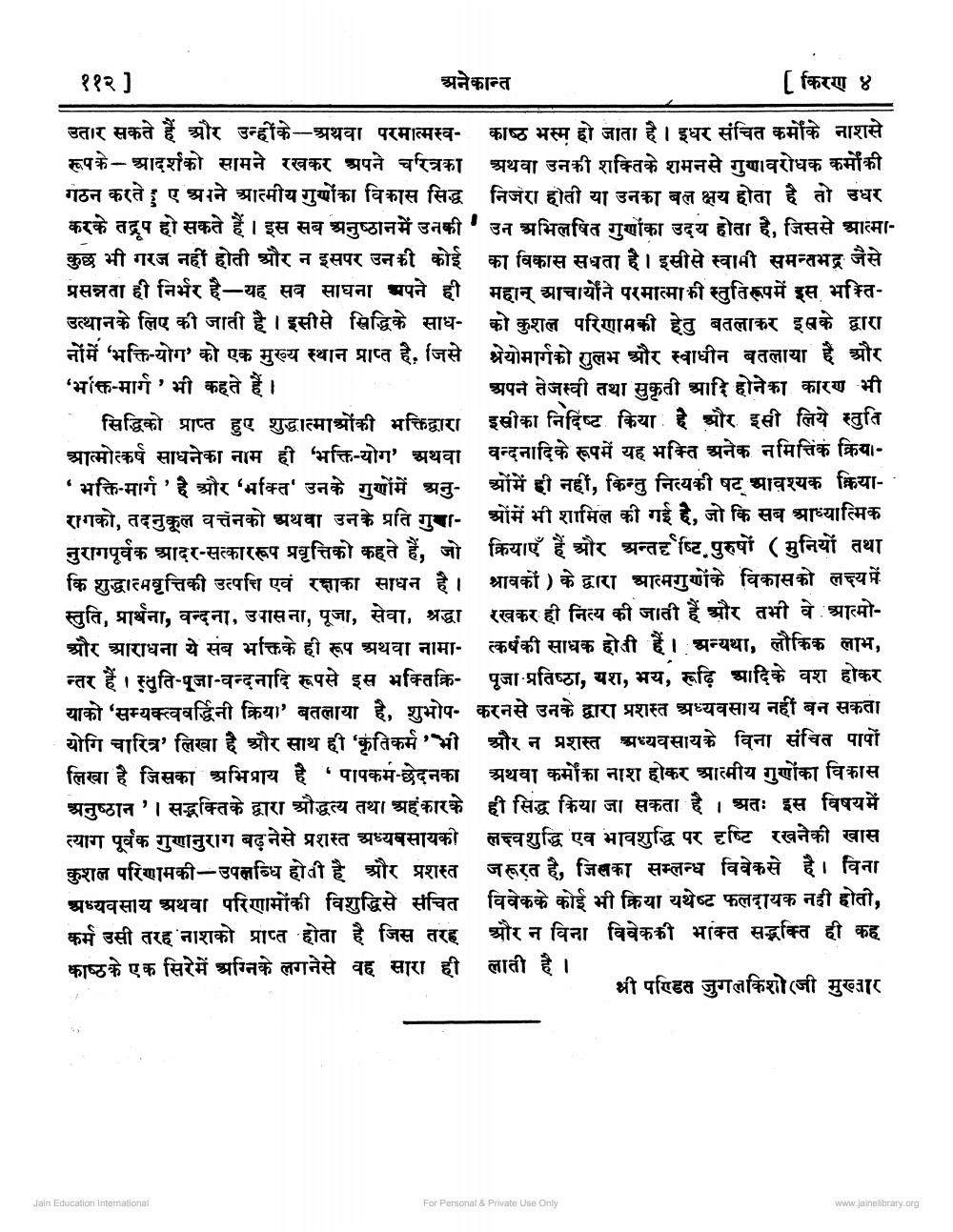________________
११२]
उतार सकते हैं और उन्होंके - अथवा परमात्मस्वरूपके - आदर्शको सामने रखकर अपने चरित्रका गठन करते हुए अपने आत्मीय गुणका विकास सिद्ध करके तद्रूप हो सकते हैं । इस सब अनुष्ठानमें उनकी कुछ भी गरज नहीं होती और न इसपर उनकी कोई प्रसन्नता ही निर्भर है - यह सब साधना अपने ही उत्थान के लिए की जाती है । इसीसे सिद्धिके साधनोंमें ‘भक्ति-योग' को एक मुख्य स्थान प्राप्त है, जिसे 'भक्ति मार्ग' भी कहते हैं ।
अनेकान्त
सिद्धिको प्राप्त हुए शुद्धात्माओं की भक्तिद्वारा आत्मोत्कर्ष साधने का नाम ही 'भक्ति योग' अथवा 'भक्ति-मार्ग' है और 'भक्ति' उनके गुणोंमें अनुरागको, तदनुकूल वत्र्त्तेनको अथवा उनके प्रति गुणानुरागपूर्वक आदर-सत्काररूप प्रवृत्तिको कहते हैं, जो कि शुद्धात्मवृत्तिकी उत्पत्ति एवं रक्षाका साधन है । स्तुति, प्रार्थना, वन्दना, उपासना, पूजा, सेवा, श्रद्धा और आराधना ये सब भक्तिके ही रूप अथवा नामान्तर हैं। तुति-पूजा-वन्दनादि रूपसे इस भक्तिक्रियाको 'सम्यक्त्ववर्द्धिनी क्रिया' बतलाया है, शुभोपयोग चारित्र' लिखा है और साथ ही 'कृतिकर्म भी लिखा है जिसका अभिप्राय है पापकर्म छेदनका अनुष्ठान ' । सद्भक्तिके द्वारा औद्धत्य तथा अहंकार के त्याग पूर्वक गुणानुराग बढ़नेसे प्रशस्त अध्यवसायको कुशल परिणामकी - उपलब्धि होती है और प्रशस्त अध्यवसाय अथवा परिणामोंकी विशुद्धिसे संचित कर्म उसी तरह नाशको प्राप्त होता है जिस तरह काष्ठके एक सिरे में अग्निके लगनेसे वह सारा ही
"
Jain Education International
[ किरण ४
काष्ठ भस्म हो जाता है । इधर संचित कर्मोंके नाशसे अथवा उनकी शक्तिके शमनसे गुणावरोधक कर्मों की निर्जरा होती या उनका बल क्षय होता है तो उधर उन अभिलषित गुणोंका उदय होता है, जिससे आत्माका विकास सकता है । इसीसे स्वामी समन्तभद्र जैसे महान् आचार्योंने परमात्मा की स्तुतिरूप में इस भक्तिको कुशल परिणामकी हेतु बतलाकर इसके द्वारा श्रेयोमार्गको शुलभ और स्वाधीन बतलाया हैं और अपने तेजस्वी तथा सुकृती आदि होनेका कारण भी इसीका निर्दिष्ट किया है और इसी लिये स्तुति वन्दनादिके रूप में यह भक्ति अनेक नमित्तिकं क्रियाओंमें ही नहीं, किन्तु नित्यकी षट् आवश्यक क्रियाओंमें भी शामिल की गई है, जो कि सब आध्यात्मिक क्रियाएँ हैं और अन्तर्दृष्टि पुरुषों ( मुनियों तथा श्रावकों ) के द्वारा आत्मगुणोंके विकासको लक्ष्य में रखकर ही नित्य की जाती हैं और तभी वे आत्मोत्कर्ष की साधक होती हैं । अन्यथा, लौकिक लाभ, पूजा-प्रतिष्ठा, यश, भय, रूढ़ि आदि के वश होकर करनसे उनके द्वारा प्रशस्त अध्यवसाय नहीं बन सकता और न प्रशस्त अध्यवसाय के विना संचित पापों अथवा कर्मोंका नाश होकर आत्मीय गुणोंका विकास ही सिद्ध किया जा सकता है । अतः इस विषय में लक्ष्वशुद्धि एव भावशुद्धि पर दृष्टि रखनेकी खास जरूरत है, जिसका सम्बन्ध विवेकसे है । विना विवेकके कोई भी क्रिया यथेष्ट फलदायक नही होती, और न विना विवेककी भक्ति सद्भक्ति ही कह लाती है ।
श्री पण्डित जुगलकिशो (जी मुख्तार
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org