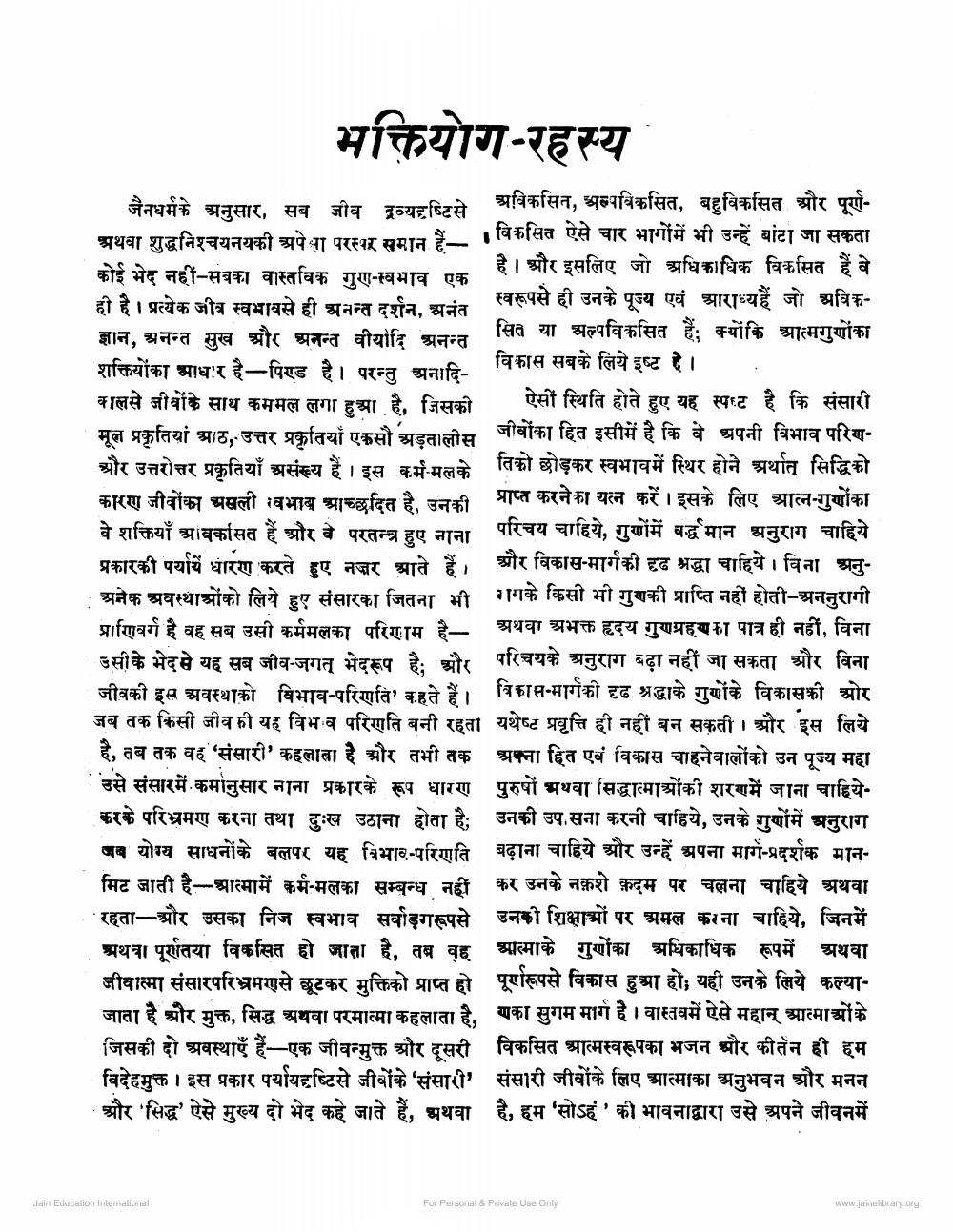________________
भक्तियोग-रहस्य
जैनधर्मके अनुसार, सब जीव द्रव्यदृष्टिसे अविकसित, अल्पविकसित, बहुविकसित और पर्णअथवा शुद्धनिश्चयनयकी अपेक्षा परस्पर समान हैं- । विकसित ऐसे चार भागोंमें भी उन्हें बांटा जा सकता कोई भेद नहीं-सबका वास्तविक गुण-स्वभाव एक है
है। और इसलिए जो अधिकाधिक विकसित हैं वे ही है। प्रत्येक जीव स्वभावसे ही अनन्त दर्शन, अनंत
स्वरूपसे ही उनके पूज्य एवं आराध्य हैं जो अविकज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीयोदि अनन्त
सित या अल्पविकसित हैं; क्योंकि आत्मगुणोंका शक्तियोंका आधार है-पिण्ड है। परन्तु अनादि
विकास सबके लिये इष्ट है। कालसे जीवों के साथ कममल लगा हुआ है, जिसकी ऐसी स्थिति होते हुए यह स्पष्ट है कि संसारी मूल प्रकृतियां आठ, उत्तर प्रकृतियाँ एकसौ अड़तालीस जीवोंका हित इसीमें है कि वे अपनी विभाव परिणऔर उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ असंख्य हैं । इस कर्म-मलके तिको छोड़कर स्वभावमें स्थिर होने अर्थात् सिद्धिको कारण जीवोंका असली स्वभाव आच्छादित है, उनकी प्राप्त करने का यत्न करें। इसके लिए आत्न-गुणोंका वे शक्तियाँ आवकसित हैं और वे परतन्त्र हुए नाना परिचय चाहिये, गुणमें वर्द्धमान अनुराग चाहिये प्रकारकी पर्यायें धारण करते हुए नजर आते हैं। और विकास-मार्गकी दृढ श्रद्धा चाहिये। विना अनुअनेक अवस्थाओंको लिये हुए संसारका जितना भी गगके किसी भी गुणकी प्राप्ति नहीं होती-अननुरागी प्राणिवर्ग है वह सब उसी कर्ममलका परिणाम है- अथवा अभक्त हृदय गुणग्रहण का पात्र ही नहीं, विना उसीके भेदसे यह सब जीव-जगत भेदरूप है. और परिचयके अनुराग बढ़ा नहीं जा सकता और विना जीवकी इस अवस्थाको विभाव-परिणति' कहते हैं। विकास-मार्गको दृढ श्रद्धाके गुणों के विकासकी ओर जब तक किसी जीव की यह विभ व परिणति बनी रहता यथेष्ट प्रवृत्ति ही नहीं बन सकती। और इस लिये है, तब तक वह 'संसारी' कहलाता है और तभी तक अपना हित एवं विकास चाहनेवालोंको उन पूज्य महा उसे संसारमें कर्मानुसार नाना प्रकारके रूप धारण पुरुषों अथवा सिद्धात्माओंकी शरणमें जाना चाहिये. करके परिभ्रमण करना तथा दुःख उठाना होता है; उनकी उपासना करनी चाहिये, उनके गुणोंमें अनुराग जब योग्य साधनोंके बलपर यह विभाव-परिणति बढ़ाना चाहिये और उन्हें अपना मार्ग-प्रदर्शक मानमिट जाती है-आत्मामें कर्म-मलका सम्बन्ध नहीं कर उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिये अथवा रहता और उसका निज स्वभाव सर्वाइंगरूपसे उनकी शिक्षाओं पर अमल करना चाहिये, जिनमें अथवा पूर्णतया विकसित हो जाता है, तब वह आत्माके गुणोंका अधिकाधिक रूपमें अथवा जीवात्मा संसारपरिभ्रमणसे छूटकर मुक्तिको प्राप्त हो पूर्णरूपसे विकास हुआ हो; यही उनके लिये कल्याजाता है और मुक्त, सिद्ध अथवा परमात्मा कहलाता है, यका सुगम मार्ग है । वास्तवमें ऐसे महान् आत्माओं के जिसकी दो अवस्थाएँ हैं—एक जीवन्मुक्त और दूसरी विकसित आत्मस्वरूपका भजन और कीर्तन ही हम विदेहमुक्त । इस प्रकार पर्यायदृष्टिसे जीवोंके 'संसारी' संसारी जीवोंके लिए आत्माका अनुभवन और मनन और 'सिद्ध' ऐसे मुख्य दो भेद कहे जाते हैं, अथवा है, हम 'सोऽहं ' की भावनाद्वारा उसे अपने जीवनमें
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org