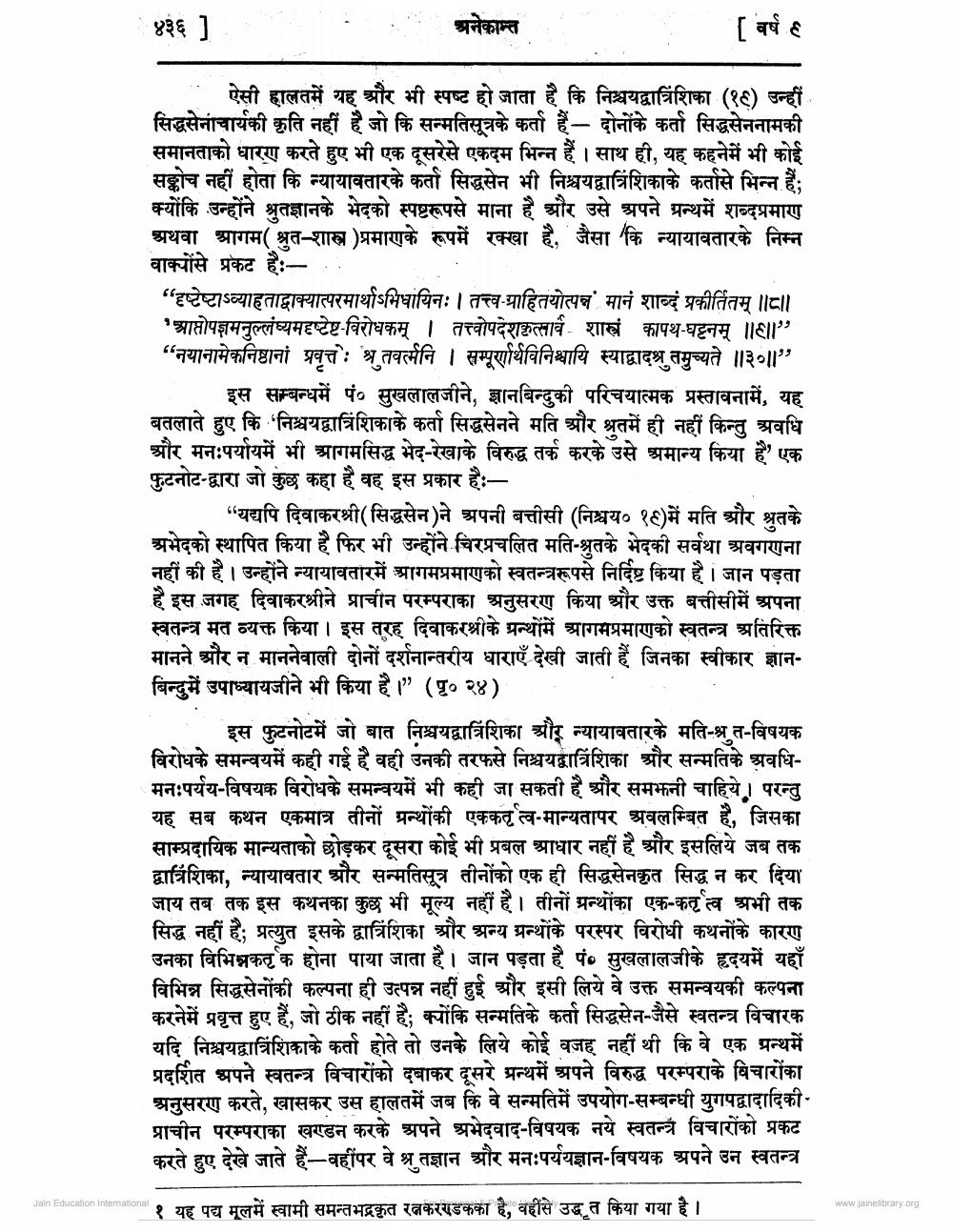________________
४३६ ]
[ वर्ष
ऐसी हालत में यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि निश्चयद्वात्रिंशिका (१६) उन्हीं सिद्धसेनाचार्य की कृति नहीं है जो कि सन्मतिसूत्रके कर्ता हैं- दोनोंके कर्ता सिद्धसेन नामकी समानताको धारण करते हुए भी एक दूसरेसे एकदम भिन्न हैं। साथ ही, यह कहने में भी कोई सङ्कोच नहीं होता कि न्यायावतारके कर्ता सिद्धसेन भी निश्चयद्वात्रिंशिका के कर्ता से भिन्न हैं; क्योंकि उन्होंने श्रुतज्ञानके भेदको स्पष्टरूपसे माना है और उसे अपने ग्रन्थमें शब्दप्रमाण अथवा आगम ( श्रुत-शास्त्र ) प्रमाणके रूपमें रक्खा है, जैसा कि न्यायावतार के निम्न वाक्योंसे प्रकट है:
का
“दृष्टेष्टाऽव्याहताद्वाक्यात्परमार्थाऽभिधायिनः । तत्त्व-ग्राहितयोत्पन्न मानं शाब्दं प्रकीर्तितम् ॥८॥ 'आप्तोपज्ञमनुल्लंघ्यमदृष्टेष्ट - विरोधकम् । तत्त्वोपदेशकृत्सार्व शास्त्रं कापथ - घट्टनम् ॥” “नयानामेकनिष्ठानां प्रवृत्त ेः श्रुतवर्त्मनि । सम्पूर्णार्थविनिश्वायि स्याद्वादश्रु तमुच्यते ॥३०॥”
इस सम्बन्धमें पं० सुखलालजीने, ज्ञानबिन्दुकी परिचयात्मक प्रस्तावना में, यह बतलाते हुए कि 'निश्चयद्वात्रिंशिका के कर्ता सिद्धसेनने मति और श्रुतमें ही नहीं किन्तु अवधि और मनःपर्याय में भी आगमसिद्ध भेद-रेखा के विरुद्ध तर्क करके उसे अमान्य किया है' एक फुटनोट- द्वारा जो कुछ कहा है वह इस प्रकार है:
“यद्यपि दिवाकरश्री(सिद्धसेन ) ने अपनी बत्तीसी (निश्चय० १६ ) में मति और श्रुतके अभेदको स्थापित किया है फिर भी उन्होंने चिरप्रचलित मति श्रुतके भेदकी सर्वथा अवगणना नहीं की है। उन्होंने न्यायावतार में आगमप्रमाणको स्वतन्त्ररूपसे निर्दिष्ट किया है । जान पड़ता है इस जगह दिवाकरश्रीने प्राचीन परम्पराका अनुसरण किया और उक्त बत्तीसी में अपना स्वतन्त्र मत व्यक्त किया । इस तरह दिवाकर श्री के ग्रन्थोंमें श्रागमप्रमाणको स्वतन्त्र अतिरिक्त मानने और न माननेवाली दोनों दर्शनान्तरीय धाराएँ देखी जाती हैं जिनका स्वीकार ज्ञानबिन्दुमें उपाध्यायजीने भी किया है ।" ( पृ० २४ )
Jain Education International.
इस फुटनोटमें जो बात निश्चयद्वात्रिंशिका और न्यायावतार के मति श्रुत-विषयक विरोधके समन्वय में कही गई है वही उनकी तरफसे निश्चयद्वात्रिंशिका और सन्मति के अवधिमन:पर्यय-विषयक विरोधके समन्वयमें भी कही जा सकती है और समझनी चाहिये । परन्तु यह सब कथन एकमात्र तीनों ग्रन्थोंकी एककट त्व- मान्यतापर अवलम्बित है, जिसका साम्प्रदायिक मान्यताको छोड़कर दूसरा कोई भी प्रबल आधार नहीं है और इसलिये जब तक द्वात्रिंशिका, न्यायावतार और सन्मतिसूत्र तीनोंको एक ही सिद्धसेनकृत सिद्ध न कर दिया जाय तब तक इस कथनका कुछ भी मूल्य नहीं है । तीनों ग्रन्थोंका एक कर्तृत्व अभी तक सिद्ध नहीं है; प्रत्युत इसके द्वात्रिंशिका और अन्य ग्रन्थोंके परस्पर विरोधी कथनों के कारण उनका विभिन्नकट के होना पाया जाता है। जान पड़ता है पं० सुखलालजीके हृदयमें यहाँ विभिन्न सिद्धसेनोंकी कल्पना ही उत्पन्न नहीं हुई और इसी लिये वे उक्त समन्वयकी कल्पना करने में प्रवृत्त हुए हैं, जो ठीक नहीं है; क्योंकि सन्मति के कर्ता सिद्धसेन - जैसे स्वतन्त्र विचारक यदि निश्चयद्वात्रिंशिका कर्ता होते तो उनके लिये कोई वजह नहीं थी कि वे एक ग्रन्थमें प्रदर्शित अपने स्वतन्त्र विचारोंको दबाकर दूसरे प्रन्थ में अपने विरुद्ध परम्परा के विचारोंका अनुसरण करते, खासकर उस हालत में जब कि वे सन्मतिमें उपयोग सम्बन्धी युगपद्वादादिकीप्राचीन परम्पराका खण्डन करके अपने अभेदवाद - विषयक नये स्वतन्त्र विचारोंको प्रकट करते हुए देखे जाते हैं- वहीं पर वे श्रुतज्ञान और मन:पर्ययज्ञान विषयक अपने उन स्वतन्त्र
१ यह पद्य मूल में स्वामी समन्तभद्रकृत रत्नकरण्डकका है, वहींसे उद्धृत किया गया है ।
www.jainelibrary.org