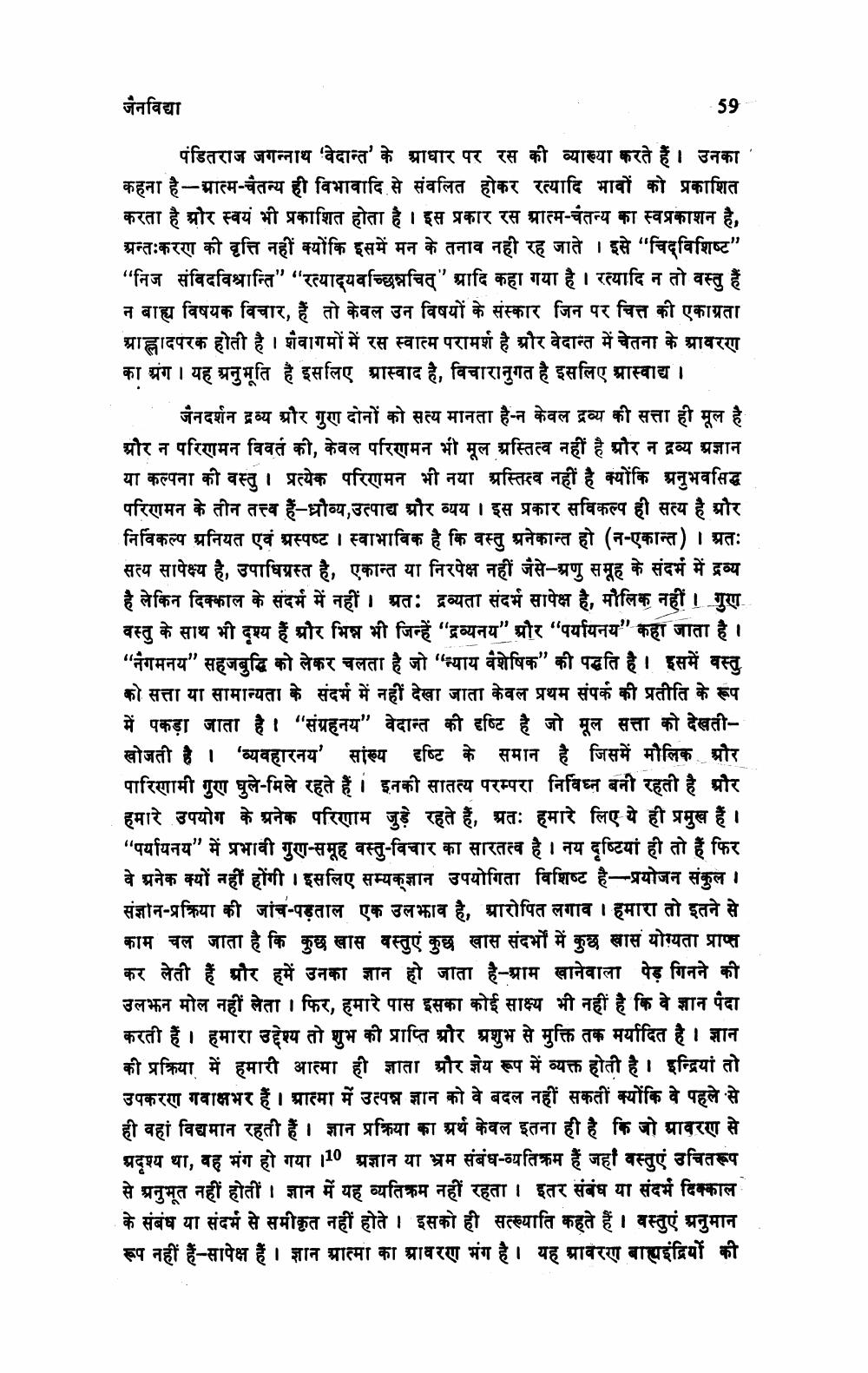________________
जैन विद्या
59
पंडितराज जगन्नाथ 'वेदान्त' के आधार पर रस की व्याख्या करते हैं । उनका कहना है - प्रात्म - चैतन्य ही विभावादि से संवलित होकर रत्यादि भावों को प्रकाशित करता है और स्वयं भी प्रकाशित होता है । इस प्रकार रस श्रात्म-चंतन्य का स्वप्रकाशन है, अन्तःकरण की वृत्ति नहीं क्योंकि इसमें मन के तनाव नही रह जाते । इसे "चिद्विशिष्ट" "निज संविदविश्रान्ति" "रत्याद्यवच्छिन्नचित्" प्रादि कहा गया है । रत्यादि न तो वस्तु हैं। न बाह्य विषयक विचार, हैं तो केवल उन विषयों के संस्कार जिन पर चित्त की एकाग्रता प्रह्लादपरक होती है । शैवागमों में रस स्वात्म परामर्श है और वेदान्त में चेतना के आवरण का अंग । यह अनुभूति है इसलिए प्रास्वाद है, विचारानुगत है इसलिए आस्वाद्य ।
जैन दर्शन द्रव्य और गुण दोनों को सत्य मानता है-न केवल द्रव्य की सत्ता ही मूल है और न परिणमन विवर्त की, केवल परिरणमन भी मूल अस्तित्व नहीं है और न द्रव्य अज्ञान या कल्पना की वस्तु । प्रत्येक परिणमन भी नया अस्तित्व नहीं है क्योंकि अनुभवसिद्ध परिणमन के तीन तत्त्व हैं- ध्रौव्य, उत्पाद्य और व्यय । इस प्रकार सविकल्प ही सत्य है और निर्विकल्प अनियत एवं अस्पष्ट । स्वाभाविक है कि वस्तु अनेकान्त हो ( न- एकान्त ) । श्रतः सत्य सापेक्ष्य है, उपाधिग्रस्त है, एकान्त या निरपेक्ष नहीं जैसे- अणु समूह के संदर्भ में द्रव्य है लेकिन दिक्काल के संदर्भ में नहीं । अतः द्रव्यता संदर्भ सापेक्ष है, मौलिक नहीं । गुरण वस्तु के साथ भी दृश्य हैं और भिन्न भी जिन्हें " द्रव्यनय" और "पर्यायनय" कहा जाता है । "नगमनय" सहजबुद्धि को लेकर चलता है जो “न्याय वैशेषिक" की पद्धति है । इसमें वस्तु को सत्ता या सामान्यता के संदर्भ में नहीं देखा जाता केवल प्रथम संपर्क की प्रतीति के रूप में पकड़ा जाता है । " संग्रहनय" वेदान्त की दृष्टि है जो मूल सत्ता को देखती - खोजती है । 'व्यवहारनय' सांख्य दृष्टि के समान है जिसमें मौलिक और पारिणामी गुरण घुले-मिले रहते हैं । इनकी सातत्य परम्परा निर्विघ्न बनी रहती है और हमारे उपयोग के अनेक परिणाम जुड़े रहते हैं, अतः हमारे लिए ये ही प्रमुख हैं । " पर्यायनय" में प्रभावी गुण-समूह वस्तु-विचार का सारतत्व है । नय दृष्टियां ही तो हैं फिर
मुक्ति तक मर्यादित है । ज्ञान
अनेक क्यों नहीं होंगी । इसलिए सम्यक्ज्ञान उपयोगिता विशिष्ट है - प्रयोजन संकुल । संज्ञान- प्रक्रिया की जांच-पड़ताल एक उलझाव है, श्रारोपित लगाव । हमारा तो इतने से काम चल जाता है कि कुछ खास वस्तुएं कुछ खास संदर्भों में कुछ खास योग्यता प्राप्त कर लेती हैं और हमें उनका ज्ञान हो जाता है - ग्राम खानेवाला पेड़ गिनने की उलझन मोल नहीं लेता । फिर, हमारे पास इसका कोई साक्ष्य भी नहीं है कि वे ज्ञान पैदा करती हैं । हमारा उद्देश्य तो शुभ की प्राप्ति और प्रशुभ से की प्रक्रिया में हमारी आत्मा ही ज्ञाता और ज्ञेय रूप में व्यक्त होती है । इन्द्रियां तो उपकरण गवाक्षभर हैं । श्रात्मा में उत्पन्न ज्ञान को वे बदल नहीं सकती क्योंकि वे पहले से ही वहां विद्यमान रहती हैं। ज्ञान प्रक्रिया का अर्थ केवल इतना ही है कि जो प्रावरण से अदृश्य था, वह भंग हो गया । 10 प्रज्ञान या भ्रम संबंध व्यतिक्रम हैं जहाँ वस्तुएं उचितरूप से अनुभूत नहीं होतीं । ज्ञान में यह व्यतिक्रम नहीं रहता । इतर संबंध या संदर्भ दिक्काल . के संबंध या संदर्भ से समीकृत नहीं होते। इसको ही सत्ख्याति कहते हैं । वस्तुएं अनुमान रूप नहीं हैं - सापेक्ष हैं । ज्ञान आत्मा का प्रावरण मंग है । यह प्रावरण बाह्यइंद्रियों की