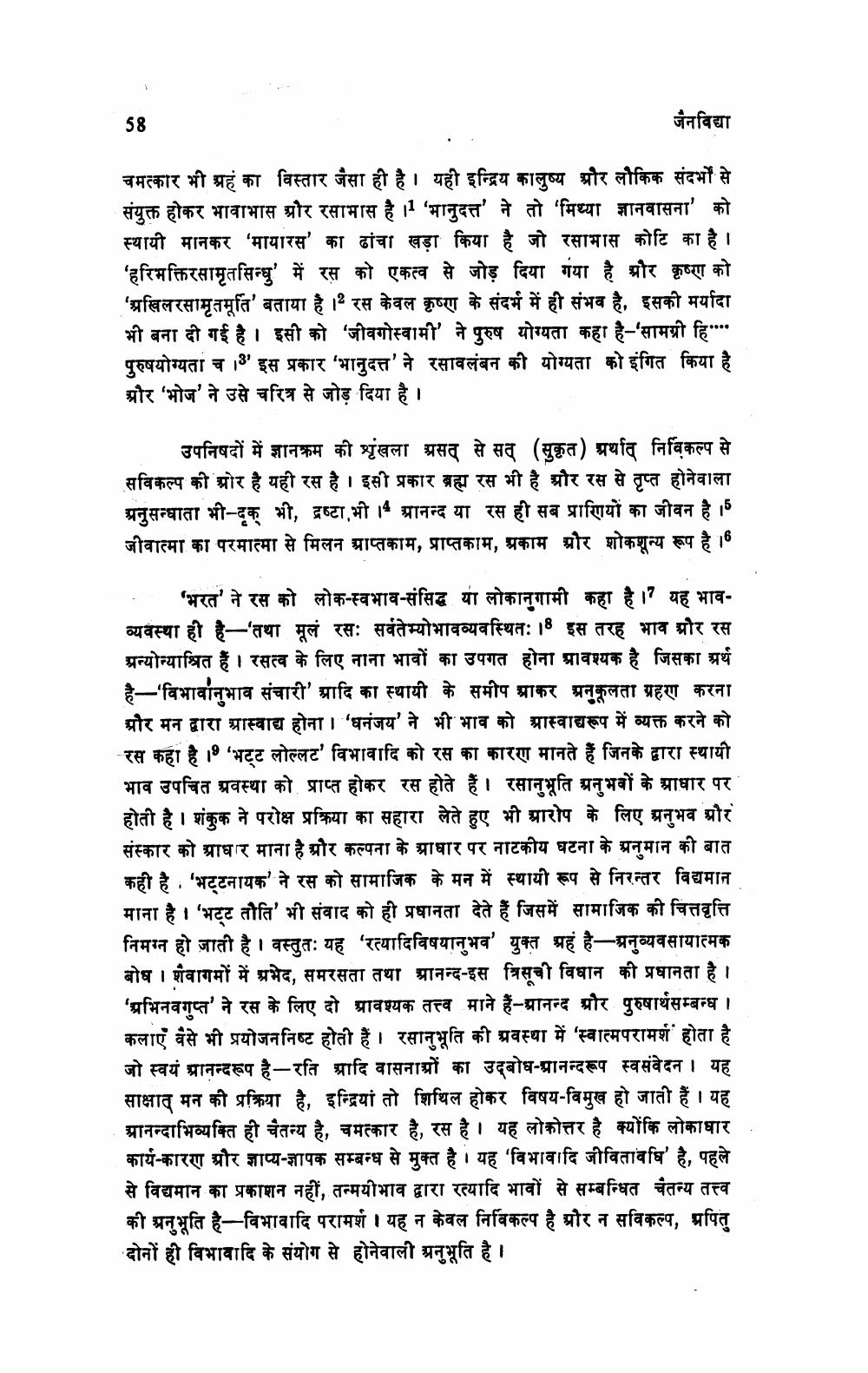________________
जैन विद्या
चमत्कार भी अहं का विस्तार जैसा ही है । यही इन्द्रिय कालुष्य और लौकिक संदर्भों से संयुक्त होकर भावाभास और रसाभास है ।1 'भानुदत्त' ने तो 'मिथ्या ज्ञानवासना' को स्थायी मानकर 'मायारस' का ढांचा खड़ा किया है जो रसाभास कोटि का है । 'हरिभक्तिरसामृत सिन्धु' में रस को एकत्व से जोड़ दिया गया है और कृष्ण को 'अखिलरसामृतमूर्ति' बताया है । 2 रस केवल कृष्ण के संदर्भ में संभव है, इसकी मर्यादा भी बना दी गई है । इसी को 'जीवगोस्वामी' ने पुरुष योग्यता कहा है- 'सामग्री हि ... पुरुषयोग्यता च । " इस प्रकार 'भानुदत्त' ने रसावलंबन की योग्यता को इंगित किया है। और 'भोज' ने उसे चरित्र से जोड़ दिया है ।
58
उपनिषदों में ज्ञानक्रम की श्रृंखला असत् से सत् (सुकृत) अर्थात् निर्विकल्प से सविकल्प की ओर है यही रस है । इसी प्रकार ब्रह्म रस भी है और रस से 'तृप्त होनेवाला अनुसन्धाता भी - दृक् भी, द्रष्टा भी । आनन्द या रस ही सब प्राणियों का जीवन है 15 जीवात्मा का परमात्मा से मिलन प्राप्तकाम, प्राप्तकाम, प्रकाम और शोकशून्य रूप है ।
'भरत' ने रस को लोक स्वभाव-संसिद्ध या लोकानुगामी कहा है। 7 यह भाव - व्यवस्था ही है- 'तथा मूलं रसः सर्वतेभ्यो भावव्यवस्थितः । 8 इस तरह भाव और रस अन्योन्याश्रित हैं । रसत्व के लिए नाना भावों का उपगत होना श्रावश्यक है जिसका अर्थ है— 'विभावानुभाव संचारी' आदि का स्थायी के समीप आकर अनुकूलता ग्रहण करना और मन द्वारा आस्वाद्य होना। 'धनंजय' ने भी भाव को प्रास्वाद्यरूप में व्यक्त करने को -रस कहा है ।" 'भट्ट लोल्लट' विभावादि को रस का कारण मानते हैं जिनके द्वारा स्थायी भाव उपचित अवस्था को प्राप्त होकर रस होते हैं । रसानुभूति अनुभवों के आधार पर होती है । शंकुक ने परोक्ष प्रक्रिया का सहारा लेते हुए भी प्रारोप के लिए अनुभव और संस्कार को आधार माना है और कल्पना के आधार पर नाटकीय घटना के अनुमान की बात कही है. 'भट्टनायक' ने रस को सामाजिक के मन में स्थायी रूप से निरन्तर विद्यमान माना है । 'भट्ट तौति' भी संवाद को ही प्रधानता देते हैं जिसमें सामाजिक की चित्तवृत्ति निमग्न हो जाती है । वस्तुतः यह 'रत्यादिविषयानुभव' युक्त प्रहं है - प्रनुव्यवसायात्मक बोध । शैवागमों में प्रभेद, समरसता तथा श्रानन्द-इस त्रिसूची विधान की प्रधानता है । 'अभिनवगुप्त' ने रस के लिए दो श्रावश्यक तत्त्व माने हैं - प्रानन्द और पुरुषार्थसम्बन्ध । कलाएँ वैसे भी प्रयोजननिष्ट होती हैं । रसानुभूति की अवस्था में 'स्वात्मपरामर्श होता है जो स्वयं श्रानन्दरूप है - रति आदि वासनाओं का उद्बोध श्रानन्दरूप स्वसंवेदन । यह साक्षात् मन की प्रक्रिया है, इन्द्रियां तो शिथिल होकर विषय-विमुख हो जाती हैं । यह आनन्दाभिव्यक्ति ही चैतन्य है, चमत्कार है, रस है । यह लोकोत्तर है क्योंकि लोकाधार कार्य-कारण और ज्ञाप्य ज्ञापक सम्बन्ध से मुक्त है। यह 'विभावादि जीवितावधि' है, पहले से विद्यमान का प्रकाशन नहीं, तन्मयीभाव द्वारा रत्यादि भावों से सम्बन्धित चैतन्य तत्त्व की अनुभूति है - विभावादि परामर्श । यह न केवल निर्विकल्प है और न सविकल्प, श्रपितु दोनों ही विभावादि के संयोग से होनेवाली अनुभूति है ।