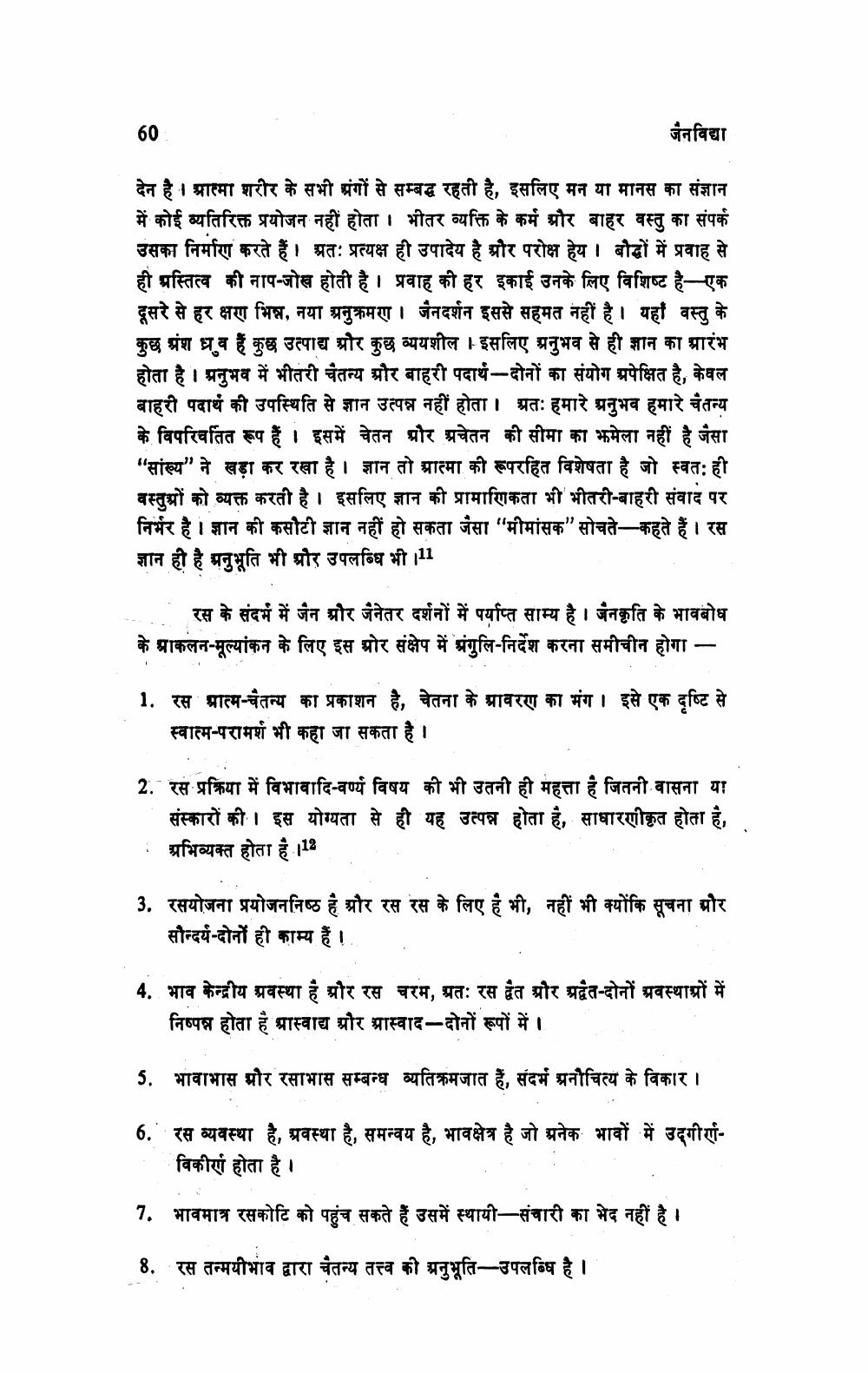________________
जनविद्या
देन है । प्रात्मा शरीर के सभी अंगों से सम्बद्ध रहती है, इसलिए मन या मानस का संज्ञान में कोई व्यतिरिक्त प्रयोजन नहीं होता। भीतर व्यक्ति के कर्म और बाहर वस्तु का संपर्क उसका निर्माण करते हैं। अतः प्रत्यक्ष ही उपादेय है और परोक्ष हेय । बौद्धों में प्रवाह से ही अस्तित्व की नाप-जोख होती है। प्रवाह की हर इकाई उनके लिए विशिष्ट है-एक दूसरे से हर क्षण भिन्न, नया अनुक्रमण । जनदर्शन इससे सहमत नहीं है। यहाँ वस्तु के कुछ अंश ध्र व हैं कुछ उत्पाद्य और कुछ व्ययशील । इसलिए अनुभव से ही ज्ञान का प्रारंभ होता है । अनुभव में भीतरी चैतन्य और बाहरी पदार्थ-दोनों का संयोग अपेक्षित है, केवल बाहरी पदार्थ की उपस्थिति से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अतः हमारे अनुभव हमारे चैतन्य के विपरिवर्तित रूप हैं । इसमें चेतन और अचेतन की सीमा का झमेला नहीं है जैसा "सांख्य" ने खड़ा कर रखा है। ज्ञान तो प्रात्मा की रूपरहित विशेषता है जो स्वत: ही वस्तुओं को व्यक्त करती है। इसलिए ज्ञान की प्रामाणिकता भी भीतरी-बाहरी संवाद पर निर्भर है । ज्ञान की कसौटी ज्ञान नहीं हो सकता जैसा "मीमांसक" सोचते-कहते हैं । रस ज्ञान ही है अनुभूति भी और उपलब्धि भी।11
- रस के संदर्भ में जैन और जनेतर दर्शनों में पर्याप्त साम्य है । जनकृति के भावबोध के प्राकलन-मूल्यांकन के लिए इस पोर संक्षेप में अंगुलि-निर्देश करना समीचीन होगा -
1. रस प्रात्म-चैतन्य का प्रकाशन है, चेतना के प्रावरण का मंग। इसे एक दृष्टि से
स्वात्म-परामर्श भी कहा जा सकता है।
2. रस प्रक्रिया में विभावादि-वर्ण्य विषय की भी उतनी ही महत्ता है जितनी वासना या
संस्कारों की। इस योग्यता से ही यह उत्पन्न होता है, साधारणीकृत होता है, . अभिव्यक्त होता है ।
3. रसयोजना प्रयोजननिष्ठ है और रस रस के लिए है भी, नहीं भी क्योंकि सूचना और ___ सौन्दर्य-दोनों ही काम्य हैं । ...
4. भाव केन्द्रीय अवस्था है और रस चरम, अतः रस द्वैत और अद्वैत-दोनों अवस्थाओं में
निष्पन्न होता है प्रास्वाद्य और प्रास्वाद-दोनों रूपों में ।
5. भावाभास और रसाभास सम्बन्ध व्यतिक्रमजात हैं, संदर्भ अनौचित्य के विकार ।
6. रस व्यवस्था है, अवस्था है, समन्वय है, भावक्षेत्र है जो अनेक भावों में उद्गीर्ण
विकीर्ण होता है। 7. भावमात्र रसकोटि को पहुंच सकते हैं उसमें स्थायी-संचारी का भेद नहीं है।
8. रस तन्मयीभाव द्वारा चैतन्य तत्त्व की अनुभूति-उपलब्धि है ।