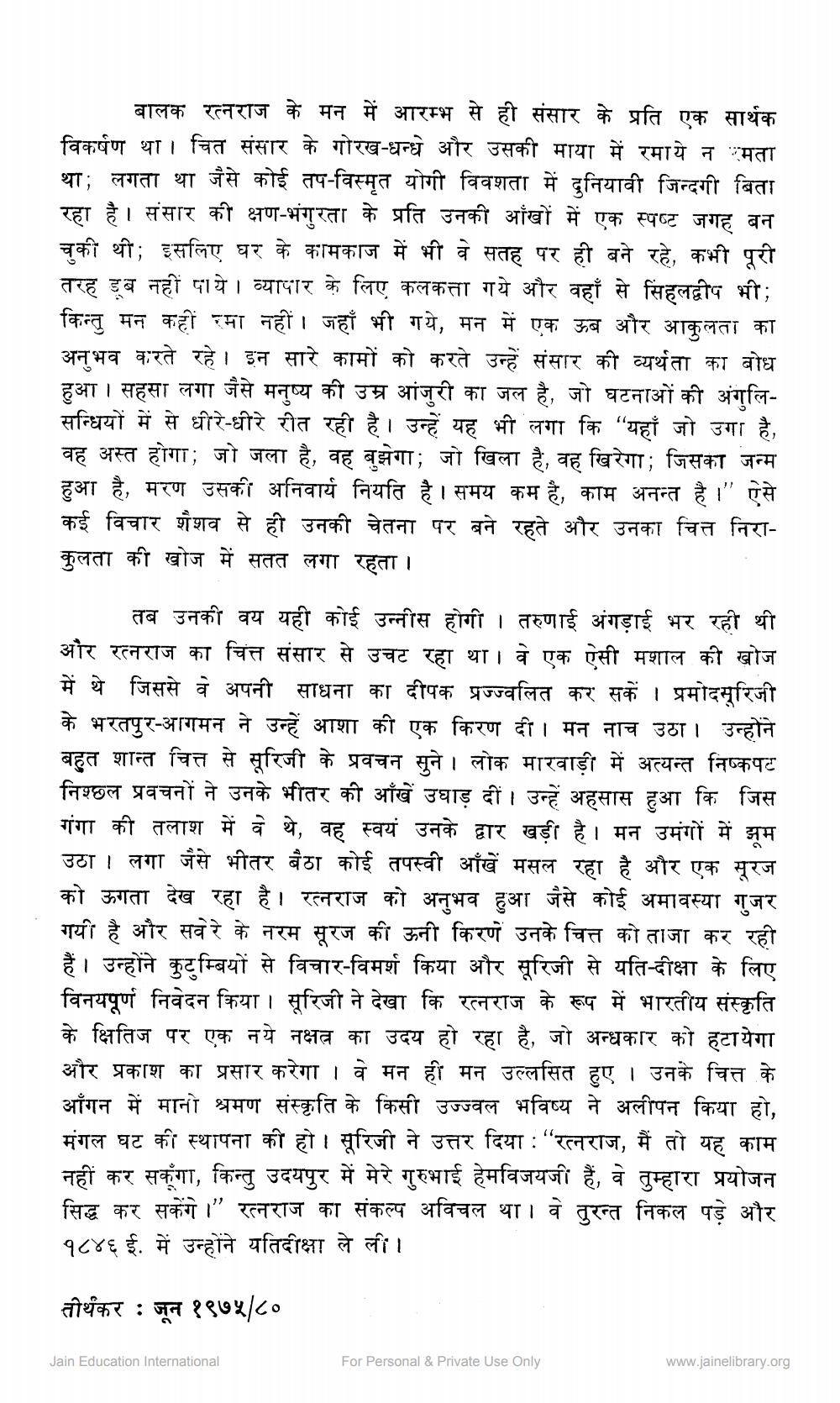________________
बालक रत्नराज के मन में आरम्भ से ही संसार के प्रति एक सार्थक विकर्षण था। चित संसार के गोरख-धन्धे और उसकी माया में रमाये न “मता था; लगता था जैसे कोई तप-विस्मृत योगी विवशता में दुनियावी जिन्दगी बिता रहा है। संसार की क्षण-भंगुरता के प्रति उनकी आँखों में एक स्पष्ट जगह बन चकी थी; इसलिए घर के कामकाज में भी वे सतह पर ही बने रहे, कभी पूरी तरह डब नहीं पाये। व्यापार के लिए कलकत्ता गये और वहाँ से सिंहलद्वीप भी; किन्तु मन कहीं रमा नहीं। जहाँ भी गये, मन में एक ऊब और आकुलता का अनुभव करते रहे। इन सारे कामों को करते उन्हें संसार की व्यर्थता का बोध हुआ। सहसा लगा जैसे मनुष्य की उम्र आंजुरी का जल है, जो घटनाओं की अंगुलिसन्धियों में से धीरे-धीरे रीत रही है। उन्हें यह भी लगा कि “यहाँ जो उगा है, वह अस्त होगा; जो जला है, वह बुझेगा; जो खिला है, वह खिरेगा; जिसका जन्म हुआ है, मरण उसकी अनिवार्य नियति है। समय कम है, काम अनन्त है।" ऐसे कई विचार शैशव से ही उनकी चेतना पर बने रहते और उनका चित्त निराकुलता की खोज में सतत लगा रहता।
तब उनकी वय यही कोई उन्नीस होगी । तरुणाई अंगड़ाई भर रही थी और रत्नराज का चित्त संसार से उचट रहा था। वे एक ऐसी मशाल की खोज में थे जिससे वे अपनी साधना का दीपक प्रज्ज्वलित कर सकें । प्रमोदसुरिजी के भरतपुर-आगमन ने उन्हें आशा की एक किरण दी। मन नाच उठा। उन्होंने बहुत शान्त चित्त से सूरिजी के प्रवचन सुने। लोक मारवाड़ी में अत्यन्त निष्कपट निश्छल प्रवचनों ने उनके भीतर की आँखें उघाड़ दीं। उन्हें अहसास हुआ कि जिस गंगा की तलाश में वे थे, वह स्वयं उनके द्वार खड़ी है। मन उमंगों में झूम उठा । लगा जैसे भीतर बैठा कोई तपस्वी आँखें मसल रहा है और एक सूरज को ऊगता देख रहा है। रत्नराज को अनुभव हुआ जैसे कोई अमावस्या गुजर गयी है और सवेरे के नरम सूरज की ऊनी किरणे उनके चित्त को ताजा कर रही हैं। उन्होंने कुटुम्बियों से विचार-विमर्श किया और सूरिजी से यति-दीक्षा के लिए विनयपूर्ण निवेदन किया। सूरिजी ने देखा कि रत्नराज के रूप में भारतीय संस्कृति के क्षितिज पर एक नये नक्षत्र का उदय हो रहा है, जो अन्धकार को हटायेगा और प्रकाश का प्रसार करेगा । वे मन ही मन उल्लसित हुए । उनके चित्त के आँगन में मानो श्रमण संस्कृति के किसी उज्ज्वल भविष्य ने अलीपन किया हो, मंगल घट की स्थापना की हो। सूरिजी ने उत्तर दिया : “रत्नराज, मैं तो यह काम नहीं कर सकूँगा, किन्तु उदयपुर में मेरे गुरुभाई हेमविजयजी हैं, वे तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध कर सकेंगे।" रत्नराज का संकल्प अविचल था। वे तुरन्त निकल पड़े और १८४६ ई. में उन्होंने यतिदीक्षा ले ली।
तीर्थकर : जून १९७५/८०
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org