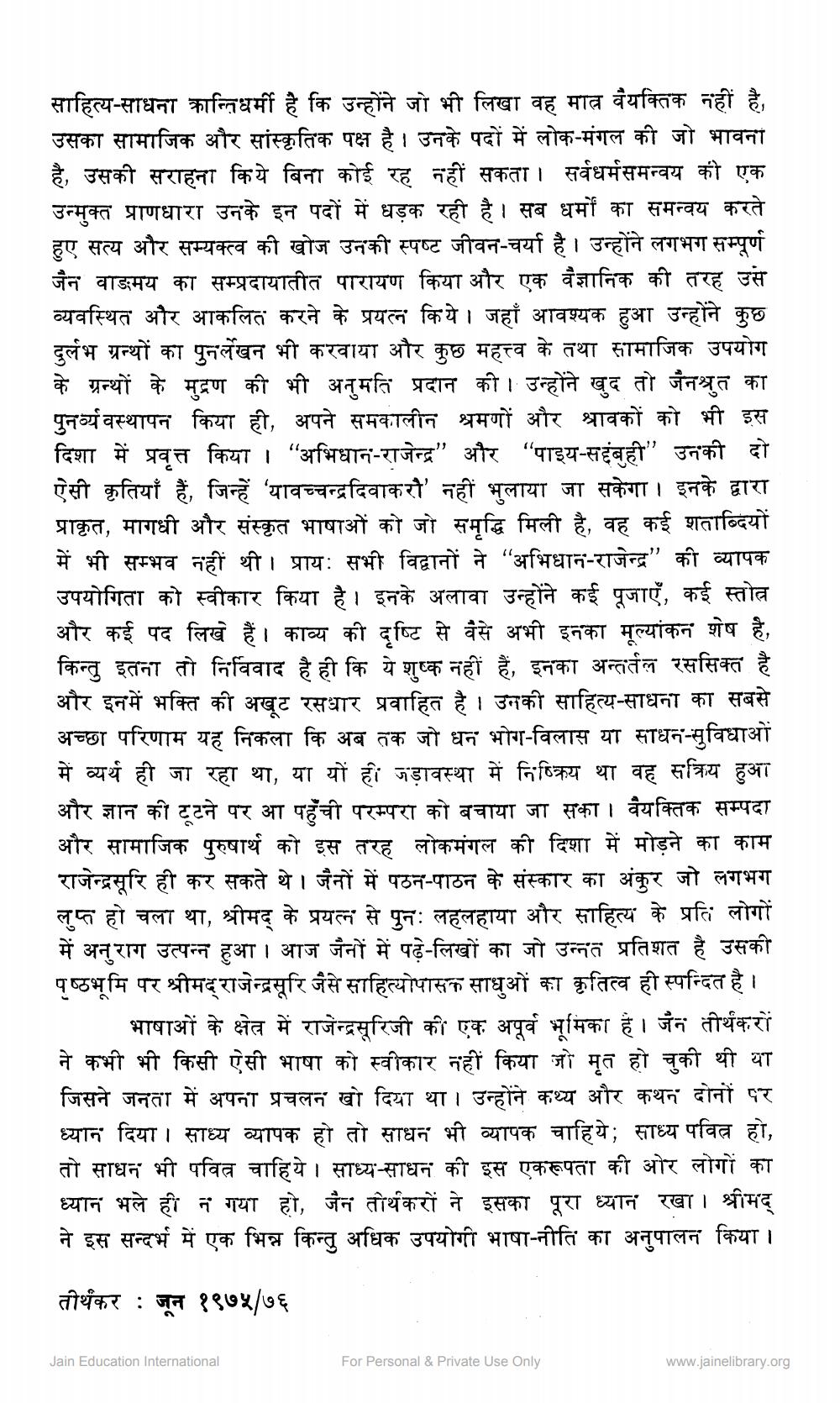________________
साहित्य-साधना कान्तिधर्मी है कि उन्होंने जो भी लिखा वह मात्र वैयक्तिक नहीं है, उसका सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष है। उनके पदों में लोक-मंगल की जो भावना है, उसकी सराहना किये बिना कोई रह नहीं सकता। सर्वधर्मसमन्वय की एक उन्मुक्त प्राणधारा उनके इन पदों में धड़क रही है। सब धर्मों का समन्वय करते हुए सत्य और सम्यक्त्व की खोज उनकी स्पष्ट जीवन-चर्या है। उन्होंने लगभग सम्पूर्ण जैन वाङमय का सम्प्रदायातीत पारायण किया और एक वैज्ञानिक की तरह उसे व्यवस्थित और आकलित करने के प्रयत्न किये। जहाँ आवश्यक हुआ उन्होंने कुछ दुर्लभ ग्रन्थों का पुनर्लेखन भी करवाया और कुछ महत्त्व के तथा सामाजिक उपयोग के ग्रन्थों के मुद्रण की भी अनुमति प्रदान की। उन्होंने खुद तो जनश्रुत का पुनर्व्यवस्थापन किया ही, अपने समकालीन श्रमणों और श्रावकों को भी इस दिशा में प्रवृत्त किया । “अभिधान-राजेन्द्र" और "पाइय-सदंबही' उनकी दो ऐसी कृतियाँ हैं, जिन्हें ‘यावच्चन्द्रदिवाकरौ' नहीं भुलाया जा सकेगा। इनके द्वारा प्राकृत, मागधी और संस्कृत भाषाओं को जो समृद्धि मिली है, वह कई शताब्दियों में भी सम्भव नहीं थी। प्रायः सभी विद्वानों ने “अभिधान-राजेन्द्र" की व्यापक उपयोगिता को स्वीकार किया है। इनके अलावा उन्होंने कई पूजाएँ, कई स्तोत्र
और कई पद लिखे हैं। काव्य की दृष्टि से वैसे अभी इनका मूल्यांकन शेष है, किन्तु इतना तो निर्विवाद है ही कि ये शुष्क नहीं हैं, इनका अन्तर्तल रससिक्त है
और इनमें भक्ति की अखूट रसधार प्रवाहित है। उनकी साहित्य-साधना का सबसे अच्छा परिणाम यह निकला कि अब तक जो धन भोग-विलास या साधन-सुविधाओं में व्यर्थ ही जा रहा था, या यों ही जड़ावस्था में निष्क्रिय था वह सत्रिय हुआ और ज्ञान की टूटने पर आ पहुँची परम्परा को बचाया जा सका। वैयक्तिक सम्पदा और सामाजिक पुरुषार्थ को इस तरह लोकमंगल की दिशा में मोड़ने का काम राजेन्द्रसूरि ही कर सकते थे। जैनों में पठन-पाठन के संस्कार का अंकूर जो लगभग लुप्त हो चला था, श्रीमद् के प्रयत्न से पुनः लहलहाया और साहित्य के प्रति लोगों में अनुराग उत्पन्न हुआ। आज जैनों में पढ़े-लिखों का जो उन्नत प्रतिशत है उसकी पृष्ठभूमि पर श्रीमद्रराजेन्द्रसूरि जैसे साहित्योपासक साधुओं का कृतित्व ही स्पन्दित है।
भाषाओं के क्षेत्र में राजेन्द्रसूरिजी की एक अपूर्व भूमिका है। जैन तीर्थंकरों ने कभी भी किसी ऐसी भाषा को स्वीकार नहीं किया जो मृत हो चुकी थी या जिसने जनता में अपना प्रचलन खो दिया था। उन्होंने कथ्य और कथन दोनों पर ध्यान दिया। साध्य व्यापक हो तो साधन भी व्यापक चाहिये; साध्य पवित्र हो, तो साधन भी पवित्र चाहिये। साध्य-साधन की इस एकरूपता की ओर लोगों का ध्यान भले ही न गया हो, जैन तीर्थकरों ने इसका पूरा ध्यान रखा। श्रीमद् ने इस सन्दर्भ में एक भिन्न किन्तु अधिक उपयोगी भाषा-नीति का अनुपालन किया।
तीर्थंकर : जून १९७५/७६
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org