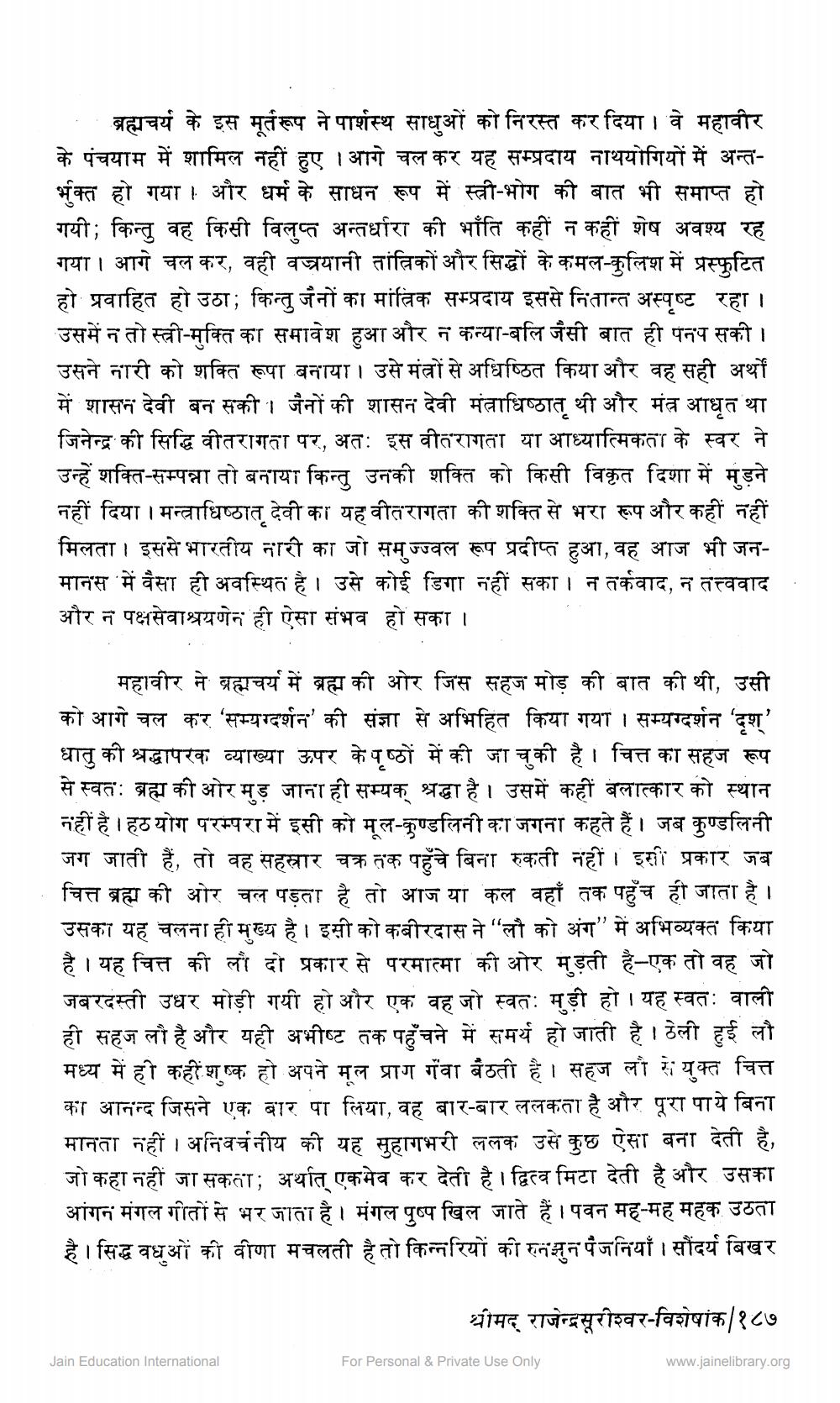________________
ब्रह्मचर्य के इस मूर्तरूप ने पार्शस्थ साधुओं को निरस्त कर दिया। वे महावीर के पंचयाम में शामिल नहीं हुए । आगे चल कर यह सम्प्रदाय नाथयोगियों में अन्तभुक्त हो गया। और धर्म के साधन रूप में स्त्री-भोग की बात भी समाप्त हो गयी; किन्तु वह किसी विलुप्त अन्तर्धारा की भाँति कहीं न कहीं शेष अवश्य रह गया। आगे चल कर, वही वज्रयानी तांत्रिकों और सिद्धों के कमल-कुलिश में प्रस्फुटित हो प्रवाहित हो उठा; किन्तु जैनों का मांत्रिक सम्प्रदाय इससे नितान्त अस्पृष्ट रहा । उसमें न तो स्त्री-मक्ति का समावेश हुआ और न कन्या-बलि जैसी बात ही पनप सकी। उसने नारी को शक्ति रूपा बनाया। उसे मंत्रों से अधिष्ठित किया और वह सही अर्थों में शासन देवी बन सकी। जैनों की शासन देवी मंत्राधिष्ठात थी और मंत्र आधृत था जिनेन्द्र की सिद्धि वीतरागता पर, अत: इस वीतरागता या आध्यात्मिकता के स्वर ने उन्हें शक्ति-सम्पन्ना तो बनाया किन्तु उनकी शक्ति को किसी विकृत दिशा में मुड़ने नहीं दिया । मन्त्राधिष्ठात देवी का यह वीतरागता की शक्ति से भरा रूप और कहीं नहीं मिलता। इससे भारतीय नारी का जो समुज्ज्वल रूप प्रदीप्त हुआ, वह आज भी जनमानस में वैसा ही अवस्थित है। उसे कोई डिगा नहीं सका। न तर्कवाद, न तत्त्ववाद और न पक्षसेवाश्रयणेन ही ऐसा संभव हो सका ।
महावीर ने ब्रह्मचर्य में ब्रह्म की ओर जिस सहज मोड़ की बात की थी, उसी को आगे चल कर 'सम्यग्दर्शन' की संज्ञा से अभिहित किया गया । सम्यग्दर्शन 'दृश्' धातु की श्रद्धापरक व्याख्या ऊपर के पृष्ठों में की जा चुकी है। चित्त का सहज रूप से स्वतः ब्रह्म की ओर मुड़ जाना ही सम्यक् श्रद्धा है। उसमें कहीं बलात्कार को स्थान नहीं है। हठ योग परम्परा में इसी को मूल-कुण्डलिनी का जगना कहते हैं। जब कुण्डलिनी जग जाती हैं, तो वह सहस्रार चक्र तक पहँचे बिना रुकती नहीं। इसी प्रकार जब चित्त ब्रह्म की ओर चल पड़ता है तो आज या कल वहाँ तक पहुँच ही जाता है। उसका यह चलना ही मख्य है। इसी को कबीरदास ने “लौ को अंग" में अभिव्यक्त किया है। यह चित्त की लौ दो प्रकार से परमात्मा की ओर मुड़ती है-एक तो वह जो जबरदस्ती उधर मोड़ी गयी हो और एक वह जो स्वतः मुड़ी हो । यह स्वत: वाली ही सहज लौ है और यही अभीष्ट तक पहुँचने में समर्थ हो जाती है। ठेली हुई लौ मध्य में ही कहीं शुष्क हो अपने मल प्राग गंवा बैठती है। सहज लौ से युक्त चित्त का आनन्द जिसने एक बार पा लिया, वह बार-बार ललकता है और पूरा पाये बिना मानता नहीं । अनिवर्चनीय की यह सुहागभरी ललक उसे कुछ ऐसा बना देती है, जो कहा नहीं जा सकता; अर्थात् एकमेव कर देती है। द्वित्व मिटा देती है और उसका आंगन मंगल गीतों से भर जाता है। मंगल पुष्प खिल जाते हैं। पवन मह-मह महक उठता है। सिद्ध वधुओं की वीणा मचलती है तो किन्नरियों की रुनझुन पैजनियाँ । सौंदर्य बिखर
श्रीमद राजेन्द्रसूरीश्वर-विशेषांक/१८७
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org