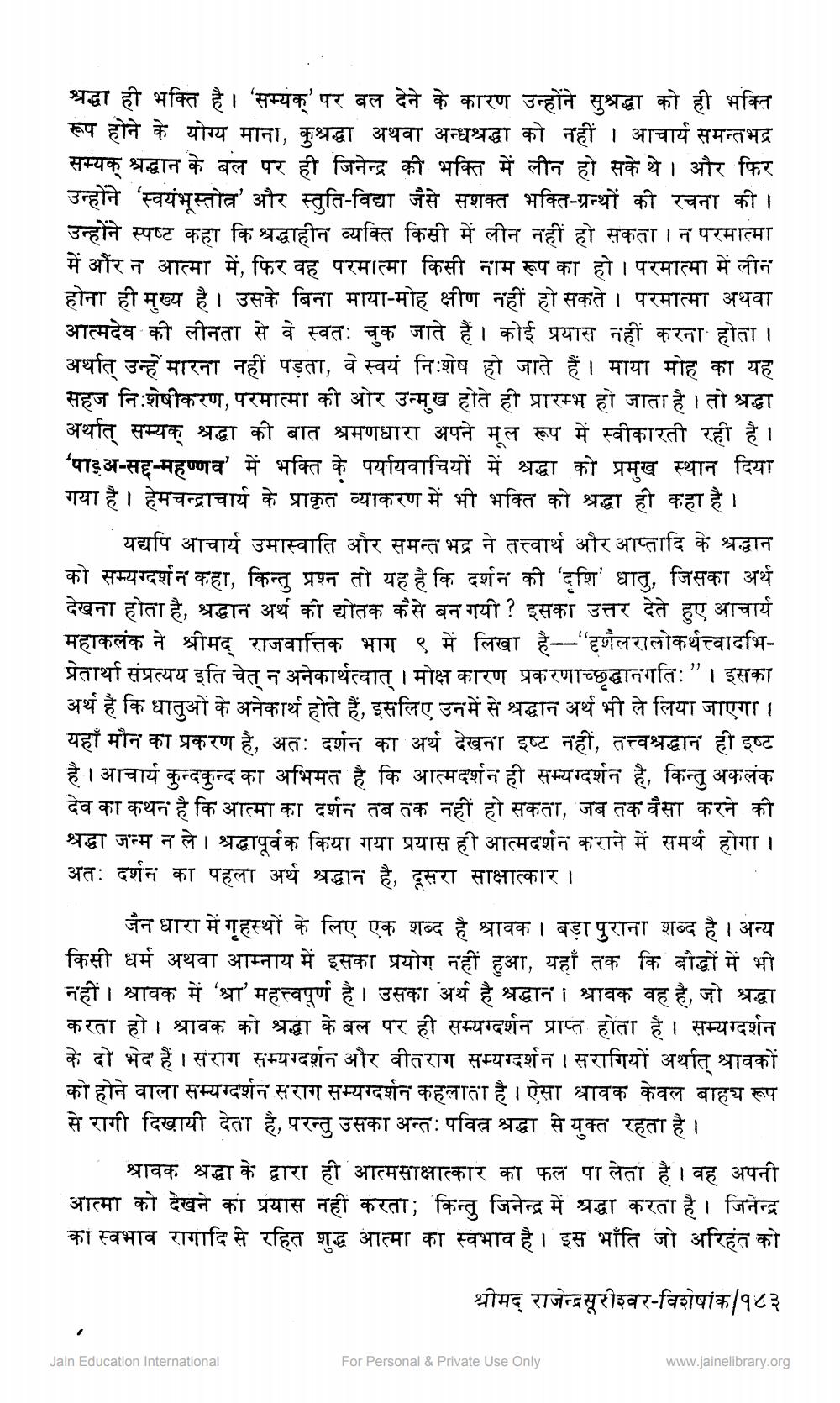________________
श्रद्धा ही भक्ति है। 'सम्यक्' पर बल देने के कारण उन्होंने सुश्रद्धा को ही भक्ति रूप होने के योग्य माना, कुश्रद्धा अथवा अन्धश्रद्धा को नहीं । आचार्य समन्तभद्र सम्यक् श्रद्धान के बल पर ही जिनेन्द्र की भक्ति में लीन हो सके थे। और फिर उन्होंने 'स्वयंभूस्तोत्र' और स्तुति-विद्या जैसे सशक्त भक्ति-ग्रन्थों की रचना की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि श्रद्धाहीन व्यक्ति किसी में लीन नहीं हो सकता । न परमात्मा में और न आत्मा में, फिर वह परमात्मा किसी नाम रूप का हो । परमात्मा में लीन होना ही मुख्य है। उसके बिना माया-मोह क्षीण नहीं हो सकते। परमात्मा अथवा आत्मदेव की लीनता से वे स्वतः चुक जाते हैं। कोई प्रयास नहीं करना होता । अर्थात् उन्हें मारना नहीं पड़ता, वे स्वयं निःशेष हो जाते हैं। माया मोह का यह सहज निःशेषीकरण, परमात्मा की ओर उन्मुख होते ही प्रारम्भ हो जाता है । तो श्रद्धा अर्थात् सम्यक् श्रद्धा की बात श्रमणधारा अपने मूल रूप में स्वीकारती रही है। 'पाइ.अ-सह-महण्णव' में भक्ति के पर्यायवाचियों में श्रद्धा को प्रमुख स्थान दिया गया है। हेमचन्द्राचार्य के प्राकृत व्याकरण में भी भक्ति को श्रद्धा ही कहा है।
यद्यपि आचार्य उमास्वाति और समन्त भद्र ने तत्त्वार्थ और आप्तादि के श्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहा, किन्तु प्रश्न तो यह है कि दर्शन की 'दशि' धातु, जिसका अर्थ देखना होता है, श्रद्धान अर्थ की द्योतक कैसे बन गयी? इसका उत्तर देते हुए आचार्य महाकलंक ने श्रीमद् राजवात्तिक भाग ९ में लिखा है--"दृशैलरालोकर्थत्त्वादभिप्रेतार्था संप्रत्यय इति चेत् न अनेकार्थत्वात् । मोक्ष कारण प्रकरणाच्छ्रद्धानगति:"। इसका अर्थ है कि धातुओं के अनेकार्थ होते हैं, इसलिए उनमें से श्रद्धान अर्थ भी ले लिया जाएगा । यहाँ मौन का प्रकरण है, अतः दर्शन का अर्थ देखना इष्ट नहीं, तत्त्वश्रद्धान' ही इष्ट है । आचार्य कुन्दकुन्द का अभिमत है कि आत्मदर्शन ही सम्यग्दर्शन है, किन्तु अकलंक देव का कथन है कि आत्मा का दर्शन तब तक नहीं हो सकता, जब तक वैसा करने की श्रद्धा जन्म न ले। श्रद्धापूर्वक किया गया प्रयास ही आत्मदर्शन कराने में समर्थ होगा। अतः दर्शन का पहला अर्थ श्रद्धान है, दूसरा साक्षात्कार ।
__ जैन धारा में गृहस्थों के लिए एक शब्द है श्रावक । बड़ा पुराना शब्द है । अन्य किसी धर्म अथवा आम्नाय में इसका प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ तक कि बौद्धों में भी नहीं। श्रावक में 'श्रा' महत्त्वपूर्ण है। उसका अर्थ है श्रद्धान । श्रावक वह है, जो श्रद्धा करता हो। श्रावक को श्रद्धा के बल पर ही सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है। सम्यग्दर्शन के दो भेद हैं । सराग सम्यग्दर्शन और वीतराग सम्यग्दर्शन । सरागियों अर्थात् श्रावकों को होने वाला सम्यग्दर्शन सराग सम्यग्दर्शन कहलाता है। ऐसा श्रावक केवल बाह्य रूप से रागी दिखायी देता है, परन्तु उसका अन्तः पवित्र श्रद्धा से युक्त रहता है।
श्रावक श्रद्धा के द्वारा ही आत्मसाक्षात्कार का फल पा लेता है। वह अपनी आत्मा को देखने का प्रयास नहीं करता; किन्तु जिनेन्द्र में श्रद्धा करता है। जिनेन्द्र का स्वभाव रागादि से रहित शुद्ध आत्मा का स्वभाव है। इस भाँति जो अरिहंत को
श्रीमद् राजेन्द्रसूरीश्वर-विशेषांक/१८३
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org