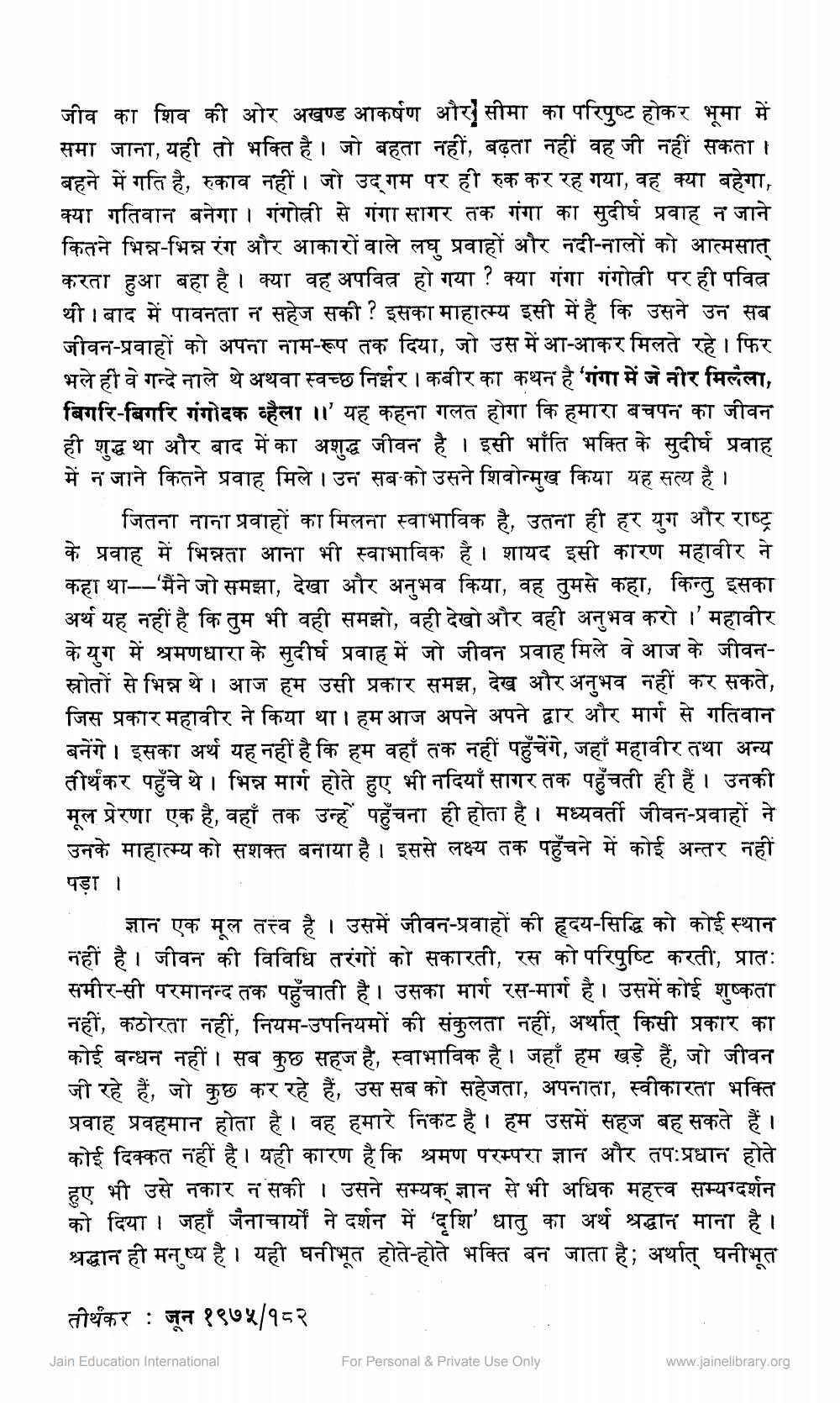________________
जीव का शिव की ओर अखण्ड आकर्षण और सीमा का परिपुष्ट होकर भूमा में समा जाना, यही तो भक्ति है। जो बहता नहीं, बढ़ता नहीं वह जी नहीं सकता। बहने में गति है, रुकाव नहीं। जो उद्गम पर ही रुक कर रह गया, वह क्या बहेगा, क्या गतिवान बनेगा। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा का सुदीर्घ प्रवाह न जाने कितने भिन्न-भिन्न रंग और आकारों वाले लघु प्रवाहों और नदी-नालों को आत्मसात् करता हुआ बहा है। क्या वह अपवित्र हो गया ? क्या गंगा गंगोत्री पर ही पवित्र थी। बाद में पावनता न सहेज सकी ? इसका माहात्म्य इसी में है कि उसने उन सब जीवन-प्रवाहों को अपना नाम-रूप तक दिया, जो उस में आ-आकर मिलते रहे। फिर भले ही वे गन्दे नाले थे अथवा स्वच्छ निर्झर । कबीर का कथन है 'गंगा में जे नीर मिलेला, बिगरि-बिगरि गंगोदक व्हैला ॥' यह कहना गलत होगा कि हमारा बचपन का जीवन ही शुद्ध था और बाद में का अशुद्ध जीवन है । इसी भाँति भक्ति के सुदीर्घ प्रवाह में न जाने कितने प्रवाह मिले। उन सब को उसने शिवोन्मुख किया यह सत्य है ।
जितना नाना प्रवाहों का मिलना स्वाभाविक है, उतना ही हर युग और राष्ट्र के प्रवाह में भिन्नता आना भी स्वाभाविक है। शायद इसी कारण महावीर ने कहा था--'मैंने जो समझा, देखा और अनुभव किया, वह तुमसे कहा, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम भी वही समझो, वही देखो और वही अनुभव करो ।' महावीर के युग में श्रमणधारा के सुदीर्घ प्रवाह में जो जीवन' प्रवाह मिले वे आज के जीवनस्रोतों से भिन्न थे। आज हम उसी प्रकार समझ, देख और अनुभव नहीं कर सकते, जिस प्रकार महावीर ने किया था। हम आज अपने अपने द्वार और मार्ग से गतिवान बनेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, जहाँ महावीर तथा अन्य तीर्थंकर पहुँचे थे। भिन्न मार्ग होते हुए भी नदियाँ सागर तक पहुँचती ही हैं। उनकी मूल प्रेरणा एक है, वहाँ तक उन्हें पहुँचना ही होता है। मध्यवर्ती जीवन-प्रवाहों ने उनके माहात्म्य को सशक्त बनाया है। इससे लक्ष्य तक पहुँचने में कोई अन्तर नहीं पड़ा ।
ज्ञान एक मूल तत्त्व है। उसमें जीवन-प्रवाहों की हृदय-सिद्धि को कोई स्थान नहीं है। जीवन की विविधि तरंगों को सकारती, रस को परिपुष्टि करती, प्रातः समीर-सी परमानन्द तक पहुँचाती है। उसका मार्ग रस-मार्ग है। उसमें कोई शुष्कता नहीं, कठोरता नहीं, नियम-उपनियमों की संकुलता नहीं, अर्थात् किसी प्रकार का कोई बन्धन नहीं। सब कुछ सहज है, स्वाभाविक है। जहाँ हम खड़े हैं, जो जीवन जी रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उस सब को सहेजता, अपनाता, स्वीकारता भक्ति प्रवाह प्रवहमान होता है। वह हमारे निकट है। हम उसमें सहज बह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यही कारण है कि श्रमण परम्परा ज्ञान और तपःप्रधान होते हए भी उसे नकार न सकी । उसने सम्यक ज्ञान से भी अधिक महत्त्व सम्यग्दर्शन को दिया। जहाँ जैनाचार्यों ने दर्शन में 'दृशि' धातु का अर्थ श्रद्धान माना है। श्रद्धान ही मनुष्य है। यही घनीभूत होते-होते भक्ति बन जाता है; अर्थात् घनीभूत
तीर्थंकर : जून १९७५/१८२
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org