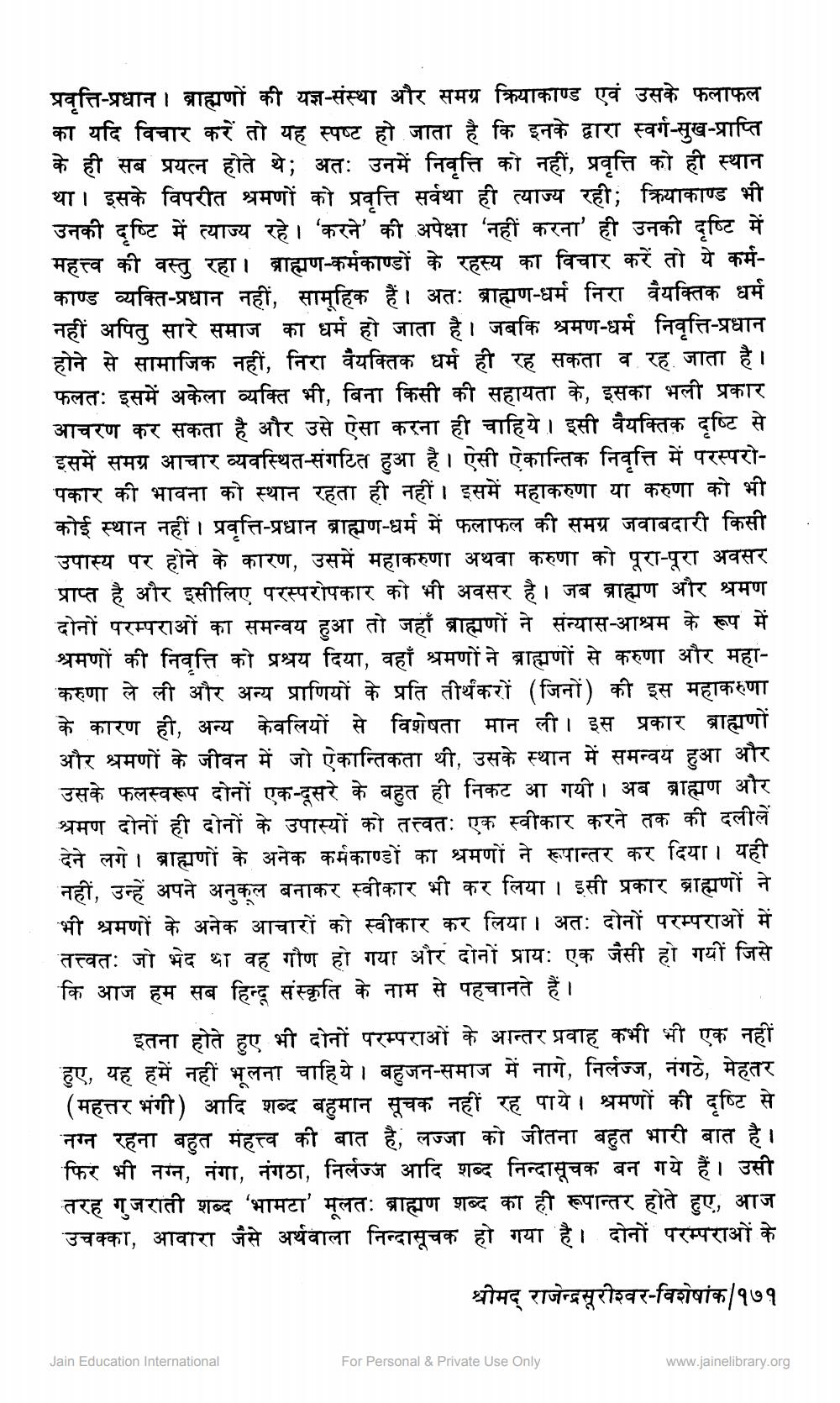________________
प्रवृत्ति-प्रधान। ब्राह्मणों की यज्ञ-संस्था और समग्र क्रियाकाण्ड एवं उसके फलाफल का यदि विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इनके द्वारा स्वर्ग-सुख-प्राप्ति के ही सब प्रयत्न होते थे; अतः उनमें निवृत्ति को नहीं, प्रवृत्ति को ही स्थान था। इसके विपरीत श्रमणों को प्रवृत्ति सर्वथा ही त्याज्य रही; क्रियाकाण्ड भी उनकी दृष्टि में त्याज्य रहे। ‘करने' की अपेक्षा नहीं करना' ही उनकी दृष्टि में महत्त्व की वस्तु रहा। ब्राह्मण-कर्मकाण्डों के रहस्य का विचार करें तो ये कर्मकाण्ड व्यक्ति-प्रधान नहीं, सामूहिक हैं। अतः ब्राह्मण-धर्म निरा वैयक्तिक धर्म नहीं अपितु सारे समाज का धर्म हो जाता है। जबकि श्रमण-धर्म निवृत्ति-प्रधान होने से सामाजिक नहीं, निरा वैयक्तिक धर्म ही रह सकता व रह जाता है। फलतः इसमें अकेला व्यक्ति भी, बिना किसी की सहायता के, इसका भली प्रकार आचरण कर सकता है और उसे ऐसा करना ही चाहिये। इसी वैयक्तिक दृष्टि से इसमें समग्र आचार व्यवस्थित-संगटित हुआ है। ऐसी ऐकान्तिक निवृत्ति में परस्परोपकार की भावना को स्थान रहता ही नहीं। इसमें महाकरुणा या करुणा को भी कोई स्थान नहीं। प्रवृत्ति-प्रधान ब्राह्मण-धर्म में फलाफल की समग्र जवाबदारी किसी उपास्य पर होने के कारण, उसमें महाकरुणा अथवा करुणा को पूरा-पूरा अवसर प्राप्त है और इसीलिए परस्परोपकार को भी अवसर है। जब ब्राह्मण और श्रमण दोनों परम्पराओं का समन्वय हुआ तो जहाँ ब्राह्मणों ने संन्यास-आश्रम के रूप में श्रमणों की निवृत्ति को प्रश्रय दिया, वहाँ श्रमणों ने ब्राह्मणों से करुणा और महाकरुणा ले ली और अन्य प्राणियों के प्रति तीर्थंकरों (जिनों) की इस महाकरुणा के कारण ही, अन्य केवलियों से विशेषता मान ली। इस प्रकार ब्राह्मणों और श्रमणों के जीवन में जो ऐकान्तिकता थी, उसके स्थान में समन्वय हुआ और उसके फलस्वरूप दोनों एक-दूसरे के बहुत ही निकट आ गयी। अब ब्राह्मण और श्रमण दोनों ही दोनों के उपास्यों को तत्त्वतः एक स्वीकार करने तक की दलीलें देने लगे। ब्राह्मणों के अनेक कर्मकाण्डों का श्रमणों ने रूपान्तर कर दिया। यही नहीं, उन्हें अपने अनुकूल बनाकर स्वीकार भी कर लिया। इसी प्रकार ब्राह्मणों ने भी श्रमणों के अनेक आचारों को स्वीकार कर लिया। अतः दोनों परम्पराओं में तत्त्वतः जो भेद था वह गौण हो गया और दोनों प्राय: एक जैसी हो गयीं जिसे कि आज हम सब हिन्दू संस्कृति के नाम से पहचानते हैं।
इतना होते हुए भी दोनों परम्पराओं के आन्तर प्रवाह कभी भी एक नहीं हुए, यह हमें नहीं भूलना चाहिये। बहुजन-समाज में नागे, निर्लज्ज, नंगठे, मेहतर (महत्तर भंगी) आदि शब्द बहुमान सूचक नहीं रह पाये। श्रमणों की दृष्टि से नग्न रहना बहुत महत्त्व की बात है, लज्जा को जीतना बहुत भारी बात है। फिर भी नग्न, नंगा, नंगठा, निर्लज्ज आदि शब्द निन्दासूचक बन गये हैं। उसी तरह गुजराती शब्द 'भामटा' मूलत: ब्राह्मण शब्द का ही रूपान्तर होते हुए, आज उचक्का, आवारा जैसे अर्थवाला निन्दासूचक हो गया है। दोनों परम्पराओं के
श्रीमद् राजेन्द्रसूरीश्वर-विशेषांक/१७१
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org