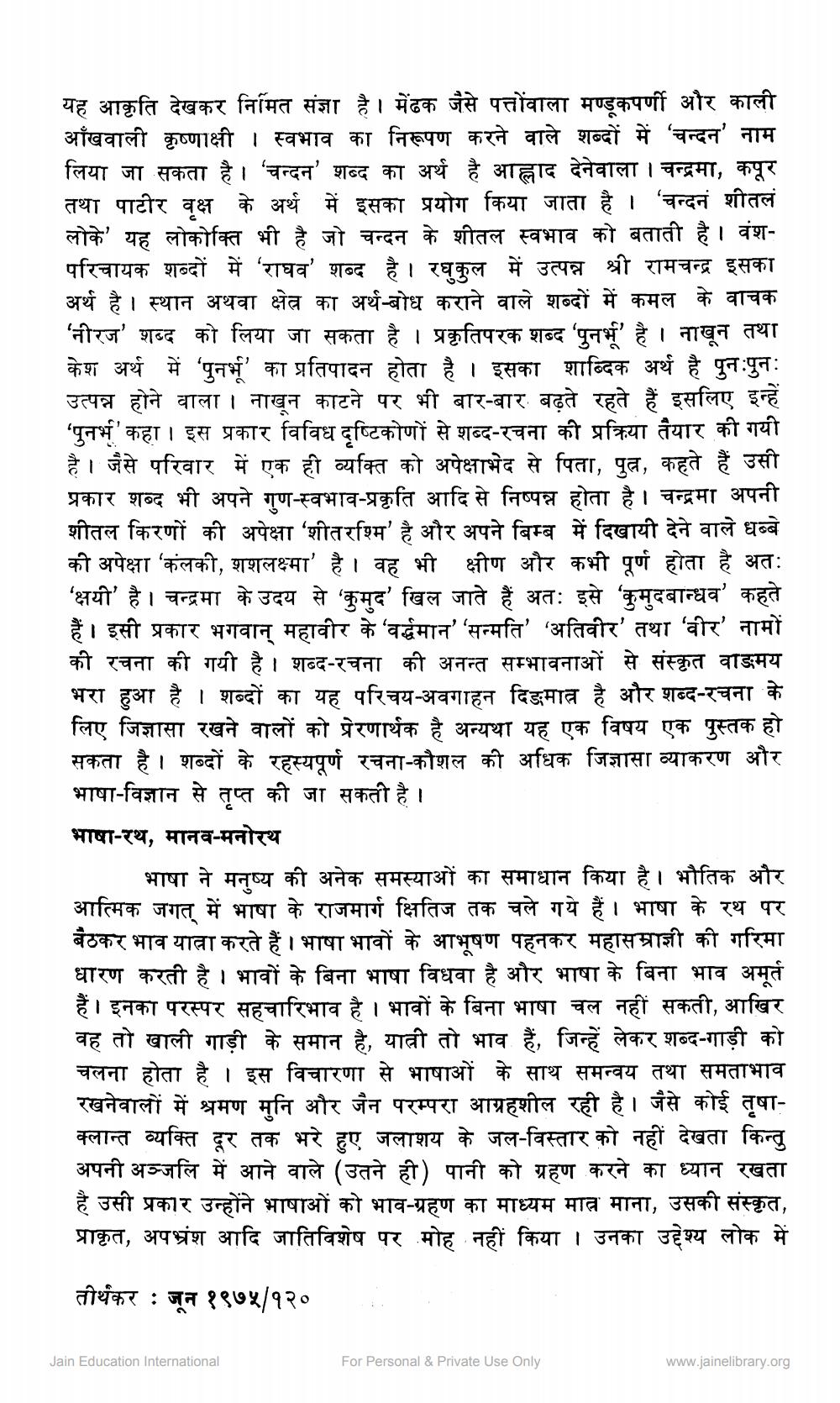________________
यह आकृति देखकर निर्मित संज्ञा है। मेंढक जैसे पत्तोंवाला मण्डूकपर्णी और काली
आँखवाली कृष्णाक्षी । स्वभाव का निरूपण करने वाले शब्दों में 'चन्दन' नाम लिया जा सकता है। 'चन्दन' शब्द का अर्थ है आह्लाद देनेवाला । चन्द्रमा, कपूर तथा पाटीर वृक्ष के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है । 'चन्दनं शीतलं लोके' यह लोकोक्ति भी है जो चन्दन के शीतल स्वभाव को बताती है। वंशपरिचायक शब्दों में 'राघव' शब्द है। रघुकुल में उत्पन्न श्री रामचन्द्र इसका अर्थ है। स्थान अथवा क्षेत्र का अर्थ-बोध कराने वाले शब्दों में कमल के वाचक 'नीरज' शब्द को लिया जा सकता है । प्रकृतिपरक शब्द 'पुनर्भू' है । नाखून तथा केश अर्थ में 'पुनर्भू' का प्रतिपादन होता है । इसका शाब्दिक अर्थ है पुनःपुनः उत्पन्न होने वाला । नाखून काटने पर भी बार-बार बढ़ते रहते हैं इसलिए इन्हें 'पुनर्भ' कहा। इस प्रकार विविध दृष्टिकोणों से शब्द-रचना की प्रक्रिया तैयार की गयी है। जैसे परिवार में एक ही व्यक्ति को अपेक्षाभेद से पिता, पुत्र, कहते हैं उसी प्रकार शब्द भी अपने गुण-स्वभाव-प्रकृति आदि से निष्पन्न होता है। चन्द्रमा अपनी शीतल किरणों की अपेक्षा 'शीतरश्मि' है और अपने बिम्ब में दिखायी देने वाले धब्बे की अपेक्षा 'कंलकी, शशलक्ष्मा' है। वह भी क्षीण और कभी पूर्ण होता है अत: 'क्षयी' है। चन्द्रमा के उदय से 'कुमुद' खिल जाते हैं अतः इसे 'कुमुदबान्धव' कहते हैं। इसी प्रकार भगवान् महावीर के 'वर्द्धमान' 'सन्मति' 'अतिवीर' तथा 'वीर' नामों की रचना की गयी है। शब्द-रचना की अनन्त सम्भावनाओं से संस्कृत वाङमय भरा हुआ है । शब्दों का यह परिचय-अवगाहन दिङमात्र है और शब्द-रचना के लिए जिज्ञासा रखने वालों को प्रेरणार्थक है अन्यथा यह एक विषय एक पुस्तक हो सकता है। शब्दों के रहस्यपूर्ण रचना-कौशल की अधिक जिज्ञासा व्याकरण और भाषा-विज्ञान से तृप्त की जा सकती है। भाषा-रथ, मानव-मनोरथ
भाषा ने मनुष्य की अनेक समस्याओं का समाधान किया है। भौतिक और आत्मिक जगत् में भाषा के राजमार्ग क्षितिज तक चले गये हैं। भाषा के रथ पर बैठकर भाव यात्रा करते हैं। भाषा भावों के आभूषण पहनकर महासम्राज्ञी की गरिमा धारण करती है । भावों के बिना भाषा विधवा है और भाषा के बिना भाव अमूर्त हैं। इनका परस्पर सहचारिभाव है । भावों के बिना भाषा चल नहीं सकती, आखिर वह तो खाली गाड़ी के समान है, यात्री तो भाव हैं, जिन्हें लेकर शब्द-गाड़ी को चलना होता है । इस विचारणा से भाषाओं के साथ समन्वय तथा समताभाव रखनेवालों में श्रमण मुनि और जैन परम्परा आग्रहशील रही है। जैसे कोई तृषाक्लान्त व्यक्ति दूर तक भरे हुए जलाशय के जल-विस्तार को नहीं देखता किन्तु अपनी अञ्जलि में आने वाले (उतने ही) पानी को ग्रहण करने का ध्यान रखता है उसी प्रकार उन्होंने भाषाओं को भाव-ग्रहण का माध्यम मात्र माना, उसकी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि जातिविशेष पर मोह नहीं किया । उनका उद्देश्य लोक में
तीर्थकर : जून १९७५/१२०
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org