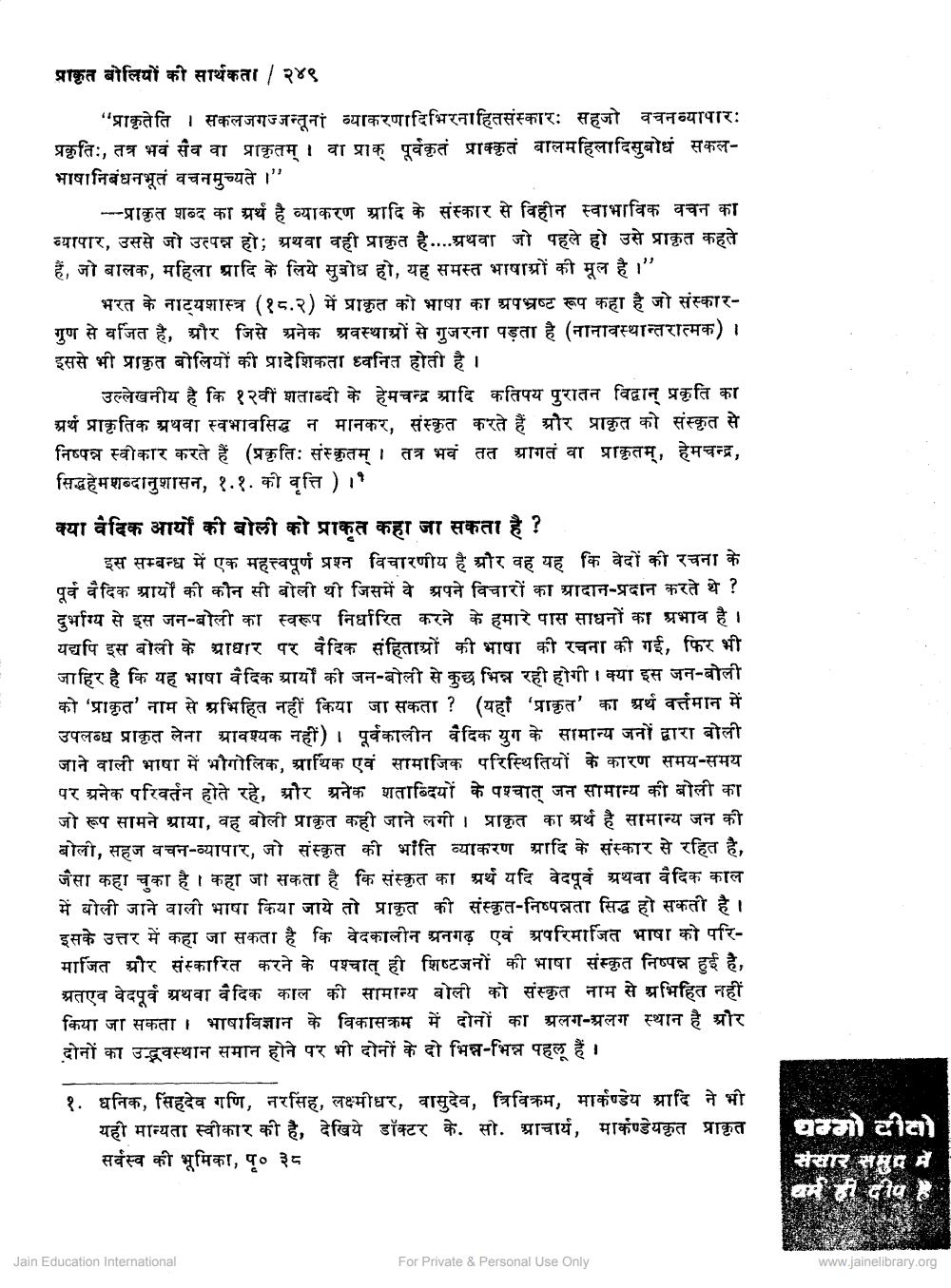________________
प्राकृत बोलियों की सार्थकता | २४९
"प्राकृतेति । सकलजगज्जन्तूनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः सहजो वचनव्यापारः प्रकृतिः, तत्र भवं सैव वा प्राकृतम् । वा प्राक पूर्वकृतं प्राक्कृतं बालमहिलादिसुबोधं सकलभाषानिबंधनभूतं वचनमुच्यते ।"
---प्राकृत शब्द का अर्थ है व्याकरण आदि के संस्कार से विहीन स्वाभाविक वचन का व्यापार, उससे जो उत्पन्न हो; अथवा वही प्राकृत है....अथवा जो पहले हो उसे प्राकृत कहते हैं, जो बालक, महिला प्रादि के लिये सुबोध हो, यह समस्त भाषानों की मूल है।"
भरत के नाट्यशास्त्र (१८.२) में प्राकृत को भाषा का अपभ्रष्ट रूप कहा है जो संस्कारगुण से वजित है, और जिसे अनेक अवस्थानों से गुजरना पड़ता है (नानावस्थान्तरात्मक) । इससे भी प्राकृत बोलियों की प्रादेशिकता ध्वनित होती है।
उल्लेखनीय है कि १२वीं शताब्दी के हेमचन्द्र आदि कतिपय पुरातन विद्वान् प्रकृति का अर्थ प्राकृतिक अथवा स्वभावसिद्ध न मानकर, संस्कृत करते हैं और प्राकृत को संस्कृत से निष्पन्न स्वीकार करते हैं (प्रकृतिः संस्कृतम् । तत्र भवं तत प्रागतं वा प्राकृतम्, हेमचन्द्र, सिद्धहेमशब्दानुशासन, १.१. की वृत्ति )।' क्या वैदिक आर्यों की बोली को प्राकृत कहा जा सकता है ?
इस सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारणीय है और वह यह कि वेदों की रचना के पूर्व वैदिक आर्यो की कौन सी बोली थी जिसमें वे अपने विचारों का आदान-प्रदान करते थे ? दुर्भाग्य से इस जन-बोली का स्वरूप निर्धारित करने के हमारे पास साधनों का प्रभाव है। यद्यपि इस बोली के आधार पर वैदिक संहिताओं की भाषा की रचना की गई, फिर भी जाहिर है कि यह भाषा वैदिक आर्यों की जन-बोली से कुछ भिन्न रही होगी। क्या इस जन-बोली को 'प्राकृत' नाम से अभिहित नहीं किया जा सकता? (यहाँ 'प्राकृत' का अर्थ वर्तमान में उपलब्ध प्राकृत लेना आवश्यक नहीं)। पूर्वकालीन वैदिक युग के सामान्य जनों द्वारा बोली जाने वाली भाषा में भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण समय-समय पर अनेक परिवर्तन होते रहे, और अनेक शताब्दियों के पश्चात् जन सामान्य की बोली का जो रूप सामने पाया, वह बोली प्राकृत कही जाने लगी। प्राकृत का अर्थ है सामान्य जन की बोली, सहज वचन-व्यापार, जो संस्कृत की भांति व्याकरण प्रादि के संस्कार से रहित है, जैसा कहा चुका है। कहा जा सकता है कि संस्कृत का अर्थ यदि वेदपूर्व अथवा वैदिक काल में बोली जाने वाली भाषा किया जाये तो प्राकृत की संस्कृत-निष्पन्नता सिद्ध हो सकती है। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदकालीन अनगढ़ एवं अपरिमाजित भाषा को परिमाजित और संस्कारित करने के पश्चात ही शिष्टजनों की भाषा संस्कृत निष्पन्न हुई है, अतएव वेदपूर्व अथवा वैदिक काल की सामान्य बोली को संस्कृत नाम से अभिहित नहीं किया जा सकता। भाषाविज्ञान के विकासक्रम में दोनों का अलग-अलग स्थान है और दोनों का उद्भवस्थान समान होने पर भी दोनों के दो भिन्न-भिन्न पहल हैं।
१. धनिक, सिंहदेव गणि, नरसिंह, लक्ष्मीधर, वासुदेव, त्रिविक्रम, मार्कण्डेय आदि ने भी
यही मान्यता स्वीकार की है, देखिये डॉक्टर के. सो. प्राचार्य, मार्कण्डेयकृत प्राकृत सर्वस्व की भूमिका, पृ० ३८
घग्गो दीतो संसार समुच में वर्मा दीप
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org