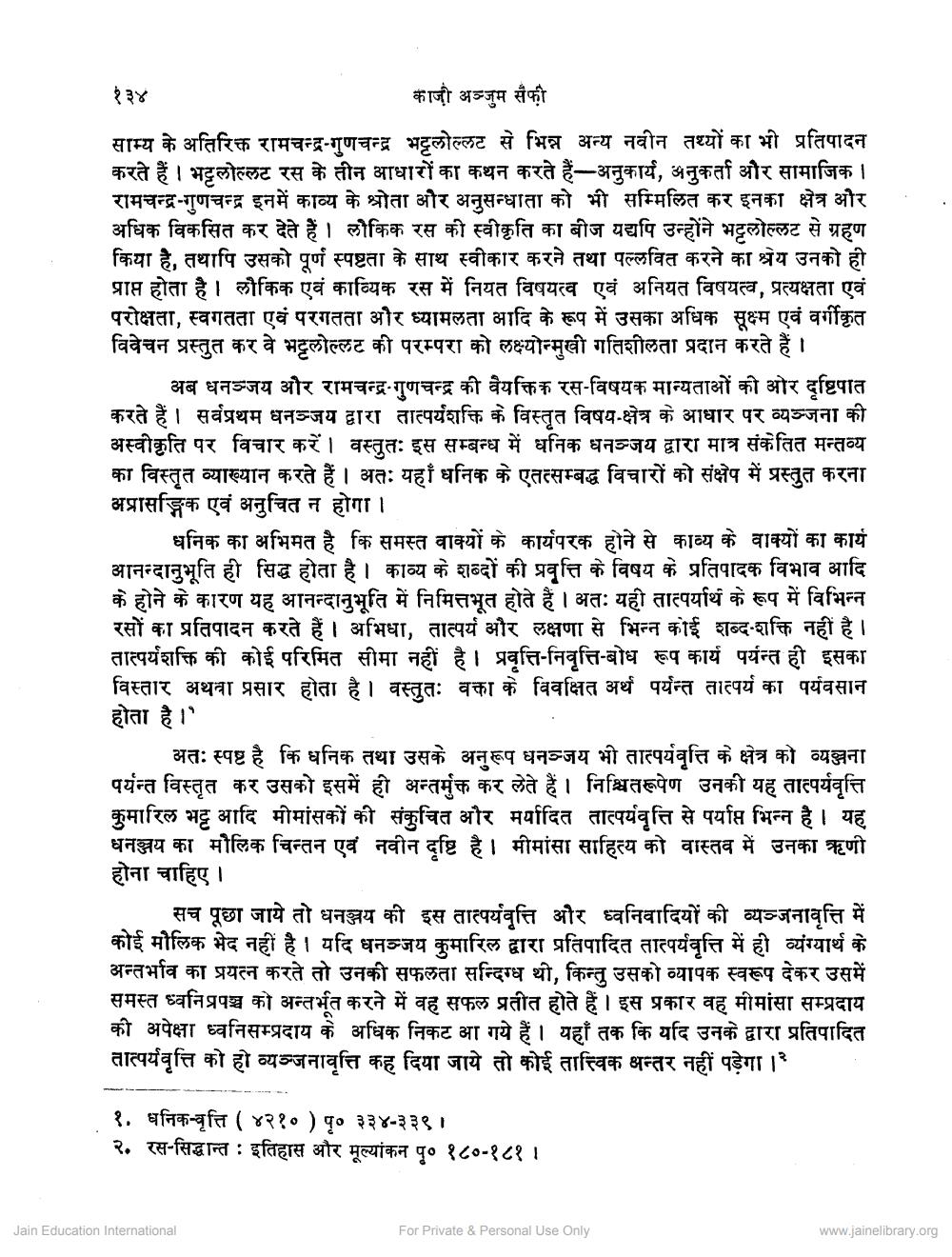________________ 134 काजी अञ्जुम सैफी साम्य के अतिरिक्त रामचन्द्र-गुणचन्द्र भट्टलोल्लट से भिन्न अन्य नवीन तथ्यों का भी प्रतिपादन करते हैं / भट्टलोल्लट रस के तीन आधारों का कथन करते हैं-अनुकार्य, अनुकर्ता और सामाजिक / रामचन्द्र-गुणचन्द्र इनमें काव्य के श्रोता और अनुसन्धाता को भी सम्मिलित कर इनका क्षेत्र और अधिक विकसित कर देते हैं। लौकिक रस की स्वीकृति का बीज यद्यपि उन्होंने भट्टलोल्लट से ग्रहण किया है, तथापि उसको पूर्ण स्पष्टता के साथ स्वीकार करने तथा पल्लवित करने का श्रेय उनको ही प्राप्त होता है। लौकिक एवं काव्यिक रस में नियत विषयत्व एवं अनियत विषयत्व, प्रत्यक्षता एवं परोक्षता, स्वगतता एवं परगतता और ध्यामलता आदि के रूप में उसका अधिक सूक्ष्म एवं वर्गीकृत विवेचन प्रस्तुत कर वे भट्टलोल्लट की परम्परा को लक्ष्योन्मुखी गतिशीलता प्रदान करते हैं / अब धनञ्जय और रामचन्द्र-गुणचन्द्र की वैयक्तिक रस-विषयक मान्यताओं की ओर दृष्टिपात करते हैं। सर्वप्रथम धनञ्जय द्वारा तात्पर्यशक्ति के विस्तृत विषय-क्षेत्र के आधार पर व्यञ्जना की अस्वीकृति पर विचार करें। वस्तुतः इस सम्बन्ध में धनिक धनञ्जय द्वारा मात्र संकेतित मन्तव्य का विस्तृत व्याख्यान करते हैं / अतः यहाँ धनिक के एतत्सम्बद्ध विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना अप्रासङ्गिक एवं अनुचित न होगा। धनिक का अभिमत है कि समस्त वाक्यों के कार्यपरक होने से काव्य के वाक्यों का कार्य आनन्दानुभूति ही सिद्ध होता है। काव्य के शब्दों की प्रवृत्ति के विषय के प्रतिपादक विभाव आदि के होने के कारण यह आनन्दानुभूति में निमित्तभूत होते हैं / अतः यही तात्पर्यार्थ के रूप में विभिन्न रसों का प्रतिपादन करते हैं। अभिधा, तात्पर्य और लक्षणा से भिन्न कोई शब्द-शक्ति नहीं है / तात्पर्यशक्ति की कोई परिमित सीमा नहीं है। प्रवृत्ति-निवृत्ति-बोध रूप कार्य पर्यन्त ही इसका विस्तार अथवा प्रसार होता है। वस्तुतः वक्ता के विवक्षित अर्थ पर्यन्त तात्पर्य का पर्यवसान होता है।' अतः स्पष्ट है कि धनिक तथा उसके अनुरूप धनञ्जय भी तात्पर्यवृत्ति के क्षेत्र को व्यञ्जना पर्यन्त विस्तृत कर उसको इसमें ही अन्तर्मुक्त कर लेते हैं। निश्चितरूपेण उनकी यह तात्पर्यवृत्ति कुमारिल भट्ट आदि मीमांसकों की संकुचित और मर्यादित तात्पर्यवृत्ति से पर्याप्त भिन्न है। यह धनञ्जय का मौलिक चिन्तन एवं नवीन दृष्टि है। मीमांसा साहित्य को वास्तव में उनका ऋणी होना चाहिए। सच पूछा जाये तो धनञ्जय की इस तात्पर्यवृत्ति और ध्वनिवादियों की व्यञ्जनावृत्ति में कोई मौलिक भेद नहीं है / यदि धनञ्जय कुमारिल द्वारा प्रतिपादित तात्पर्यवृत्ति में ही व्यंग्यार्थ के अन्तर्भाव का प्रयत्न करते तो उनकी सफलता सन्दिग्ध थी, किन्तु उसको व्यापक स्वरूप देकर उसमें समस्त ध्वनिप्रपञ्च को अन्तर्भूत करने में वह सफल प्रतीत होते हैं / इस प्रकार वह मीमांसा सम्प्रदाय की अपेक्षा ध्वनिसम्प्रदाय के अधिक निकट आ गये हैं। यहाँ तक कि यदि उनके द्वारा प्रतिपादित तात्पर्यवृत्ति को हो व्यञ्जनावृत्ति कह दिया जाये तो कोई तात्त्विक अन्तर नहीं पड़ेगा।' ------ 1. धनिक-वृत्ति ( 4210 ) पृ० 334-339 / 2. रस-सिद्धान्त : इतिहास और मूल्यांकन पृ० 180-181 / Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org