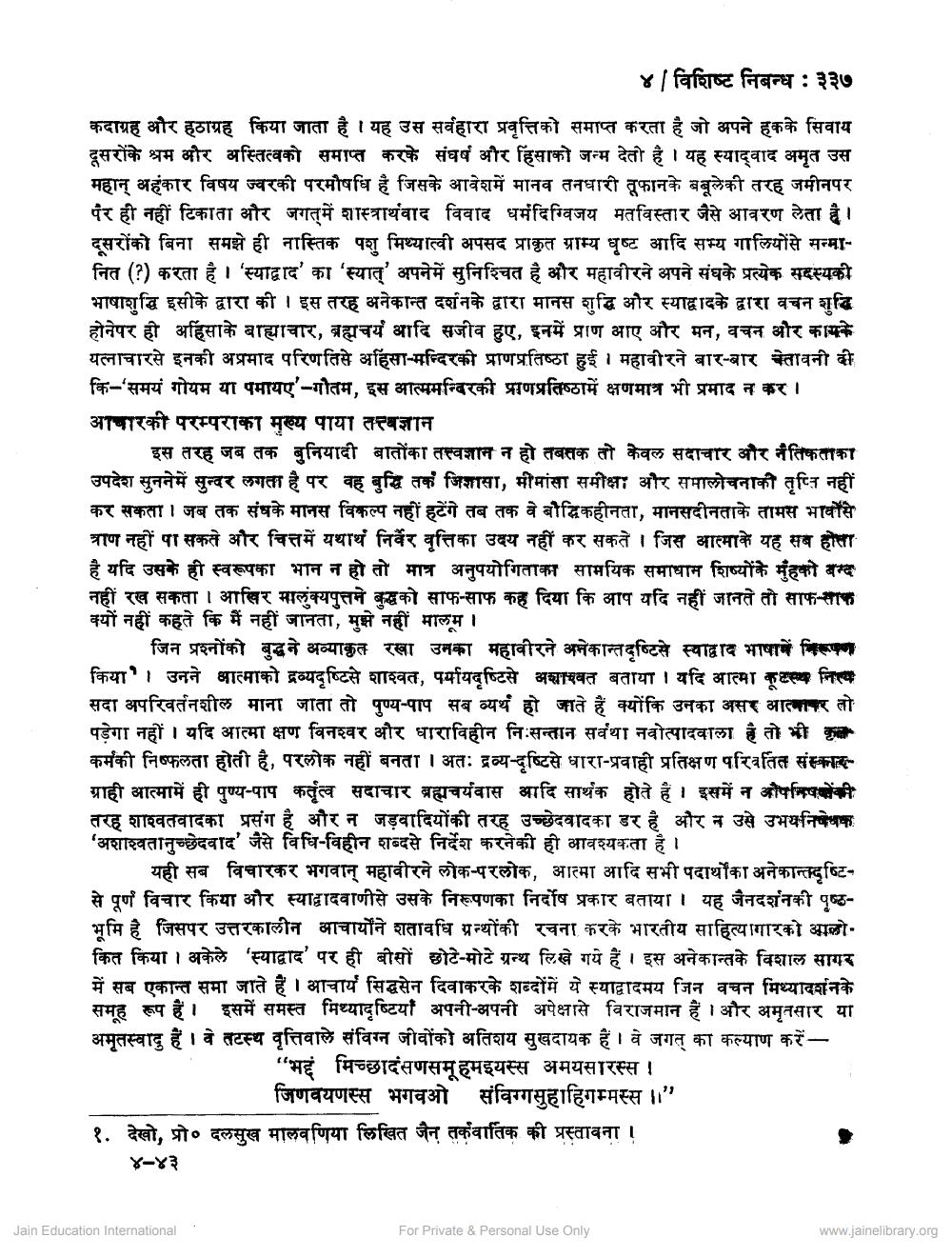________________ ४/विशिष्ट निबन्ध : 337 कदाग्रह और हठाग्रह किया जाता है / यह उस सर्वहारा प्रवृत्तिको समाप्त करता है जो अपने हकके सिवाय दूसरोंके श्रम और अस्तित्वको समाप्त करके संघर्ष और हिंसाको जन्म देती है। यह स्याद्वाद अमृत उस महान् अहंकार विषय ज्वरकी परमौषधि है जिसके आवेशमें मानव तनधारी तूफानके बबूलेकी तरह जमीनपर पर ही नहीं टिकाता और जगतमें शास्त्रार्थवाद विवाद धर्मदिग्विजय मतविस्तार जैसे आवरण लेता है। दूसरोंको बिना समझे ही नास्तिक पशु मिथ्यात्वी अपसद प्राकृत ग्राम्य धृष्ट आदि सभ्य गालियोंसे सन्मानित (?) करता है / 'स्याद्वाद' का 'स्यात्' अपनेमें सुनिश्चित है और महावीरने अपने संघके प्रत्येक सदस्यकी भाषाशद्धि इसीके द्वारा की / इस तरह अनेकान्त दर्शनके द्वारा मानस शुद्धि और स्याद्वादके द्वारा वचन शद्धि होनेपर ही अहिंसाके बाह्याचार, ब्रह्मचर्य आदि सजीव हुए, इनमें प्राण आए और मन, वचन और कायके यत्नाचारसे इनकी अप्रमाद परिणतिसे अहिंसा-मन्दिरकी प्राणप्रतिष्ठा हुई। महावीरने बार-बार चेतावनी दी कि-'समयं गोयम या पमायए'-गौतम, इस आत्ममन्दिरकी प्राणप्रतिष्ठामें क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। आचारकी परम्पराका मुख्य पाया तत्त्वज्ञान इस तरह जब तक बुनियादी बातोंका तत्त्वज्ञान न हो तबतक तो केवल सदाचार और नैतिकताका उपदेश सुनने में सुन्दर लगता है पर वह बुद्धि तक जिज्ञासा, मीमांसा समीक्षा और समालोचनाकी तृप्ति नहीं कर सकता। जब तक संघके मानस विकल्प नहीं हटेंगे तब तक वे बौद्धिकहीनता, मानसदीनताके तामस भावोंसे त्राण नहीं पा सकते और चित्तमें यथार्थ निर्वैर वृत्तिका उदय नहीं कर सकते / जिस आत्माके यह सब होता है यदि उसके ही स्वरूपका भान न हो तो मात्र अनुपयोगिताका सामयिक समाधाम शिष्योंके मुंहको बन्द नहीं रख सकता / आखिर मालुक्यपुत्तने बुद्धको साफ-साफ कह दिया कि आप यदि नहीं जानते तो साफ-साफ क्यों नहीं कहते कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालम / जिन प्रश्नोंको बुद्धने अव्याकृत रखा उनका महावीरने अनेकान्तदष्टिसे स्वाद्वाद भाषामें निरूपण किया। उनने आत्माको द्रव्यदृष्टिसे शाश्वत, पर्यायष्टिसे अशाश्वत बताया। यदि आत्मा सदा अपरिवर्तनशील माना जाता तो पुण्य-पाप सब व्यर्थ हो जाते हैं क्योंकि उनका असर आत्मापर लो पड़ेगा नहीं। यदि आत्मा क्षण विनश्वर और धाराविहीन निःसन्तान सर्वथा नवोत्पादवाला है तो भी कृत कर्मकी निष्फलता होती है, परलोक नहीं बनता / अतः द्रव्य-दृष्टिसे धारा-प्रवाही प्रतिक्षण परिवर्तित संस्कारग्राही आत्मामें ही पुण्य-पाप कर्तृत्व सदाचार ब्रह्मचर्यवास आदि सार्थक होते है। इसमें न औपनिषदोंकी तरह शाश्वतवादका प्रसंग है और न जड़वादियोंकी तरह उच्छेदवादका डर है और न उसे उभयनिषेषक 'अशाश्वतानुच्छेदवाद' जैसे विधि-विहीन शब्दसे निर्देश करनेकी ही आवश्यकता है। यही सब विचारकर भगवान् महावीरने लोक-परलोक, आत्मा आदि सभी पदार्थोंका अनेकान्तदृष्टिसे पूर्ण विचार किया और स्याद्वादवाणीसे उसके निरूपणका निर्दोष प्रकार बताया। यह जैनदर्शनकी पृष्ठभूमि है जिसपर उत्तरकालीन आचार्योंने शतावधि ग्रन्थोंकी रचना करके भारतीय साहित्यागारको आलो. कित किया। अकेले 'स्याद्वाद' पर ही बीसों छोटे-मोटे ग्रन्थ लिखे गये हैं / इस अनेकान्तके विशाल सागर में सब एकान्त समा जाते हैं / आचार्य सिद्धसेन दिवाकरके शब्दोंमें ये स्याद्वादमय जिन वचन मिथ्यादर्शनके समह रूप है। इसमें समस्त मिथ्यादृष्टियां अपनी-अपनी अपेक्षासे विराजमान हैं / और अमृतसार या अमतस्वादू हैं। वे तटस्थ वृत्तिवाले संविग्न जीवोंको अतिशय सुखदायक हैं। वे जगत का कल्याण करें "भई मिच्छादसणसमूहमइयस्स अमयसारस्स / जिणवयणस्स भगवओ संविग्गसुहाहिगम्मस्स / / " 1. देखो, प्रो० दलसुख मालवणिया लिखित जैन तर्कवार्तिक की प्रस्तावना / 4-43 Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org