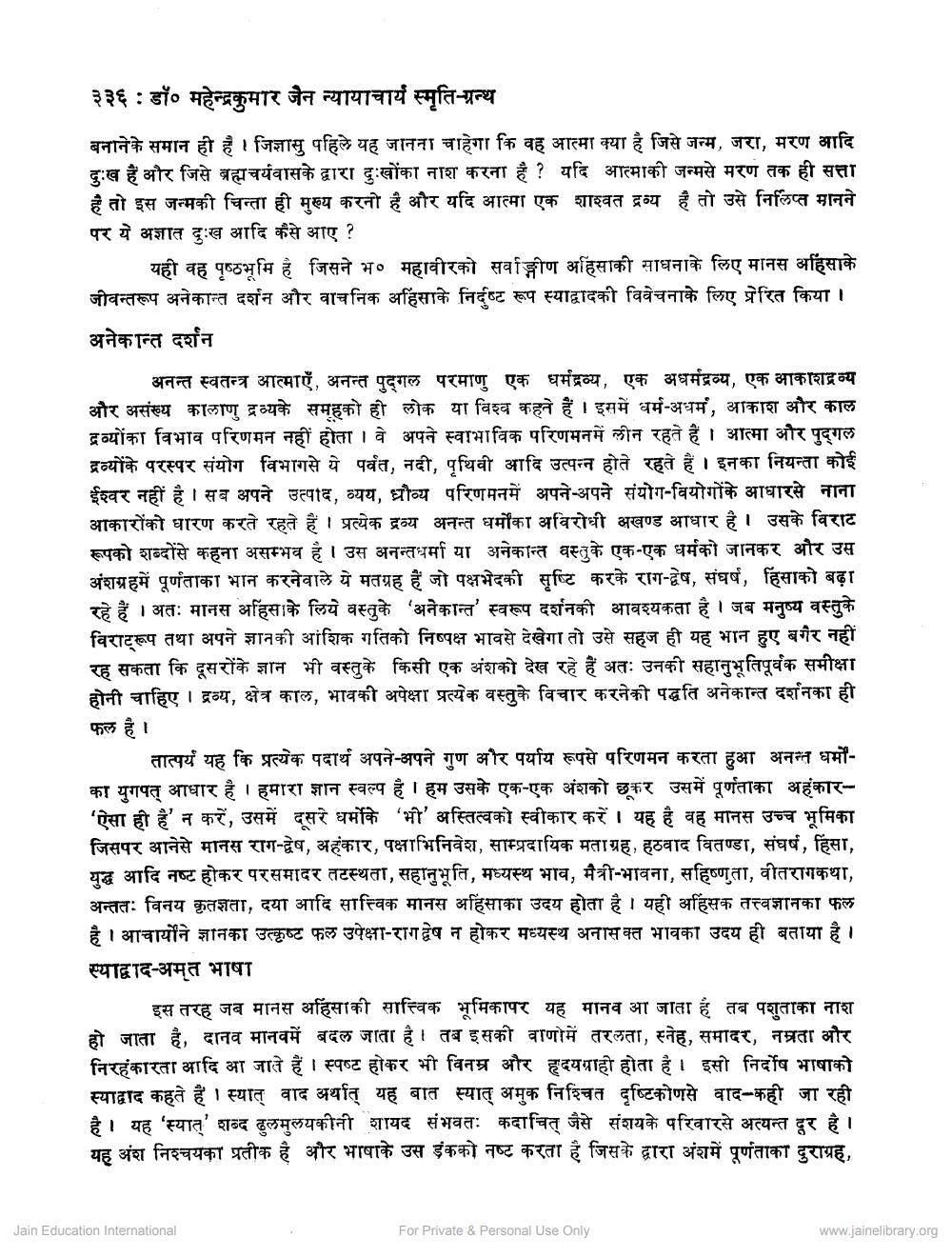________________
३३६ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ बनाने के समान ही है । जिज्ञासु पहिले यह जानना चाहेगा कि वह आत्मा क्या है जिसे जन्म, जरा, मरण आदि दुःख है और जिसे ब्रह्मचर्यवासके द्वारा दुःखोंका नाश करना है ? यदि आत्माकी जन्मसे मरण तक ही सत्ता है तो इस जन्मकी चिन्ता ही मुख्य करनी है और यदि आत्मा एक शाश्वत द्रव्य है तो उसे निर्लिप्त मानने पर ये अज्ञात दुःख आदि कैसे आए ?
यही वह पृष्ठभूमि है जिसने भ० महावीरको सर्वाङ्गीण अहिंसाकी साधनाके लिए मानस अहिंसाके जीवन्तरूप अनेकान्त दर्शन और वाचनिक अहिंसाके निर्दुष्ट रूप स्याद्वादकी विवेचनाके लिए प्रेरित किया । अनेकान्त दर्शन
अनन्त स्वतन्त्र आत्माएँ, अनन्त पुद्गल परमाणु एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य और असंख्य कालाणु द्रव्यके समहको ही लोक या विश्व कहते हैं । इसमें धर्म-अधर्म, आकाश और काल द्रव्योंका विभाव परिणमन नहीं होता । वे अपने स्वाभाविक परिणमनमें लीन रहते हैं । आत्मा और पुद्गल द्रव्योंके परस्पर संयोग विभागसे ये पर्वत, नदी, पृथिवी आदि उत्पन्न होते रहते हैं । इनका नियन्ता कोई ईश्वर नहीं है । सब अपने उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य परिणमनमें अपने-अपने संयोग-वियोगोंके आधारसे नाना आकारोंको धारण करते रहते हैं। प्रत्येक द्रव्य अनन्त धर्मोंका अविरोधी अखण्ड आधार है। उसके विराट रूपको शब्दोंसे कहना असम्भव है । उस अनन्तधर्मा या अनेकान्त वस्तुके एक-एक धर्मको जानकर और उस अंशग्रहमें पूर्णताका भान करनेवाले ये मतग्रह हैं जो पक्षभेदकी सृष्टि करके राग-द्वेष, संघर्ष, हिंसाको बढ़ा रहे हैं । अतः मानस अहिंसाके लिये वस्तुके 'अनेकान्त' स्वरूप दर्शनकी आवश्यकता है । जब मनुष्य वस्तुके विराटप तथा अपने ज्ञानकी आंशिक गतिको निष्पक्ष भावसे देखेगा तो उसे सहज ही यह भान हुए बगैर नहीं रह सकता कि दूसरोंके ज्ञान भी वस्तुके किसी एक अंशको देख रहे हैं अतः उनकी सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा होनी चाहिए । द्रव्य, क्षेत्र काल, भावकी अपेक्षा प्रत्येक वस्तुके विचार करनेकी पद्धति अनेकान्त दर्शनका ही
तात्पर्य यह कि प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने गुण और पर्याय रूपसे परिणमन करता हुआ अनन्त धर्मोंका युगपत् आधार है । हमारा ज्ञान स्वल्प है । हम उसके एक-एक अंशको छूकर उसमें पूर्णताका अहंकार'ऐसा ही है' न करें, उसमें दूसरे धर्मोके 'भी' अस्तित्वको स्वीकार करें। यह है वह मानस उच्च भूमिका जिसपर आनेसे मानस राग-द्वेष, अहंकार, पक्षाभिनिवेश, साम्प्रदायिक मता ग्रह, हठवाद वितण्डा, संघर्ष, हिंसा, युद्ध आदि नष्ट होकर परसमादर तटस्थता, सहानुभूति, मध्यस्थ भाव, मैत्री-भावना, सहिष्णुता, वीतरागकथा, अन्ततः विनय कृतज्ञता, दया आदि सात्त्विक मानस अहिंसाका उदय होता है। यही अहिंसक तत्त्वज्ञानका फल है। आचार्योंने ज्ञानका उत्कृष्ट फल उपेक्षा-राग द्वेष न होकर मध्यस्थ अनासक्त भावका उदय ही बताया है। स्याद्वाद-अमृत भाषा
___ इस तरह जब मानस अहिंसाकी सात्त्विक भूमिकापर यह मानव आ जाता है तब पशुताका नाश हो जाता है, दानव मानवमें बदल जाता है। तब इसकी वाणोमें तरलता, स्नेह, समादर, नम्रता और निरहंकारता आदि आ जाते हैं । स्पष्ट होकर भी विनम्र और हृदयग्राही होता है। इसी निर्दोष भाषाको स्याद्वाद कहते हैं । स्यात् वाद अर्थात् यह बात स्यात् अमुक निश्चित दृष्टिकोणसे वाद-कही जा रही है। यह 'स्यात्' शब्द ढुलमुलयकीनी शायद संभवतः कदाचित् जैसे संशयके परिवारसे अत्यन्त दूर है। यह अंश निश्चयका प्रतीक है और भाषाके उस इंकको नष्ट करता है जिसके द्वारा अंशमें पूर्णताका दुराग्रह,
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org