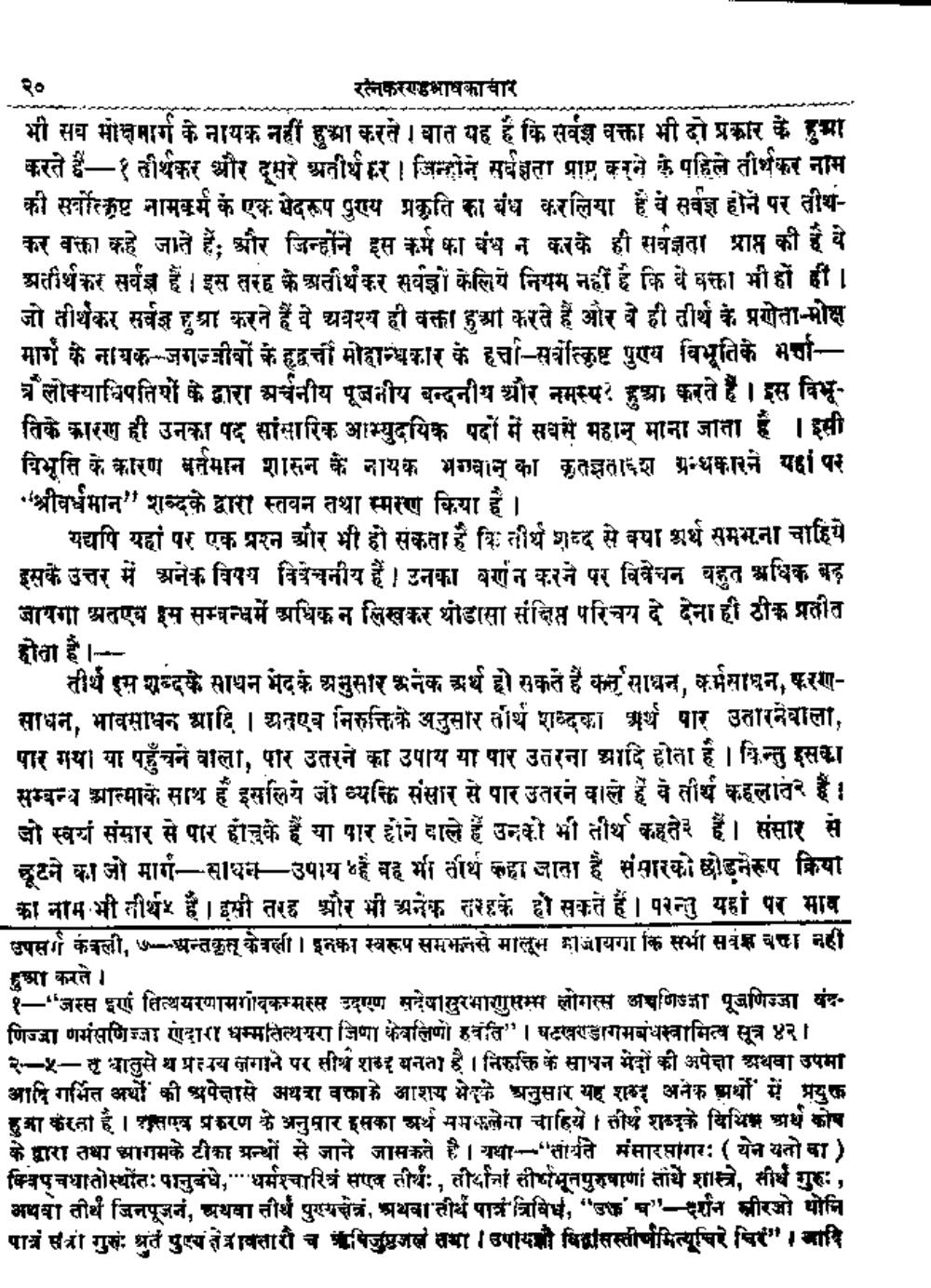________________
रत्नकरण्डभाषकाचार
भी सब मोक्षमार्ग के नायक नहीं हुआ करते । बात यह हैं कि सर्वज्ञ वक्ता भी दो प्रकार के हुआ करते हैं— १ तीर्थकर और दूसरे अतीर्थकर | जिन्होने सर्वज्ञता प्राप्त करने के पहिले तीर्थकर नाम की सर्वोत्कृष्ट नाम के एक भेदरूप पुण्य प्रकृति का बंध कर लिया है वे सर्वज्ञ होने पर तीर्थकर वक्ता कहे जाते हैं; और जिन्होंने इस कर्म का बंधन करके ही सर्वज्ञता प्राप्त की हैं वे तीर्थकर सर्वज्ञ हैं । इस तरह के तीर्थंकर सर्वज्ञों के लिये नियम नहीं है कि वे बक्ता भी हों ह्रीं । जो तीर्थंकर सर्वज्ञ हुआ करते हैं वे अवश्य ही वक्ता हुआ करते हैं और वे ही तीर्थ के प्रणेता मोक्ष मार्ग के नायक- जगज्जीवों के हृद्वर्त्ती मोहान्धकार के हर्त्ता - सर्वस्कृष्ट पुण्य विभूतिके भर्चा त्रैलोक्याधिपतियों के द्वारा अर्चनीय पूजनीय चन्दनीय और नमस्पर हुआ करते हैं। इस विभूतिके कारण ही उनका पद सांसारिक आभ्युदयिक पदों में सबसे महान माना जाता है । इसी विभूति के कारण वर्तमान शासन के नायक भगवान का कृतज्ञतावश ग्रन्थकारने यहां पर "श्रीवर्धमान" शब्दके द्वारा स्तवन तथा स्मरण किया हैं ।
यद्यपि यहां पर एक प्रश्न और भी हो सकता है कि तीर्थ शब्द से क्या श्रर्थ समझना चाहिये इसके उत्तर में अनेक विषय विवेचनीय हैं। उनका वर्णन करने पर विवेचन बहुत अधिक बढ़ जायगा अतएव इस सम्बन्ध में अधिक न लिखकर थोडासा संक्षिप्त परिचय दे देना ही ठीक प्रतीत होता है ।--
तीर्थ इस शब्द के साधन भेद के अनुसार अनेक अर्थ हो सकते हैं कर्तु साधन, कर्मसाधन करणासाधन, भावसाधन श्रादि । श्रतएव निरुक्ति के अनुसार तीर्थ शब्दका अर्थ पार उतारनेवाला, पार गया या पहुँचने वाला, पार उतरने का उपाय या पार उतरना आदि होता है । किन्तु इसका सम्बन्ध आत्मा के साथ हैं इसलिये जो व्यक्ति संसार से पार उतरने वाले है वे तीर्थ कहलावर हैं । जो स्वयं संसार से पार होचुके हैं या पार होने वाले हैं उनको भी तीर्थ कहते हैं। संसार सं छूटने का जो मार्ग - साधन — उपाय हैं वह भी तीर्थ कहा जाता है संसारको छोड़नेरूप क्रिया का नाम भी तीर्थ है। इसी तरह और भी अनेक तरहके हो सकते हैं। परन्तु यहां पर भाव उपसर्ग कंवली, प्रन्तकृत केवली । इनका स्वरूप समझन से मालूम हो जायगा कि सभी सर्वज्ञ वच्चा नहीं हुआ करते ।
१ - "जस्स इतित्थयरणामगांवकम्मरस उदएण सदेवासुरमासम्म लोगस्स अचनिज्ञा पूजणिज्जा वंद णिज्जा णर्मसणिज्जा दारा धम्मतित्थयरा जिष्णा केवलिणी हवति" । घटखण्डागमबंधस्वामित्व सूत्र ४२ । २५- तृ धातुसे प्रलय लगाने पर सीओ शब्द बनता है । निरुक्ति के साधन भेदों की अपेक्षा अथवा उपमा आदि गर्भित अर्थों की अपेक्षासे अथवा वक्ता के आशय के अनुसार यह शब्द अनेक अर्थो में प्रयुक्त हुआ करता है। एक प्रकरण के अनुसार इसका अर्थ समझ लेना चाहिये। तीर्थ शब्दके विभिन्न अर्थ कोष के द्वारा तथा आगम टीका प्रन्थों से जाने जासकते है । यथा-"सार्यते संसारसागरः ( येन यतो का ) क्विप्चधातोस्थतः पानुबंधे, धर्मश्चारित्रं सएव तीर्थः तीर्थानां तीर्थमून पुरुषाणां तार्थे शास्त्रे, सीधे गुरुः, अथवा तीर्थं जिनपूजनं, अथवा तीर्थं पुण्यक्षेत्रं श्रथवा तीर्थं पात्रं त्रिविधं, "उफ घ" दर्शन श्रीरजो पोनि पात्रं सत्री गुरुः श्रुतं पुष्य क्षेत्रावतारौ च ऋषिजुष्टजलं तथा । उपायशी विद्वांसस्तीर्णमित्युविरे विर" । जादि