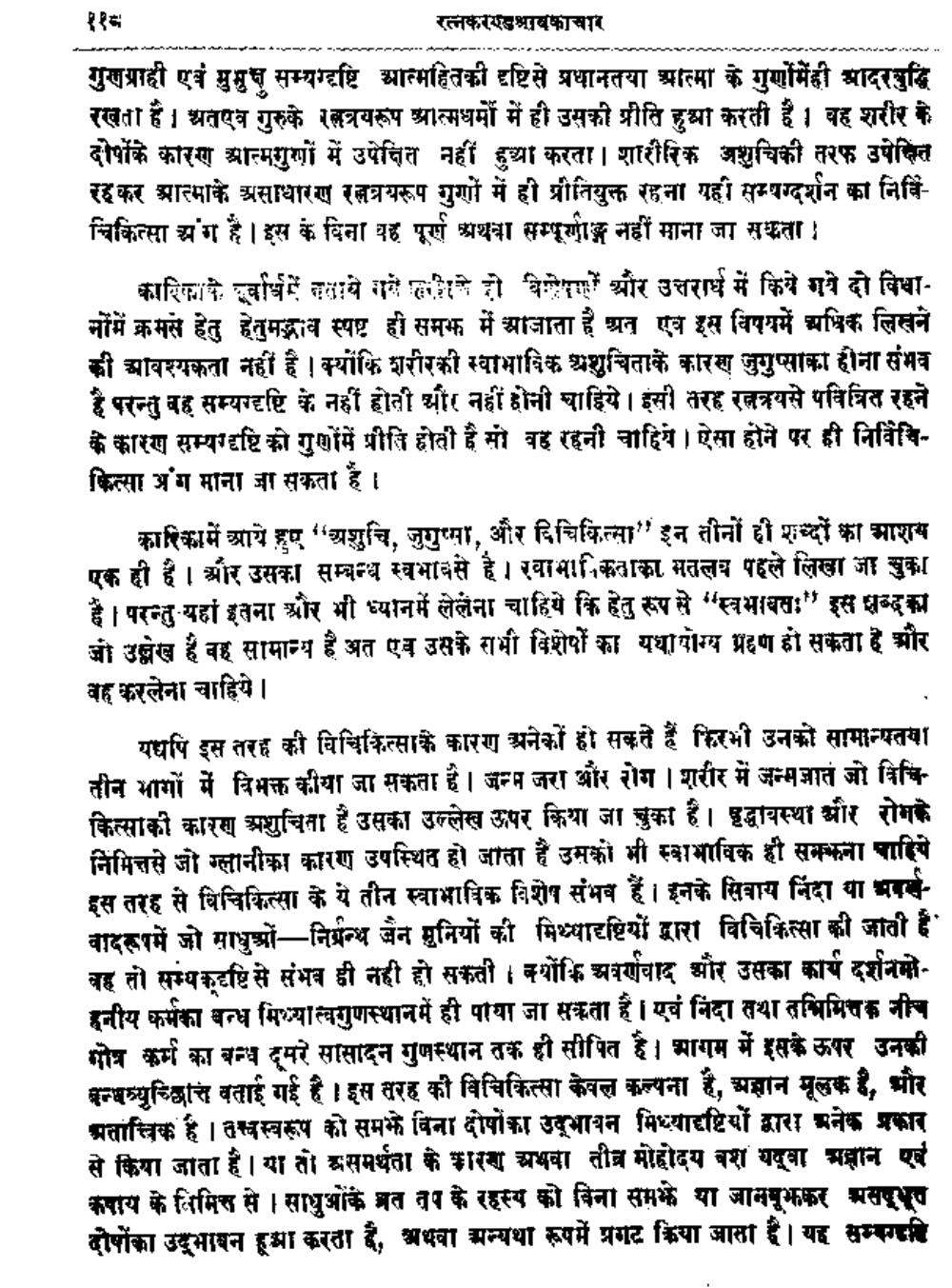________________
रत्नकरश्वश्रावकाचार गुणग्राही एवं मुमुक्षु सम्यग्दृष्टि आत्महितकी दृष्टि से प्रधानतया अात्मा के गुणों मेंही आदरयुद्धि रखता है। अतएव गुरुके लत्रयरूप श्रात्मधर्मों में ही उसकी प्रीति हुआ करती है । वह शरीर के दोषकि कारण आत्मगुरगों में उपेक्षित नहीं हुया करता । शारीरिक अशुचिकी तरफ उपेक्षित रहकर आत्माके असाधारण रसत्रयरूप गुणों में ही प्रीतियुक्त रहना यही सम्यग्दर्शन का निर्विचिकित्सा अंग है। इस के विना यह पूर्ण अथवा सम्पूर्णीङ्ग नहीं माना जा सकता। __ कारिगाय पूर्वार्ध बताये गये तो दो बोषणों और उत्तरार्ध में किये गये दो विधा. नों में क्रमस हेतु हेतुमद्भाव स्पष्ट ही समझ में आजाता है अन एव इस विषयमें अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि शरीरकी स्वाभाविक अशुचिताके कारण जुगुप्साका होना संभव है परन्तु वह सम्यग्दृष्टि के नहीं होती और नहीं होनी चाहिये । इसी तरह रत्नत्रयसे पवित्रित रहने के कारण सम्यग्दृष्टिको गुणों में प्रीति होती है मो वह रहनी चाहिये । ऐसा होने पर ही निविधिकित्सा अंग माना जा सकता है।
कारिकामें आये हुए "अशुचि, जुगुप्मा, और विचिकित्सा" इन तीनों ही शब्दों का भाशय एक ही है । और उसका सम्बन्ध स्वभावसे है । रवामानिकताका. मतलब पहले लिखा जा चुका है। परन्तु-यहां इतना और भी ध्यान में लेना चाहिये कि हेतु रूप से "स्वभावतः" इस शब्दका जो उल्लेख है वह सामान्य है अत एव उसके सभी विशेषों का यथायोग्य प्रहण हो सकता है और वह करलेना चाहिये। ___ यधपि इस तरह की विचिकित्साके कारण अनेकों हो सकते है रिभी उनको सामान्यतया तीन भागों में विभक्त कीया जा सकता है । जन्म जरा और रोग । शरीर में जन्मजातं जो विधि कित्साकी कारण अशुचिता है उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। वृद्धावस्था और रोमके निमित्तसे जो ग्लानीका कारण उपस्थित हो जाता है उसको भी स्वाभाविक ही समझना चाहिये इस तरह से विचिकित्सा के ये तीन स्वाभाविक विशेष संभव हैं। इनके सिवाय निंदा या भवई वादरूपमें जो माधुओं-निग्रन्थ जैन मुनियों की मिथ्याष्टियों द्वारा विचिकित्सा की जाती है वह सो सम्यकदृष्टि से संभव ही नहीं हो सकती। क्योंकि अवर्णवाद और उसका कार्य दर्शनमोहनीय फर्मका बन्ध मिथ्यात्वगुणस्थानमें ही पाया जा सकता है । एवं निंदा सथा तबिमिचक नीच गोत्र कर्म का बन्ध दूसरे सासादन गुणस्थान तक ही सीपित है। मागम में इसके ऊपर उनकी बन्धयुच्छिात बताई गई है। इस तरह की विचिकित्सा केवल कल्पना है, अज्ञान मूलक है, और प्रताचिक है । तस्वस्वरूप को समझे विना दोषोंका उद्भावन मिश्यादृष्टियों द्वारा अनेक प्रकार से किया जाता है। या तो असमर्थता के कारण अथवा तीन मोहोदय वश यद्वा अमान एवं कपाय के निमित्त से । साधुओंके प्रत तप के रहस्य को बिना समझे या जानबूझकर असदश्व दोषोंका उद्भावन हूआ करता है, अथवा अन्यथा रूपमें प्रगट किया जाता है। यह सम्मति