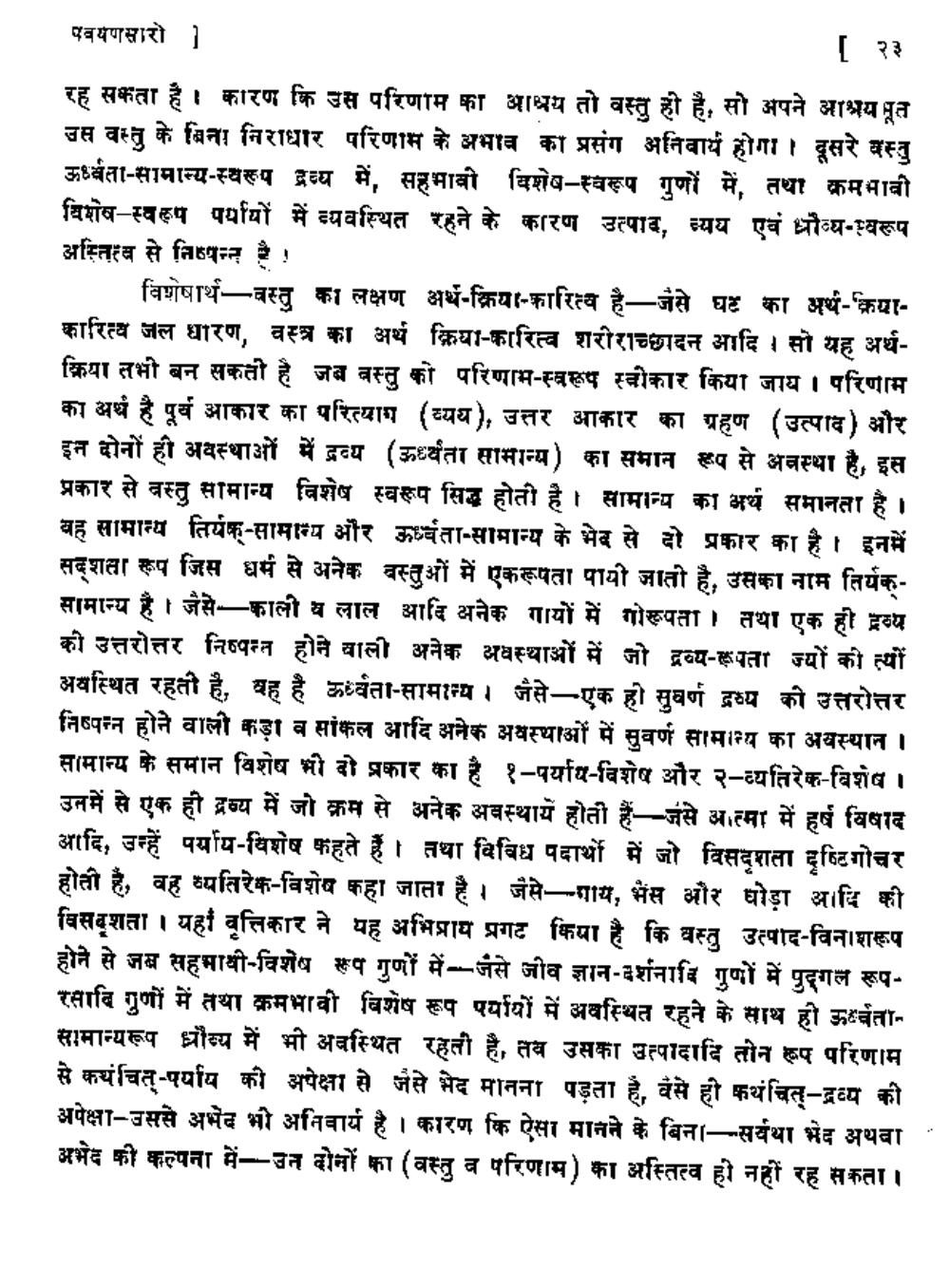________________
पवयणसारो ।
[ २३ रह सकता है। कारण कि उस परिणाम का आश्रय तो वस्तु ही है, सो अपने आश्रय भूत उस वस्तु के बिना निराधार परिणाम के अभाव का प्रसंग अनिवार्य होगा। दूसरे वस्तु ऊवता-सामान्य-स्वरूप द्रव्य में, सहभावी विशेष-स्वरूप गुणों में, तथा क्रमभावी विशेष-स्वरूप पर्यायों में व्यवस्थित रहने के कारण उत्पाद, व्यय एवं धौव्य-स्वरूप अस्तित्व से निष्पन्न है।
विशेषार्थ-वस्तु का लक्षण अर्थ-क्रिया-कारित्व है-जैसे घट का अर्थ-'क्रयाकारित्व जल धारण, वस्त्र का अर्थ क्रिया-कारित्व शरीराच्छादन आदि । सो यह अर्थक्रिया तभी बन सकती है जब वस्तु को परिणाम स्वरूप स्वीकार किया जाय । परिणाम का अर्थ है पूर्व आकार का परित्याग (व्यय), उत्तर आकार का ग्रहण (उत्पाद) और इन दोनों ही अवस्थाओं में द्रव्य (ऊर्ध्वता सामान्य) का समान रूप से अवस्था है, इस प्रकार से वस्तु सामान्य विशेष स्वरूप सिद्ध होती है। सामान्य का अर्थ समानता है । वह सामान्य तिर्यक-सामान्य और ऊर्वता-सामान्य के भेव से दो प्रकार का है। इनमें सदशता रूप जिस धर्म से अनेक वस्तुओं में एकरूपता पायी जाती है, उसका नाम तिर्यक्सामान्य है। जैसे—काली व लाल आदि अनेक गायों में गोरूपता। तथा एक ही द्रव्य को उत्तरोत्तर निष्पन्न होने वाली अनेक अवस्थाओं में जो द्रव्य-रूपता ज्यों की त्यों अवस्थित रहती है, वह है ऊवता-सामान्य । जैसे-एक ही सुवर्ण द्रव्य को उत्तरोत्तर निष्पन्न होने वाली कड़ा व सांकल आदि अनेक अवस्थाओं में सुवर्ण सामान्य का अवस्थान । सामान्य के समान विशेष भी दो प्रकार का है १-पर्याय-विशेष और २-व्यतिरेक-विशेष । उनमें से एक ही द्रव्य में जो क्रम से अनेक अवस्थायें होती हैं-जैसे आत्मा में हर्ष विषाद आदि, उन्हें पर्याय-विशेष कहते हैं। तथा विविध पदार्थों में जो विसदृशता दृष्टिगोचर होती है, वह व्यतिरेक-विशेष कहा जाता है। जैसे-पाय, भैंस और घोड़ा आदि की विसदशता । यहाँ वृत्तिकार ने यह अभिप्राय प्रगट किया है कि वस्तु उत्पाद-विनाशरूप होने से जब सहभावी-विशेष रूप गुणों में-जैसे जीव ज्ञान-दर्शनादि गुणों में पुद्गल रूपरसादि गुणों में तथा क्रमभावी विशेष रूप पर्यायों में अवस्थित रहने के साथ ही ऊर्चतासामान्यरूप ध्रौव्य में भी अवस्थित रहती है, तब उसका उत्पादादि तीन रूप परिणाम से कथंचित-पर्याय की अपेक्षा से जैसे भेद मानना पड़ता है, वैसे ही कथंचित-द्रव्य की अपेक्षा-उससे अभेद भी अनिवार्य है । कारण कि ऐसा मानने के बिना-सर्वथा भेद अथवा " अभेद की कल्पना में--उन दोनों का (वस्तु व परिणाम) का अस्तित्व ही नहीं रह सकता।