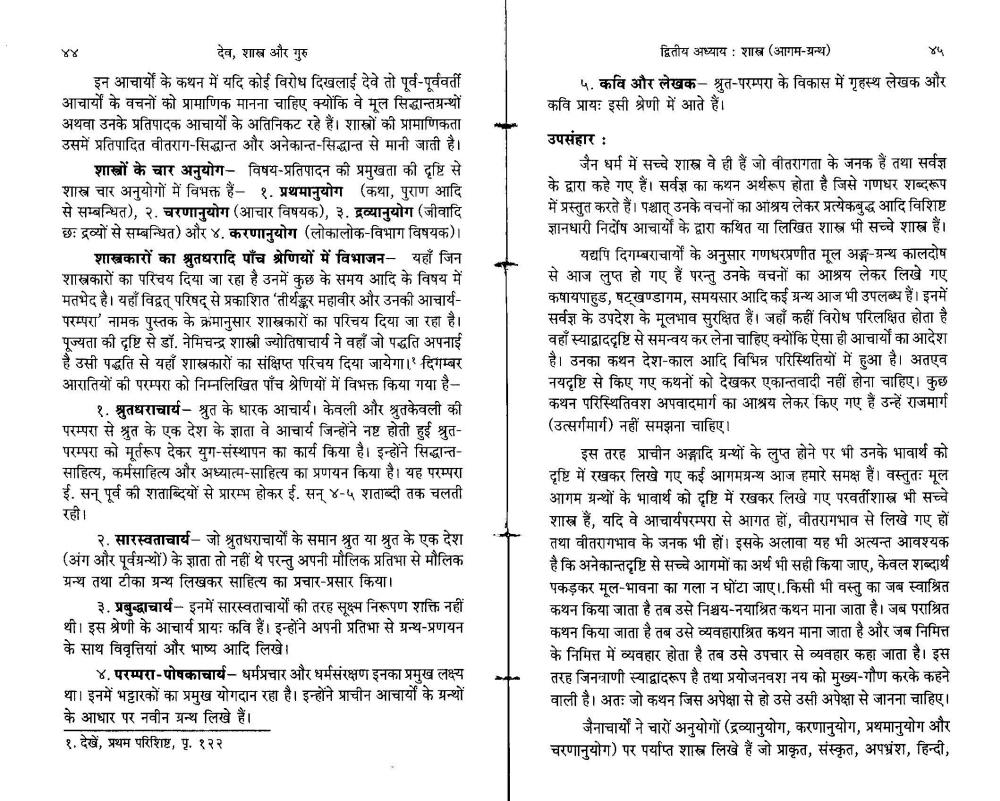________________ देव, शास्त्र और गुरु इन आचार्यों के कथन में यदि कोई विरोध दिखलाई देवे तो पूर्व-पूर्ववर्ती आचार्यों के वचनों को प्रामाणिक मानना चाहिए क्योंकि वे मूल सिद्धान्तग्रन्थों अथवा उनके प्रतिपादक आचार्यों के अतिनिकट रहे हैं। शास्त्रों की प्रामाणिकता उसमें प्रतिपादित वीतराग-सिद्धान्त और अनेकान्त-सिद्धान्त से मानी जाती है। शास्त्रों के चार अनुयोग- विषय-प्रतिपादन की प्रमुखता की दृष्टि से शास्त्र चार अनुयोगों में विभक्त हैं- 1. प्रथमानुयोग (कथा, पुराण आदि से सम्बन्धित), 2. चरणानुयोग (आचार विषयक), 3. द्रव्यानुयोग (जीवादि छः द्रव्यों से सम्बन्धित) और 4. करणानुयोग (लोकालोक-विभाग विषयक)। शास्त्रकारों का श्रुतधरादि पाँच श्रेणियों में विभाजन- यहाँ जिन शास्त्रकारों का परिचय दिया जा रहा है उनमें कुछ के समय आदि के विषय में मतभेद है। यहाँ विद्वत् परिषद् से प्रकाशित 'तीर्थङ्कर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा' नामक पुस्तक के क्रमानुसार शास्त्रकारों का परिचय दिया जा रहा है। पूज्यता की दृष्टि से डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री ज्योतिषाचार्य ने वहाँ जो पद्धति अपनाई है उसी पद्धति से यहाँ शास्त्रकारों का संक्षिप्त परिचय दिया जायेगा। दिगम्बर आरातियों की परम्परा को निम्नलिखित पाँच श्रेणियों में विभक्त किया गया है 1. श्रुतधराचार्य- श्रुत के धारक आचार्य। केवली और श्रुतकेवली की परम्परा से श्रुत के एक देश के ज्ञाता वे आचार्य जिन्होंने नष्ट होती हुई श्रुतपरम्परा को मूर्तरूप देकर युग-संस्थापन का कार्य किया है। इन्होंने सिद्धान्तसाहित्य, कर्मसाहित्य और अध्यात्म-साहित्य का प्रणयन किया है। यह परम्परा ई. सन पर्व की शताब्दियों से प्रारम्भ होकर ई. सन् 4-5 शताब्दी तक चलती रही। 2. सारस्वताचार्य- जो श्रुतधराचार्यों के समान श्रत या श्रत के एक देश (अंग और पूर्वग्रन्थों) के ज्ञाता तो नहीं थे परन्तु अपनी मौलिक प्रतिभा से मौलिक ग्रन्थ तथा टीका ग्रन्थ लिखकर साहित्य का प्रचार-प्रसार किया। 3. प्रबुद्धाचार्य- इनमें सारस्वताचार्यों की तरह सूक्ष्म निरूपण शक्ति नहीं थी। इस श्रेणी के आचार्य प्रायः कवि हैं। इन्होंने अपनी प्रतिभा से ग्रन्थ-प्रणयन के साथ विवृत्तियां और भाष्य आदि लिखे। 4. परम्परा-पोषकाचार्य- धर्मप्रचार और धर्मसंरक्षण इनका प्रमुख लक्ष्य था। इनमें भट्टारकों का प्रमुख योगदान रहा है। इन्होंने प्राचीन आचार्यों के ग्रन्थों के आधार पर नवीन ग्रन्थ लिखे हैं। 1. देखें, प्रथम परिशिष्ट, पृ. 122 द्वितीय अध्याय : शास्त्र (आगम-ग्रन्थ) 5. कवि और लेखक- श्रुत-परम्परा के विकास में गृहस्थ लेखक और कवि प्रायः इसी श्रेणी में आते हैं। उपसंहार : जैन धर्म में सच्चे शास्त्र वे ही हैं जो वीतरागता के जनक हैं तथा सर्वज्ञ के द्वारा कहे गए हैं। सर्वज्ञ का कथन अर्थरूप होता है जिसे गणधर शब्दरूप में प्रस्तुत करते हैं। पश्चात् उनके वचनों का आश्रय लेकर प्रत्येकबुद्ध आदि विशिष्ट ज्ञानधारी निर्दोष आचार्यों के द्वारा कथित या लिखित शास्त्र भी सच्चे शास्त्र हैं। यद्यपि दिगम्बराचार्यों के अनुसार गणधरप्रणीत मूल अङ्ग-ग्रन्थ कालदोष से आज लुप्त हो गए हैं परन्तु उनके वचनों का आश्रय लेकर लिखे गए कषायपाहुड, षट्खण्डागम, समयसार आदि कई ग्रन्थ आज भी उपलब्ध हैं। इनमें सर्वज्ञ के उपदेश के मूलभाव सुरक्षित हैं। जहाँ कहीं विरोध परिलक्षित होता है वहाँ स्याद्वाददृष्टि से समन्वय कर लेना चाहिए क्योंकि ऐसा ही आचार्यों का आदेश है। उनका कथन देश-काल आदि विभिन्न परिस्थितियों में हुआ है। अतएव नयदृष्टि से किए गए कथनों को देखकर एकान्तवादी नहीं होना चाहिए। कुछ कथन परिस्थितिवश अपवादमार्ग का आश्रय लेकर किए गए हैं उन्हें राजमार्ग (उत्सर्गमार्ग) नहीं समझना चाहिए। इस तरह प्राचीन अङ्गादि ग्रन्थों के लुप्त होने पर भी उनके भावार्थ को दृष्टि में रखकर लिखे गए कई आगमग्रन्थ आज हमारे समक्ष हैं। वस्तुतः मूल आगम ग्रन्थों के भावार्थ को दृष्टि में रखकर लिखे गए परवर्तीशास्त्र भी सच्चे शास्त्र हैं, यदि वे आचार्यपरम्परा से आगत हों, वीतरागभाव से लिखे गए हों तथा वीतरागभाव के जनक भी हों। इसके अलावा यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि अनेकान्तदृष्टि से सच्चे आगमों का अर्थ भी सही किया जाए, केवल शब्दार्थ पकड़कर मूल-भावना का गला न घोंटा जाए।.किसी भी वस्तु का जब स्वाश्रित कथन किया जाता है तब उसे निश्चय-नयाश्रित कथन माना जाता है। जब पराश्रित कथन किया जाता है तब उसे व्यवहाराश्रित कथन माना जाता है और जब निमित्त के निमित्त में व्यवहार होता है तब उसे उपचार से व्यवहार कहा जाता है। इस तरह जिनवाणी स्याद्वादरूप है तथा प्रयोजनवश नय को मुख्य-गौण करके कहने वाली है। अतः जो कथन जिस अपेक्षा से हो उसे उसी अपेक्षा से जानना चाहिए। जैनाचार्यों ने चारों अनुयोगों (द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, प्रथमानुयोग और चरणानुयोग) पर पर्याप्त शास्त्र लिखे हैं जो प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी,