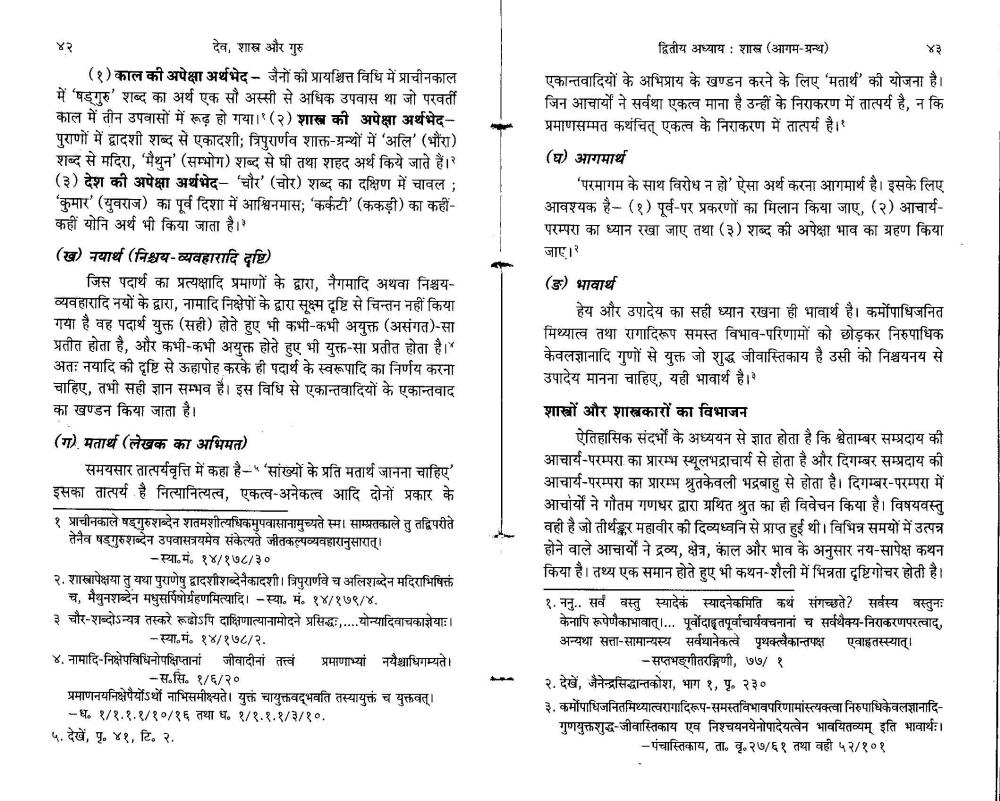________________ 42 देव, शास्त्र और गुरु (1) काल की अपेक्षा अर्थभेद- जैनों की प्रायश्चित्त विधि में प्राचीनकाल में 'षड्गुरु' शब्द का अर्थ एक सौ अस्सी से अधिक उपवास था जो परवर्ती काल में तीन उपवासों में रूढ़ हो गया। (2) शास्त्र की अपेक्षा अर्थभेदपुराणों में द्वादशी शब्द से एकादशी; त्रिपुरार्णव शाक्त-ग्रन्थों में 'अलि' (भौंरा) शब्द से मदिरा, 'मैथुन' (सम्भोग) शब्द से घी तथा शहद अर्थ किये जाते हैं। (3) देश की अपेक्षा अर्थभेद- 'चौर' (चोर) शब्द का दक्षिण में चावल ; 'कुमार' (युवराज) का पूर्व दिशा में आश्विनमास; 'कर्कटी' (ककड़ी) का कहींकहीं योनि अर्थ भी किया जाता है।' (ख) नयार्थ (निश्चय-व्यवहारादि दृष्टि) जिस पदार्थ का प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा, नैगमादि अथवा निश्चयव्यवहारादि नयों के द्वारा, नामादि निक्षेपों के द्वारा सूक्ष्म दृष्टि से चिन्तन नहीं किया गया है वह पदार्थ युक्त (सही) होते हुए भी कभी-कभी अयुक्त (असंगत)-सा प्रतीत होता है, और कभी-कभी अयक्त होते हुए भी युक्त-सा प्रतीत होता है। अतः नयादि की दृष्टि से ऊहापोह करके ही पदार्थ के स्वरूपादि का निर्णय करना चाहिए, तभी सही ज्ञान सम्भव है। इस विधि से एकान्तवादियों के एकान्तवाद का खण्डन किया जाता है। (ग) मतार्थ (लेखक का अभिमत) समयसार तात्पर्यवृत्ति में कहा है- 5 ‘सांख्यों के प्रति मतार्थ जानना चाहिए' इसका तात्पर्य है नित्यानित्यत्व, एकत्व-अनेकत्व आदि दोनों प्रकार के 1 प्राचीनकाले षड्गुरुशब्देन शतमशीत्यधिकमुपवासानामुच्यते स्म। साम्प्रतकाले तु तद्विपरीते तेनैव षड्गुरुशब्देन उपवासत्रयमेव संकेत्यते जीतकल्पव्यवहारानुसारात्। -स्या. मं. 14/178/30 2. शास्त्रापेक्षया तु यथा पुराणेषु द्वादशीशब्देनैकादशी। त्रिपुरार्णवे च अलिशब्देन मदिराभिषिक्तं च, मैथुनशब्देन मधुसर्पिषोर्ग्रहणमित्यादि। -स्या. मं. 14/179/4. 3 चौर-शब्दोऽन्यत्र तस्करे रूढोऽपि दाक्षिणात्यानामोदने प्रसिद्धः,....योन्यादिवाचकाज्ञेयाः। -स्या.मं. 14/178/2. 4. नामादि-निक्षेपविधिनोपक्षिप्तानां जीवादीनां तत्त्वं प्रमाणाभ्यां नयैचाधिगम्यते। -स.सि. 1/6/20 प्रमाणनयनिक्षेपर्योऽथों नाभिसमीक्ष्यते। युक्तं चायुक्तवद्भवति तस्यायुक्तं च युक्तवत्। -ध. 1/1.1.1/10/16 तथा घ, 1/1.1.1/3/10. 5. देखें, पृ. 41, टि. 2. द्वितीय अध्याय : शास्त्र (आगम-ग्रन्थ) एकान्तवादियों के अभिप्राय के खण्डन करने के लिए 'मतार्थ' की योजना है। जिन आचार्यों ने सर्वथा एकत्व माना है उन्हीं के निराकरण में तात्पर्य है, न कि प्रमाणसम्मत कथंचित् एकत्व के निराकरण में तात्पर्य है।' (घ) आगमार्थ 'परमागम के साथ विरोध न हो ऐसा अर्थ करना आगमार्थ है। इसके लिए आवश्यक है- (1) पूर्व-पर प्रकरणों का मिलान किया जाए, (2) आचार्यपरम्परा का ध्यान रखा जाए तथा (3) शब्द की अपेक्षा भाव का ग्रहण किया जाए। (ङ) भावार्थ हेय और उपादेय का सही ध्यान रखना ही भावार्थ है। कर्मोपाधिजनित मिथ्यात्व तथा रागादिरूप समस्त विभाव-परिणामों को छोड़कर निरुपाधिक केवलज्ञानादि गुणों से युक्त जो शुद्ध जीवास्तिकाय है उसी को निश्चयनय से उपादेय मानना चाहिए, यही भावार्थ है। शास्त्रों और शास्त्रकारों का विभाजन ऐतिहासिक संदर्भो के अध्ययन से ज्ञात होता है कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय की आचार्य-परम्परा का प्रारम्भ स्थूलभद्राचार्य से होता है और दिगम्बर सम्प्रदाय की आचार्य-परम्परा का प्रारम्भ श्रुतकेवली भद्रबाहु से होता है। दिगम्बर-परम्परा में आचार्यों ने गौतम गणधर द्वारा ग्रथित श्रुत का ही विवेचन किया है। विषयवस्तु वही है जो तीर्थङ्कर महावीर की दिव्यध्वनि से प्राप्त हुई थी। विभिन्न समयों में उत्पन्न होने वाले आचार्यों ने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार नय-सापेक्ष कथन किया है। तथ्य एक समान होते हुए भी कथन-शैली में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। 1. ननु.. सर्व वस्तु स्यादेकं स्यादनेकमिति कथं संगच्छते? सर्वस्य वस्तुनः केनापि रूपेणैकाभावात्।... पूर्वोदाइतपूर्वाचार्यवचनानां च सर्वथैक्य-निराकरणपरत्वाद, अन्यथा सत्ता-सामान्यस्य सर्वथानेकत्वे पृथक्त्वैकान्तपक्ष एवाहतस्स्यात्। -सप्तभङ्गीतरङ्गिणी, 77/1 2. देखें, जैनेन्द्रसिद्धान्तकोश, भाग 1, पृ. 230 3. कर्मोपाधिजनितमिथ्यात्वरागादिरूप-समस्तविभावपरिणामांस्त्यक्त्वा निरुपाधिकेवलज्ञानादिगुणयुक्तशुद्ध-जीवास्तिकाय एव निश्चयनयेनोपादेयत्वेन भावयितव्यम् इति भावार्थः। -पंचास्तिकाय, ता. वृ.२७/६१ तथा वही 52/101