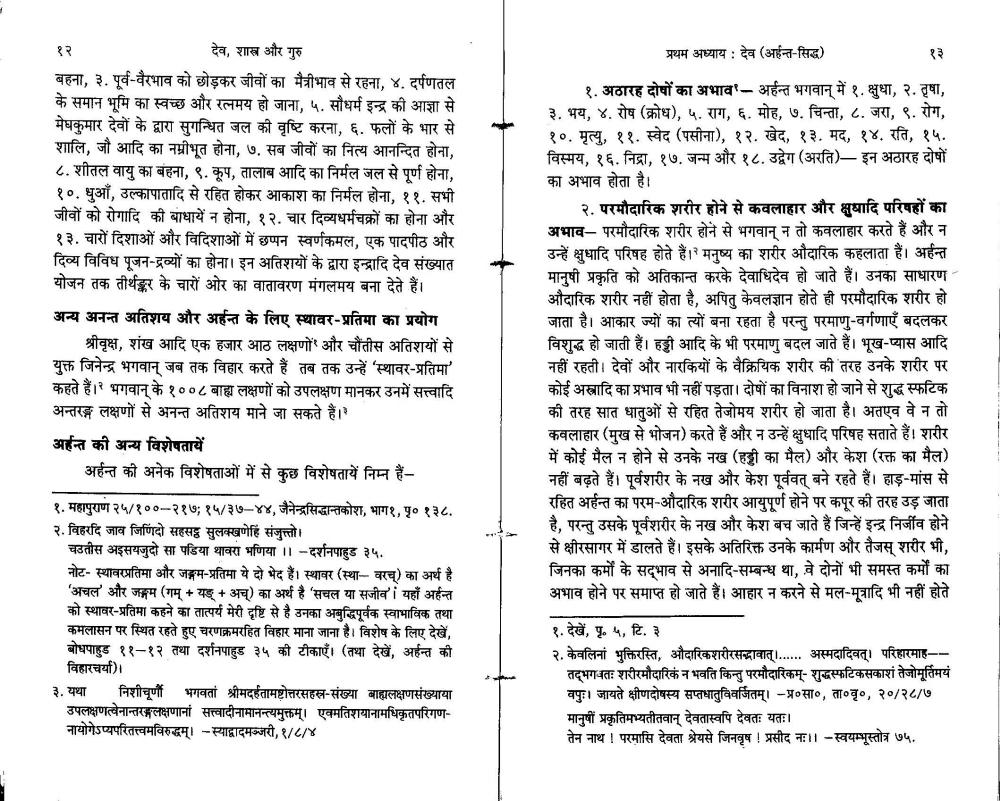________________ प्रथम अध्याय : देव (अर्हन्त-सिद्ध) देव, शास्त्र और गुरु बहना, 3. पूर्व-वैरभाव को छोड़कर जीवों का मैत्रीभाव से रहना, 4. दर्पणतल के समान भूमि का स्वच्छ और रलमय हो जाना, 5. सौधर्म इन्द्र की आज्ञा से मेघकुमार देवों के द्वारा सुगन्धित जल की वृष्टि करना, 6. फलों के भार से शालि, जौ आदि का नम्रीभूत होना, 7. सब जीवों का नित्य आनन्दित होना, 8. शीतल वायु का बहना, 9. कूप, तालाब आदि का निर्मल जल से पूर्ण होना, 10. धुआँ, उल्कापातादि से रहित होकर आकाश का निर्मल होना, 11. सभी जीवों को रोगादि की बाधायें न होना, 12. चार दिव्यधर्मचक्रों का होना और 13. चारों दिशाओं और विदिशाओं में छप्पन स्वर्णकमल, एक पादपीठ और दिव्य विविध पूजन-द्रव्यों का होना। इन अतिशयों के द्वारा इन्द्रादि देव संख्यात योजन तक तीर्थङ्कर के चारों ओर का वातावरण मंगलमय बना देते हैं। अन्य अनन्त अतिशय और अर्हन्त के लिए स्थावर-प्रतिमा का प्रयोग श्रीवृक्ष, शंख आदि एक हजार आठ लक्षणों और चौतीस अतिशयों से युक्त जिनेन्द्र भगवान् जब तक विहार करते हैं तब तक उन्हें 'स्थावर-प्रतिमा' कहते हैं। भगवान् के 1008 बाह्य लक्षणों को उपलक्षण मानकर उनमें सत्त्वादि अन्तरङ्ग लक्षणों से अनन्त अतिशय माने जा सकते हैं। अर्हन्त की अन्य विशेषतायें ___ अर्हन्त की अनेक विशेषताओं में से कुछ विशेषतायें निम्न हैं 1. अठारह दोषों का अभाव'- अर्हन्त भगवान् में 1. क्षुधा, 2. तृषा, 3. भय, 4. रोष (क्रोध), 5. राग, 6. मोह, 7. चिन्ता, 8. जरा, 9. रोग, 10. मृत्यु, 11. स्वेद (पसीना), 12. खेद, 13. मद, 14. रति, 15. विस्मय, 16. निद्रा, 17. जन्म और 18. उद्वेग (अरति)- इन अठारह दोषों का अभाव होता है। 2. परमौदारिक शरीर होने से कवलाहार और क्षुषादि परिषहों का अभाव- परमौदारिक शरीर होने से भगवान् न तो कवलाहार करते हैं और न उन्हें क्षुधादि परिषह होते हैं। मनुष्य का शरीर औदारिक कहलाता हैं। अर्हन्त मानुषी प्रकृति को अतिकान्त करके देवाधिदेव हो जाते हैं। उनका साधारण औदारिक शरीर नहीं होता है, अपितु केवलज्ञान होते ही परमौदारिक शरीर हो जाता है। आकार ज्यों का त्यों बना रहता है परन्तु परमाणु-वर्गणाएँ बदलकर विशुद्ध हो जाती हैं। हड्डी आदि के भी परमाणु बदल जाते हैं। भूख-प्यास आदि नहीं रहती। देवों और नारकियों के वैक्रियिक शरीर की तरह उनके शरीर पर कोई अस्त्रादि का प्रभाव भी नहीं पड़ता। दोषों का विनाश हो जाने से शुद्ध स्फटिक की तरह सात धातुओं से रहित तेजोमय शरीर हो जाता है। अतएव वे न तो कवलाहार (मुख से भोजन) करते हैं और न उन्हें क्षुधादि परिषह सताते हैं। शरीर में कोई मैल न होने से उनके नख (हड्डी का मैल) और केश (रक्त का मैल) नहीं बढ़ते हैं। पूर्वशरीर के नख और केश पूर्ववत् बने रहते हैं। हाड़-मांस से रहित अर्हन्त का परम-औदारिक शरीर आयुपूर्ण होने पर कपूर की तरह उड़ जाता है, परन्तु उसके पूर्वशरीर के नख और केश बच जाते हैं जिन्हें इन्द्र निर्जीव होने से क्षीरसागर में डालते हैं। इसके अतिरिक्त उनके कार्मण और तैजस् शरीर भी, जिनका कर्मों के सद्भाव से अनादि-सम्बन्ध था, वे दोनों भी समस्त कर्मों का अभाव होने पर समाप्त हो जाते हैं। आहार न करने से मल-मूत्रादि भी नहीं होते 1. महापुराण 25/100-217; 15/37-44, जैनेन्द्रसिद्धान्तकोश, भाग१, पृ० 138. 2. विहरदि जाव जिणिंदो सहस? सुलक्खणेहिं संजुत्तो। चउतीस अइसयजुदो सा पडिया थावरा भणिया / / -दर्शनपाहुड 35. नोट- स्थावरप्रतिमा और जङ्गम-प्रतिमा ये दो भेद हैं। स्थावर (स्था- वरच्) का अर्थ है 'अचल' और जगम (गम् + यङ् + अच्) का अर्थ है 'सचल या सजीव' यहाँ अर्हन्त को स्थावर-प्रतिमा कहने का तात्पर्य मेरी दृष्टि से है उनका अबुद्धिपूर्वक स्वाभाविक तथा कमलासन पर स्थित रहते हुए चरणक्रमरहित विहार माना जाना है। विशेष के लिए देखें, बोधपाहुड 11-12 तथा दर्शनपाहुड 35 की टीकाएँ। (तथा देखें, अर्हन्त की विहारचर्या)। 3. यथा निशीचूर्णी भगवतां श्रीमदर्हतामष्टोत्तरसहस्र-संख्या बाहालक्षणसंख्याया उपलक्षणत्वेनान्तरङ्गलक्षणानां सत्त्वादीनामानन्त्यमुक्तम्। एवमतिशयानामधिकृतपरिगणनायोगेऽप्यपरितत्त्वमविरुद्धम्। -स्याद्वादमञ्जरी,१/८/४ 1. देखें, पृ.५, टि.३ 2. केवलिना भुक्तिरस्ति, औदारिकशरीरसद्भावात्।...... अस्मदादिवत्। परिहारमाह-- तद्भगवतः शरीरमौदारिक न भवति किन्तु परमौदारिकम्-शुद्धस्फटिकसकाशं तेजोमूर्तिमयं वपुः। जायते क्षीणदोषस्य सप्तधातुविवर्जितम्। -प्र०सा०, ता०वृ०, 20/28/7 मानुषी प्रकृतिमभ्यतीतवान् देवतास्वपि देवतः यतः। तेन नाथ | परमासि देवता श्रेयसे जिनवृष ! प्रसीद नः।। -स्वयम्भूस्तोत्र 75.