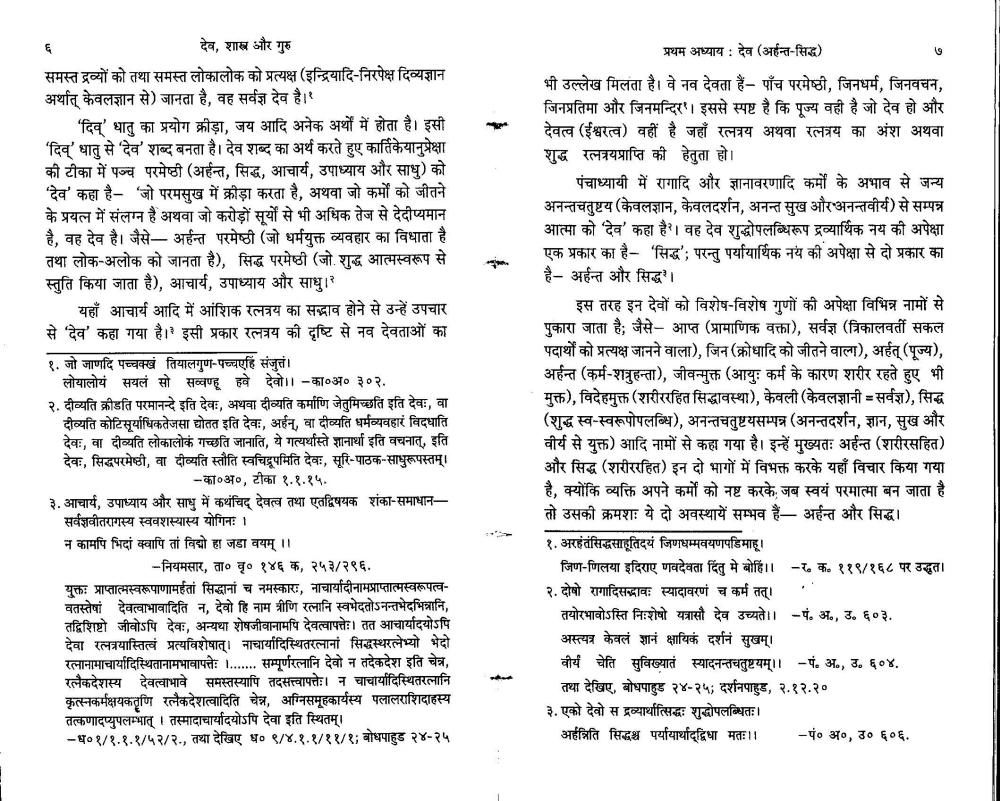________________ देव, शास्त्र और गुरु समस्त द्रव्यों को तथा समस्त लोकालोक को प्रत्यक्ष (इन्द्रियादि-निरपेक्ष दिव्यज्ञान अर्थात् केवलज्ञान से) जानता है, वह सर्वज्ञ देव है। ___"दिव्' धातु का प्रयोग क्रीड़ा, जय आदि अनेक अर्थों में होता है। इसी 'दिव्' धातु से 'देव' शब्द बनता है। देव शब्द का अर्थ करते हुए कार्तिकेयानुप्रेक्षा की टीका में पञ्च परमेष्ठी (अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु) को 'देव' कहा है- 'जो परमसुख में क्रीड़ा करता है, अथवा जो कर्मों को जीतने के प्रयल में संलग्न है अथवा जो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेज से देदीप्यमान है, वह देव है। जैसे- अर्हन्त परमेष्ठी (जो धर्मयुक्त व्यवहार का विधाता है तथा लोक-अलोक को जानता है), सिद्ध परमेष्ठी (जो. शुद्ध आत्मस्वरूप से स्तुति किया जाता है), आचार्य, उपाध्याय और साधु।२ / यहाँ आचार्य आदि में आंशिक रत्नत्रय का सद्भाव होने से उन्हें उपचार से 'देव' कहा गया है। इसी प्रकार रत्नत्रय की दृष्टि से नव देवताओं का 1. जो जाणदि पच्चक्खं तियालगुण-पच्चएहिं संजुत्तं। लोयालोयं सयलं सो सव्वण्हू हवे देवो।। -का०अ०३०२. 2. दीव्यति क्रीडति परमानन्दे इति देवः, अथवा दीव्यति कर्माणि जेतुमिच्छति इति देवा, वा दीव्यति कोटिसूर्याधिकतेजसा द्योतत इति देवः, अर्हन, वा दीव्यति धर्मव्यवहारं विदधाति देवा, वा दीव्यति लोकालोकं गच्छति जानाति, ये गत्यर्थास्ते ज्ञानार्था इति वचनात्, इति देवः, सिद्धपरमेष्ठी, वा दीव्यति स्तौति स्वचिद्रूपमिति देवः, सूरि-पाठक-साधुरूपस्तम्। -का०अ०, टीका 1.1.15. 3. आचार्य, उपाध्याय और साधु में कथंचिद् देवत्व तथा एतद्विषयक शंका-समाधान सर्वज्ञवीतरागस्य स्ववशस्यास्य योगिनः / न कामपि भिदां क्वापि तां विद्यो हा जडा वयम् / / -नियमसार, ता० वृ० 146 क, 253/296. युक्ता प्राप्तात्मस्वरूपाणामर्हता सिद्धानां च नमस्कार, नाचार्यादीनामप्राप्तात्मस्वरूपत्ववतस्तेषां देवत्वाभावादिति न, देवो हि नाम त्रीणि रत्नानि स्वभेदतोऽनन्तभेदभिन्नानि, तद्विशिष्टो जीवोऽपि देवा, अन्यथा शेषजीवानामपि देवत्वापत्तेः। तत आचार्यादयोऽपि देवा रत्नत्रयास्तित्वं प्रत्यविशेषात्। नाचार्यादिस्थितरलानां सिद्धस्थरलेभ्यो भेदो रलानामाचार्यादिस्थितानामभावापत्तेः / ....... सम्पूर्णरलानि देवो न तदेकदेश इति चेत्र, रत्लैकदेशस्य देवत्वाभावे समस्तस्यापि तदसत्त्वापत्तेः। न चाचार्यादिस्थितरत्नानि कृत्स्नकर्मक्षयकतृणि रलैकदेशत्वादिति चेन्न, अग्निसमूहकार्यस्य पलालराशिदाहस्य तत्कणादप्युपलम्भात् / तस्मादाचार्यादयोऽपि देवा इति स्थितम्। -501/1.1.1/52/2., तथा देखिए ध०९/४.१.१/११/१; बोधपाहुड 24-25 प्रथम अध्याय : देव (अर्हन्त-सिद्ध) भी उल्लेख मिलता है। वे नव देवता हैं- पाँच परमेष्ठी, जिनधर्म, जिनवचन, जिनप्रतिमा और जिनमन्दिर। इससे स्पष्ट है कि पूज्य वही है जो देव हो और देवत्व (ईश्वरत्व) वहीं है जहाँ रत्नत्रय अथवा रत्नत्रय का अंश अथवा शुद्ध रत्नत्रयप्राप्ति की हेतुता हो। पंचाध्यायी में रागादि और ज्ञानावरणादि कर्मों के अभाव से जन्य अनन्तचतुष्टय (केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्त सुख और अनन्तवीर्य) से सम्पन्न आत्मा को 'देव' कहा है। वह देव शुद्धोपलब्धिरूप द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा एक प्रकार का है- "सिद्ध'; परन्तु पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से दो प्रकार का है- अर्हन्त और सिद्ध। इस तरह इन देवों को विशेष-विशेष गुणों की अपेक्षा विभिन्न नामों से पुकारा जाता है; जैसे- आप्त (प्रामाणिक वक्ता), सर्वज्ञ (त्रिकालवी सकल पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाला), जिन (क्रोधादि को जीतने वाला), अर्हत् (पूज्य), अर्हन्त (कर्म-शत्रुहन्ता), जीवन्मुक्त (आयुः कर्म के कारण शरीर रहते हुए भी मुक्त), विदेहमुक्त (शरीररहित सिद्धावस्था), केवली (केवलज्ञानी = सर्वज्ञ), सिद्ध (शुद्ध स्व-स्वरूपोपलब्धि), अनन्तचतुष्टयसम्पन्न (अनन्तदर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य से युक्त) आदि नामों से कहा गया है। इन्हें मुख्यतः अर्हन्त (शरीरसहित) और सिद्ध (शरीररहित) इन दो भागों में विभक्त करके यहाँ विचार किया गया है, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों को नष्ट करके जब स्वयं परमात्मा बन जाता है तो उसकी क्रमशः ये दो अवस्थायें सम्भव हैं- अर्हन्त और सिद्ध। 1. अरहंतंसिद्धसाहूतिदयं जिणधम्मवयणपडिमाहू। जिण-णिलया इदिराए णवदेवता दितु मे बोहिं।। -र. क. 119/168 पर उद्धृत। 2. दोषो रागादिसद्भावः स्यादावरणं च कर्म तत्। ' तयोरभावोऽस्ति निःशेषो यत्रासौ देव उच्यते।। -पं. अ., उ. 603. अस्त्यत्र केवलं शानं क्षायिकं दर्शनं सुखम्। वीर्यं चेति सुविख्यातं स्यादनन्तचतुष्टयम्।। -पं. अ., उ. 604. तथा देखिए, बोधपाहुड 24-25, दर्शनपाहुड, 2.12.20 3. एको देवो स द्रव्यात्सिद्धः शुद्धोपलब्धितः। अर्हन्निति सिद्धश्च पर्यायार्थाविधा मतः।। -पं० अ०, उ०६०६.