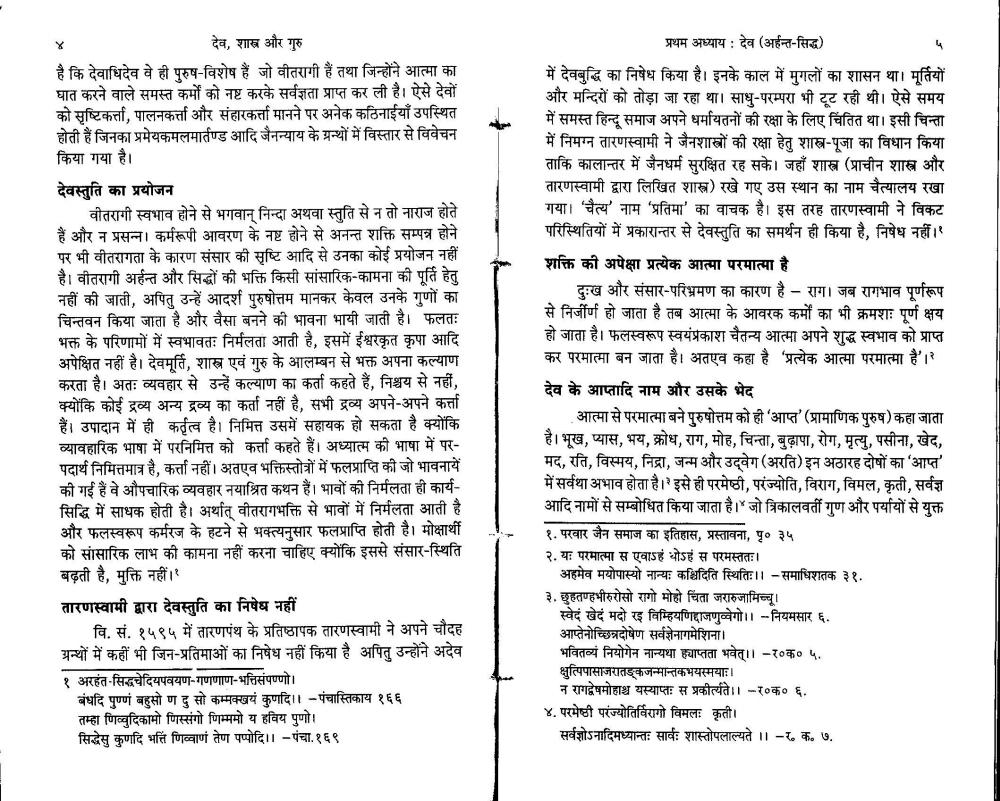________________ देव, शास्त्र और गुरु है कि देवाधिदेव वे ही पुरुष-विशेष हैं जो वीतरागी हैं तथा जिन्होंने आत्मा का घात करने वाले समस्त कर्मों को नष्ट करके सर्वज्ञता प्राप्त कर ली है। ऐसे देवों को सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता मानने पर अनेक कठिनाईयाँ उपस्थित होती हैं जिनका प्रमेयकमलमार्तण्ड आदि जैनन्याय के ग्रन्थों में विस्तार से विवेचन किया गया है। देवस्तुति का प्रयोजन वीतरागी स्वभाव होने से भगवान् निन्दा अथवा स्तुति से न तो नाराज होते हैं और न प्रसन्न। कर्मरूपी आवरण के नष्ट होने से अनन्त शक्ति सम्पन्न होने पर भी वीतरागता के कारण संसार की सृष्टि आदि से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। वीतरागी अर्हन्त और सिद्धों की भक्ति किसी सांसारिक-कामना की पूर्ति हेतु नहीं की जाती, अपितु उन्हें आदर्श पुरुषोत्तम मानकर केवल उनके गुणों का चिन्तवन किया जाता है और वैसा बनने की भावना भायी जाती है। फलतः भक्त के परिणामों में स्वभावतः निर्मलता आती है, इसमें ईश्वरकृत कृपा आदि अपेक्षित नहीं है। देवमूर्ति, शास्त्र एवं गुरु के आलम्बन से भक्त अपना कल्याण करता है। अतः व्यवहार से उन्हें कल्याण का कर्ता कहते हैं, निश्चय से नहीं, क्योंकि कोई द्रव्य अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है, सभी द्रव्य अपने-अपने कर्ता हैं। उपादान में ही कर्तृत्व है। निमित्त उसमें सहायक हो सकता है क्योंकि व्यावहारिक भाषा में परनिमित्त को कर्त्ता कहते हैं। अध्यात्म की भाषा में परपदार्थ निमित्तमात्र है, कर्त्ता नहीं। अतएव भक्तिस्तोत्रों में फलप्राप्ति की जो भावनायें की गई हैं वे औपचारिक व्यवहार नयाश्रित कथन हैं। भावों की निर्मलता ही कार्यसिद्धि में साधक होती है। अर्थात् वीतरागभक्ति से भावों में निर्मलता आती है और फलस्वरूप कर्मरज के हटने से भक्त्यनुसार फलप्राप्ति होती है। मोक्षार्थी को सांसारिक लाभ की कामना नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे संसार-स्थिति बढ़ती है, मुक्ति नहीं। तारणस्वामी द्वारा देवस्तुति का निषेध नहीं वि. सं. 1595 में तारणपंथ के प्रतिष्ठापक तारणस्वामी ने अपने चौदह ग्रन्थों में कहीं भी जिन-प्रतिमाओं का निषेध नहीं किया है अपितु उन्होंने अदेव 1 अरहंत-सिद्धचेदियपवयण-गणणाण-भत्तिसंपण्णो। बंधदि पुण्णं बहुसो ण दु सो कम्मक्खयं कणदि।। -पंचास्तिकाय 166 तम्हा णिव्वुदिकामो णिस्संगो णिम्ममो य हविय पुणो। सिद्धेसु कुणदि भत्ति णिव्वाणं तेण पप्पोदि।। -पंचा.१६९ प्रथम अध्याय : देव (अर्हन्त-सिद्ध) में देवबुद्धि का निषेध किया है। इनके काल में मुगलों का शासन था। मूर्तियों और मन्दिरों को तोड़ा जा रहा था। साधु-परम्परा भी टूट रही थी। ऐसे समय में समस्त हिन्दू समाज अपने धर्मायतनों की रक्षा के लिए चिंतित था। इसी चिन्ता में निमग्न तारणस्वामी ने जैनशास्त्रों की रक्षा हेतु शास्त्र-पूजा का विधान किया ताकि कालान्तर में जैनधर्म सुरक्षित रह सके। जहाँ शास्त्र (प्राचीन शास्त्र और तारणस्वामी द्वारा लिखित शास्त्र) रखे गए उस स्थान का नाम चैत्यालय रखा गया। 'चैत्य' नाम 'प्रतिमा' का वाचक है। इस तरह तारणस्वामी ने विकट परिस्थितियों में प्रकारान्तर से देवस्तुति का समर्थन ही किया है, निषेध नहीं।' शक्ति की अपेक्षा प्रत्येक आत्मा परमात्मा है दुःख और संसार-परिभ्रमण का कारण है - राग। जब रागभाव पूर्णरूप से निर्जीर्ण हो जाता है तब आत्मा के आवरक कर्मों का भी क्रमशः पूर्ण क्षय हो जाता है। फलस्वरूप स्वयंप्रकाश चैतन्य आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर परमात्मा बन जाता है। अतएव कहा है 'प्रत्येक आत्मा परमात्मा है'। देव के आप्तादि नाम और उसके भेद ___ आत्मा से परमात्मा बने पुरुषोत्तम को ही 'आप्त' (प्रामाणिक पुरुष) कहा जाता है। भूख, प्यास, भय, क्रोध, राग, मोह, चिन्ता, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, पसीना, खेद, मद, रति, विस्मय, निद्रा, जन्म और उद्वेग (अरति) इन अठारह दोषों का 'आप्त' में सर्वथा अभाव होता है। इसे ही परमेष्ठी, परंज्योति, विराग, विमल, कृती, सर्वज्ञ आदि नामों से सम्बोधित किया जाता है। जो त्रिकालवर्ती गुण और पर्यायों से युक्त 1. परवार जैन समाज का इतिहास, प्रस्तावना, पृ० 35 2. या परमात्मा स एवाऽहं थोऽहं स परमस्ततः। अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः।। -समाधिशतक 31. 3. छुहतण्हभीरुरोसो रागो मोहो चिंता जरारुजामिच्चू। स्वेदं खेदं मदो रइ विम्हियणिहाजणुव्वेगो।। -नियमसार 6. आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना। भवितव्यं नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्।। -र०क० 5. क्षुत्पिपासाजरातङ्कजन्मान्तकभयस्मया। न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते।। -र०क०६. 4. परमेष्ठी परंज्योतिर्विरागो विमल: कृती। सर्वज्ञोऽनादिमध्यान्तः सार्वः शास्तोपलाल्यते / / -र. क. 7.