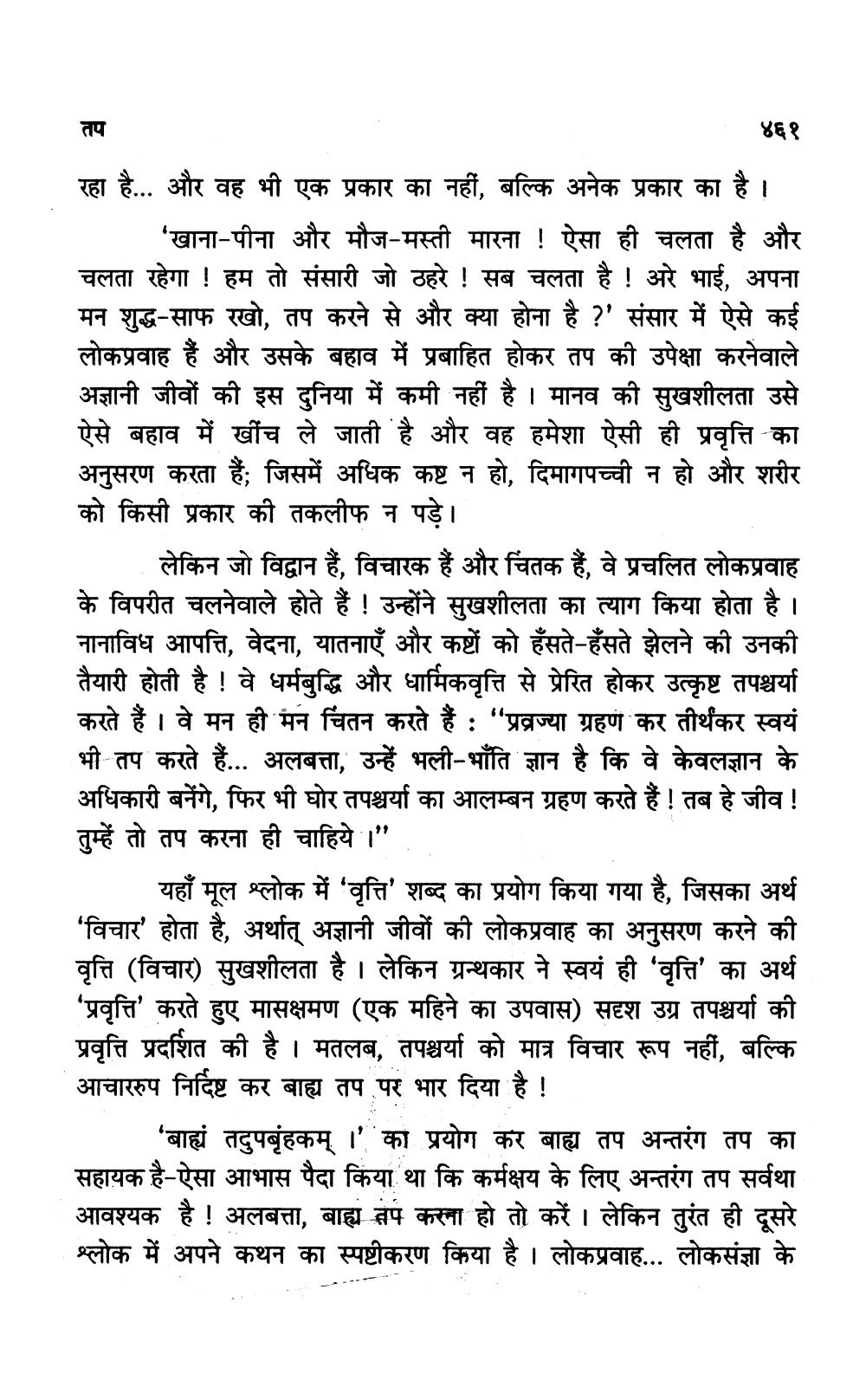________________
४६१ रहा है... और वह भी एक प्रकार का नहीं, बल्कि अनेक प्रकार का है।
'खाना-पीना और मौज-मस्ती मारना ! ऐसा ही चलता है और चलता रहेगा ! हम तो संसारी जो ठहरे ! सब चलता है ! अरे भाई, अपना मन शुद्ध-साफ रखो, तप करने से और क्या होना है ?' संसार में ऐसे कई लोकप्रवाह हैं और उसके बहाव में प्रवाहित होकर तप की उपेक्षा करनेवाले अज्ञानी जीवों की इस दुनिया में कमी नहीं है । मानव की सुखशीलता उसे ऐसे बहाव में खींच ले जाती है और वह हमेशा ऐसी ही प्रवृत्ति का अनुसरण करता हैं; जिसमें अधिक कष्ट न हो, दिमागपच्ची न हो और शरीर को किसी प्रकार की तकलीफ न पड़े।
लेकिन जो विद्वान हैं, विचारक हैं और चिंतक हैं, वे प्रचलित लोकप्रवाह के विपरीत चलनेवाले होते हैं ! उन्होंने सुखशीलता का त्याग किया होता है । नानाविध आपत्ति, वेदना, यातनाएँ और कष्टों को हँसते-हँसते झेलने की उनकी तैयारी होती है ! वे धर्मबुद्धि और धार्मिकवृत्ति से प्रेरित होकर उत्कृष्ट तपश्चर्या करते हैं । वे मन ही मन चिंतन करते हैं : "प्रव्रज्या ग्रहण कर तीर्थंकर स्वयं भी तप करते हैं... अलबत्ता, उन्हें भली-भाँति ज्ञान है कि वे केवलज्ञान के अधिकारी बनेंगे, फिर भी घोर तपश्चर्या का आलम्बन ग्रहण करते हैं ! तब हे जीव! तुम्हें तो तप करना ही चाहिये ।" ...
यहाँ मूल श्लोक में 'वृत्ति' शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ 'विचार' होता है, अर्थात् अज्ञानी जीवों की लोकप्रवाह का अनुसरण करने की वृत्ति (विचार) सुखशीलता है । लेकिन ग्रन्थकार ने स्वयं ही 'वृत्ति' का अर्थ 'प्रवृत्ति' करते हुए मासक्षमण (एक महिने का उपवास) सदृश उग्र तपश्चर्या की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है । मतलब, तपश्चर्या को मात्र विचार रूप नहीं, बल्कि आचाररुप निर्दिष्ट कर बाह्य तप पर भार दिया है !
___ 'बाह्यं तदुपबंहकम् ।' का प्रयोग कर बाह्य तप अन्तरंग तप का सहायक है-ऐसा आभास पैदा किया था कि कर्मक्षय के लिए अन्तरंग तप सर्वथा आवश्यक है ! अलबत्ता, बाह्य तप करना हो तो करें । लेकिन तुरंत ही दूसरे श्लोक में अपने कथन का स्पष्टीकरण किया है। लोकप्रवाह... लोकसंज्ञा के