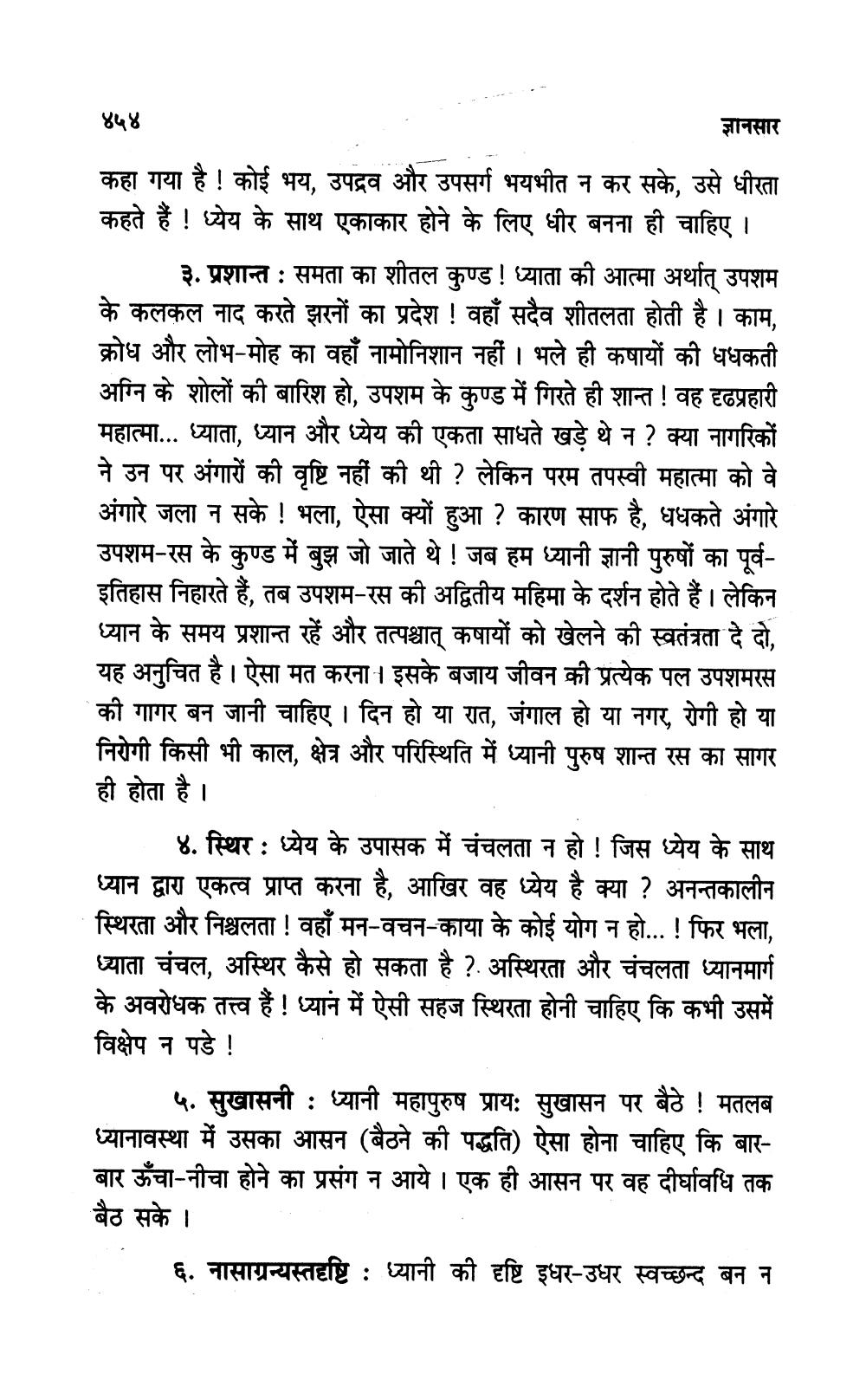________________
४५४
ज्ञानसार
कहा गया है ! कोई भय, उपद्रव और उपसर्ग भयभीत न कर सके, उसे धीरता कहते हैं ! ध्येय के साथ एकाकार होने के लिए धीर बनना ही चाहिए ।
३. प्रशान्त: समता का शीतल कुण्ड ! ध्याता की आत्मा अर्थात् उपशम के कलकल नाद करते झरनों का प्रदेश ! वहाँ सदैव शीतलता होती है । काम, क्रोध और लोभ-मोह का वहाँ नामोनिशान नहीं । भले ही कषायों की धधकती अग्नि के शोलों की बारिश हो, उपशम के कुण्ड में गिरते ही शान्त ! वह दृढप्रहारी महात्मा... ध्याता, ध्यान और ध्येय की एकता साधते खड़े थे न ? क्या नागरिकों ने उन पर अंगारों की वृष्टि नहीं की थी ? लेकिन परम तपस्वी महात्मा को वे अंगारे जला न सके ! भला, ऐसा क्यों हुआ ? कारण साफ है, धधकते अंगारे उपशम-रस के कुण्ड में बुझ जो जाते थे ! जब हम ध्यानी ज्ञानी पुरुषों का पूर्व - इतिहास निहारते हैं, तब उपशम-रस की अद्वितीय महिमा के दर्शन होते हैं। लेकिन ध्यान के समय प्रशान्त रहें और तत्पश्चात् कषायों को खेलने की स्वतंत्रता दे दो, यह अनुचित है । ऐसा मत करना । इसके बजाय जीवन की प्रत्येक पल उपशमरस की गागर बन जानी चाहिए। दिन हो या रात, जंगाल हो या नगर, रोगी हो या निरोगी किसी भी काल, क्षेत्र और परिस्थिति में ध्यानी पुरुष शान्त रस का सागर
होता है ।
४. स्थिर : ध्येय के उपासक में चंचलता न हो ! जिस ध्येय के साथ ध्यान द्वारा एकत्व प्राप्त करना है, आखिर वह ध्येय है क्या ? अनन्तकालीन स्थिरता और निश्चलता ! वहाँ मन-वचन-काया के कोई योग न हो... ! फिर भला, ध्याता चंचल, अस्थिर कैसे हो सकता है ? अस्थिरता और चंचलता ध्यानमार्ग के अवरोधक तत्त्व हैं ! ध्यान में ऐसी सहज स्थिरता होनी चाहिए कि कभी उसमें विक्षेप न पडे !
५. सुखासनी : ध्यानी महापुरुष प्रायः सुखासन पर बैठे ! मतलब ध्यानावस्था में उसका आसन (बैठने की पद्धति) ऐसा होना चाहिए कि बारबार ऊँचा - नीचा होने का प्रसंग न आये । एक ही आसन पर वह दीर्घावधि तक बैठ सके ।
६. नासाग्रन्यस्तदृष्टि : ध्यानी की दृष्टि इधर-उधर स्वच्छन्द बन न