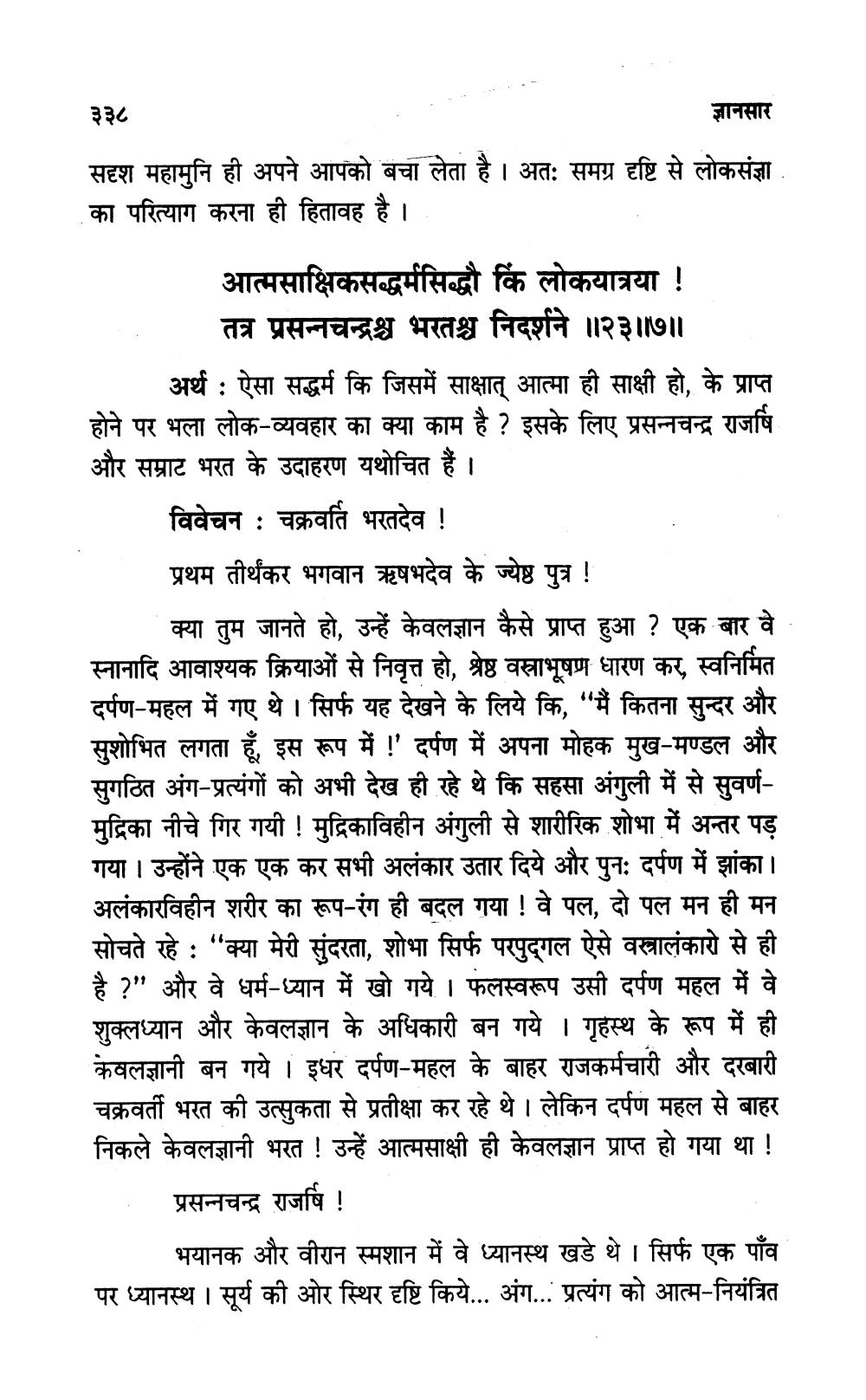________________
३३८
ज्ञानसार
सदृश महामुनि ही अपने आपको बचा लेता है । अतः समग्र दृष्टि से लोकसंज्ञा . का परित्याग करना ही हितावह है।
आत्मसाक्षिकसद्धर्मसिद्धौ किं लोकयात्रया !
तत्र प्रसन्नचन्द्रश्च भरतश्च निदर्शने ॥२३॥७॥
अर्थ : ऐसा सद्धर्म कि जिसमें साक्षात् आत्मा ही साक्षी हो, के प्राप्त होने पर भला लोक-व्यवहार का क्या काम है ? इसके लिए प्रसन्नचन्द्र राजर्षि और सम्राट भरत के उदाहरण यथोचित हैं ।
विवेचन : चक्रवर्ति भरतदेव ! प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र !
क्या तुम जानते हो, उन्हें केवलज्ञान कैसे प्राप्त हुआ ? एक बार वे : स्नानादि आवाश्यक क्रियाओं से निवृत्त हो, श्रेष्ठ वस्राभूषण धारण कर, स्वनिर्मित दर्पण-महल में गए थे। सिर्फ यह देखने के लिये कि, "मैं कितना सुन्दर और सुशोभित लगता हूँ, इस रूप में !' दर्पण में अपना मोहक मुख-मण्डल और सुगठित अंग-प्रत्यंगों को अभी देख ही रहे थे कि सहसा अंगुली में से सुवर्णमुद्रिका नीचे गिर गयी ! मुद्रिकाविहीन अंगुली से शारीरिक शोभा में अन्तर पड़ गया। उन्होंने एक एक कर सभी अलंकार उतार दिये और पुनः दर्पण में झांका। अलंकारविहीन शरीर का रूप-रंग ही बदल गया ! वे पल, दो पल मन ही मन सोचते रहे : "क्या मेरी सुंदरता, शोभा सिर्फ परपुद्गल ऐसे वस्त्रालंकारो से ही है ?" और वे धर्म-ध्यान में खो गये । फलस्वरूप उसी दर्पण महल में वे शुक्लध्यान और केवलज्ञान के अधिकारी बन गये । गृहस्थ के रूप में ही केवलज्ञानी बन गये । इधर दर्पण-महल के बाहर राजकर्मचारी और दरबारी चक्रवर्ती भरत की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन दर्पण महल से बाहर निकले केवलज्ञानी भरत ! उन्हें आत्मसाक्षी ही केवलज्ञान प्राप्त हो गया था !
प्रसन्नचन्द्र राजर्षि !
भयानक और वीरान स्मशान में वे ध्यानस्थ खडे थे । सिर्फ एक पाँव पर ध्यानस्थ । सूर्य की ओर स्थिर दृष्टि किये... अंग... प्रत्यंग को आत्म-नियंत्रित