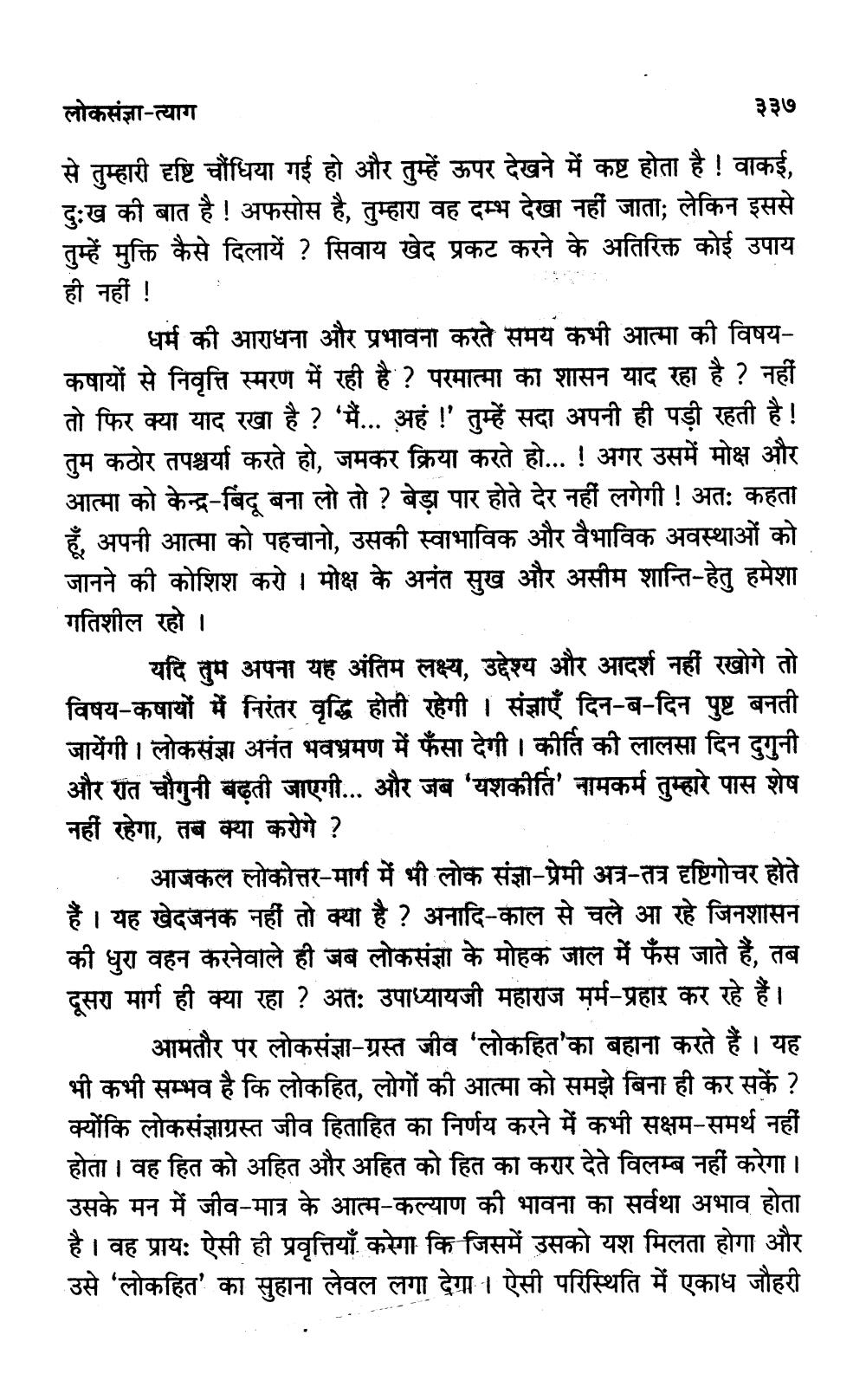________________
लोकसंज्ञा-त्याग
३३७ से तुम्हारी दृष्टि चौंधिया गई हो और तुम्हें ऊपर देखने में कष्ट होता है ! वाकई, दुःख की बात है ! अफसोस है, तुम्हारा वह दम्भ देखा नहीं जाता; लेकिन इससे तुम्हें मुक्ति कैसे दिलायें ? सिवाय खेद प्रकट करने के अतिरिक्त कोई उपाय ही नहीं !
धर्म की आराधना और प्रभावना करते समय कभी आत्मा की विषयकषायों से निवत्ति स्मरण में रही है? परमात्मा का शासन याद रहा है? नहीं तो फिर क्या याद रखा है ? 'मैं... अहं !' तुम्हें सदा अपनी ही पड़ी रहती है ! तुम कठोर तपश्चर्या करते हो, जमकर क्रिया करते हो... ! अगर उसमें मोक्ष और आत्मा को केन्द्र-बिंदू बना लो तो? बेड़ा पार होते देर नहीं लगेगी ! अतः कहता हूँ, अपनी आत्मा को पहचानो, उसकी स्वाभाविक और वैभाविक अवस्थाओं को जानने की कोशिश करो । मोक्ष के अनंत सुख और असीम शान्ति-हेतु हमेशा गतिशील रहो ।
यदि तुम अपना यह अंतिम लक्ष्य, उद्देश्य और आदर्श नहीं रखोगे तो विषय-कषायों में निरंतर वृद्धि होती रहेगी । संज्ञाएँ दिन-ब-दिन पुष्ट बनती जायेंगी। लोकसंज्ञा अनंत भवभ्रमण में फँसा देगी। कीर्ति की लालसा दिन दुगुनी
और रात चौगनी बढती जाएगी... और जब 'यशकीति' नामकर्म तुम्हारे पास शेष नहीं रहेगा, तब क्या करोगे?
- आजकल लोकोत्तर-मार्ग में भी लोक संज्ञा-प्रेमी अत्र-तत्र दृष्टिगोचर होते हैं । यह खेदजनक नहीं तो क्या है ? अनादि-काल से चले आ रहे जिनशासन की धुरा वहन करनेवाले ही जब लोकसंज्ञा के मोहक जाल में फँस जाते हैं, तब दूसरा मार्ग ही क्या रहा ? अत: उपाध्यायजी महाराज मर्म-प्रहार कर रहे हैं।
आमतौर पर लोकसंज्ञा-ग्रस्त जीव 'लोकहित'का बहाना करते हैं। यह भी कभी सम्भव है कि लोकहित, लोगों की आत्मा को समझे बिना ही कर सकें? क्योंकि लोकसंज्ञाग्रस्त जीव हिताहित का निर्णय करने में कभी सक्षम-समर्थ नहीं होता । वह हित को अहित और अहित को हित का करार देते विलम्ब नहीं करेगा। उसके मन में जीव-मात्र के आत्म-कल्याण की भावना का सर्वथा अभाव होता है। वह प्रायः ऐसी ही प्रवृत्तियाँ करेगा कि जिसमें उसको यश मिलता होगा और उसे 'लोकहित' का सुहाना लेवल लगा देगा । ऐसी परिस्थिति में एकाध जौहरी