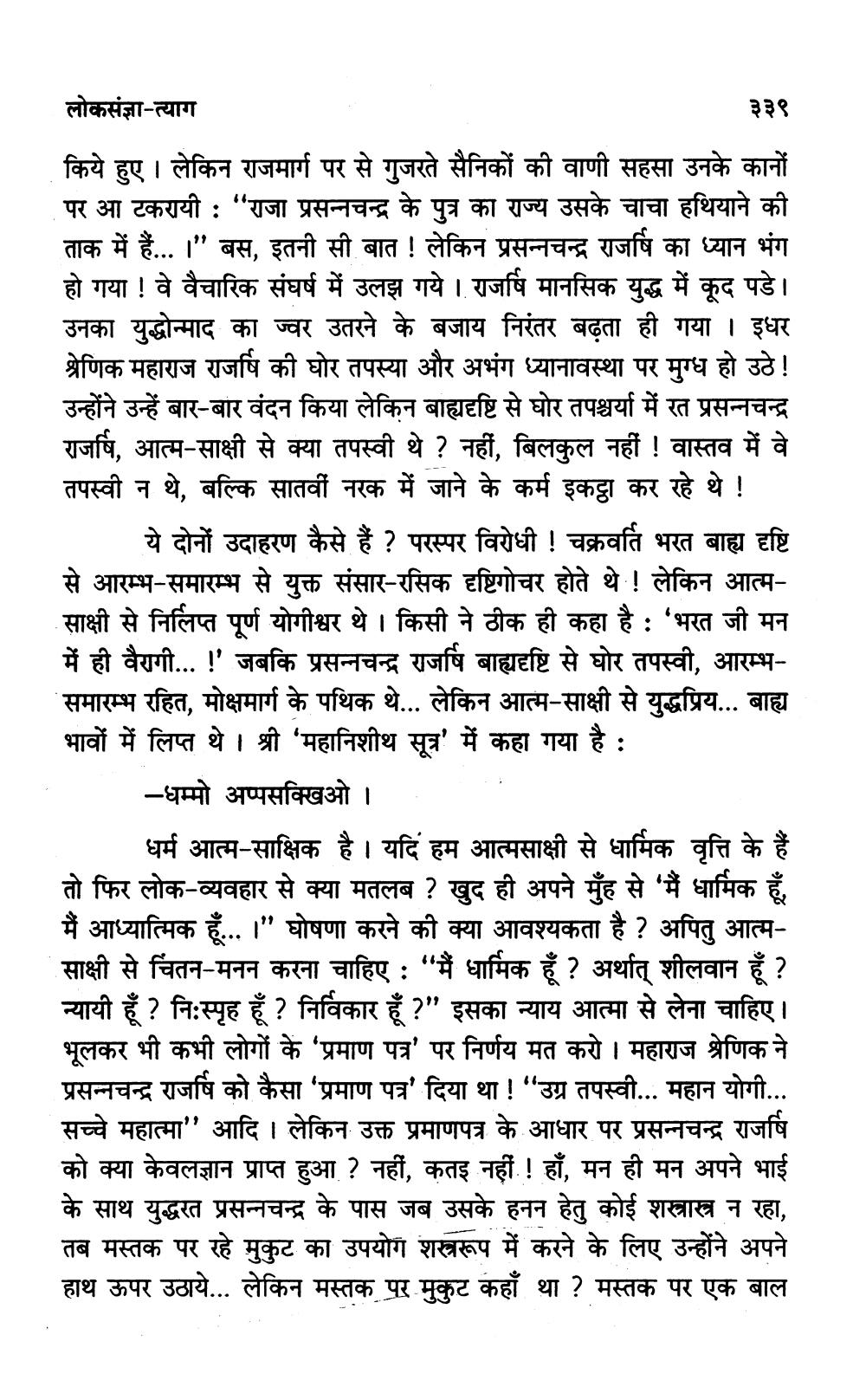________________
लोकसंज्ञा-त्याग
३३९
किये हुए। लेकिन राजमार्ग पर से गुजरते सैनिकों की वाणी सहसा उनके कानों पर आ टकरायी : " राजा प्रसन्नचन्द्र के पुत्र का राज्य उसके चाचा हथियाने की ताक में हैं... ।" बस, इतनी सी बात ! लेकिन प्रसन्नचन्द्र राजर्षि का ध्यान भंग हो गया ! वे वैचारिक संघर्ष में उलझ गये । राजर्षि मानसिक युद्ध में कूद पडे । उनका युद्धोन्माद का ज्वर उतरने के बजाय निरंतर बढ़ता ही गया । इधर श्रेणिक महाराज राजर्षि की घोर तपस्या और अभंग ध्यानावस्था पर मुग्ध हो उठे ! उन्होंने उन्हें बार-बार वंदन किया लेकिन बाह्यदृष्टि से घोर तपश्चर्या में रत प्रसन्नचन्द्र राजर्षि, आत्म-साक्षी से क्या तपस्वी थे ? नहीं, बिलकुल नहीं ! वास्तव में वे तपस्वी न थे, बल्कि सातवीं नरक में जाने के कर्म इकट्ठा कर रहे थे !
ये दोनों उदाहरण कैसे हैं ? परस्पर विरोधी ! चक्रवर्ति भरत बाह्य दृष्टि से आरम्भ - समारम्भ से युक्त संसार - रसिक दृष्टिगोचर होते थे ! लेकिन आत्मसाक्षी से निर्लिप्त पूर्ण योगीश्वर थे । किसी ने ठीक ही कहा है : 'भरत जी मन में ही वैरागी... !' जबकि प्रसन्नचन्द्र राजर्षि बाह्यदृष्टि से घोर तपस्वी, आरम्भसमारम्भ रहित, मोक्षमार्ग के पथिक थे... लेकिन आत्म- साक्षी से युद्धप्रिय... बाह्य भावों में लिप्त थे । श्री 'महानिशीथ सूत्र' में कहा गया है :
I
- धम्मो अप्पसक्खिओ ।
धर्म आत्म-साक्षिक है। यदि हम आत्मसाक्षी से धार्मिक वृत्ति के हैं तो फिर लोक-व्यवहार से क्या मतलब ? खुद ही अपने मुँह से 'मैं धार्मिक हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ... ।” घोषणा करने की क्या आवश्यकता है ? अपितु आत्मसाक्षी से चिंतन-मनन करना चाहिए : "मैं धार्मिक हूँ ? अर्थात् शीलवान हूँ ? न्यायी हूँ ? नि:स्पृह हूँ ? निर्विकार हूँ ?" इसका न्याय आत्मा से लेना चाहिए। भूलकर भी कभी लोगों के 'प्रमाण पत्र' पर निर्णय मत करो । महाराज श्रेणिक ने प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को कैसा 'प्रमाण पत्र' दिया था ! "उग्र तपस्वी ... महान योगी.... सच्चे महात्मा” आदि । लेकिन उक्त प्रमाणपत्र के आधार पर प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को क्या केवलज्ञान प्राप्त हुआ ? नहीं, कतई नहीं ! हाँ, मन ही मन अपने भाई के साथ युद्धरत प्रसन्नचन्द्र के पास जब उसके हनन हेतु कोई शस्त्रास्त्र न रहा, तब मस्तक पर रहे मुकुट का उपयोग शस्त्ररूप में करने के लिए उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाये... लेकिन मस्तक पर मुकुट कहाँ था ? मस्तक पर एक बाल