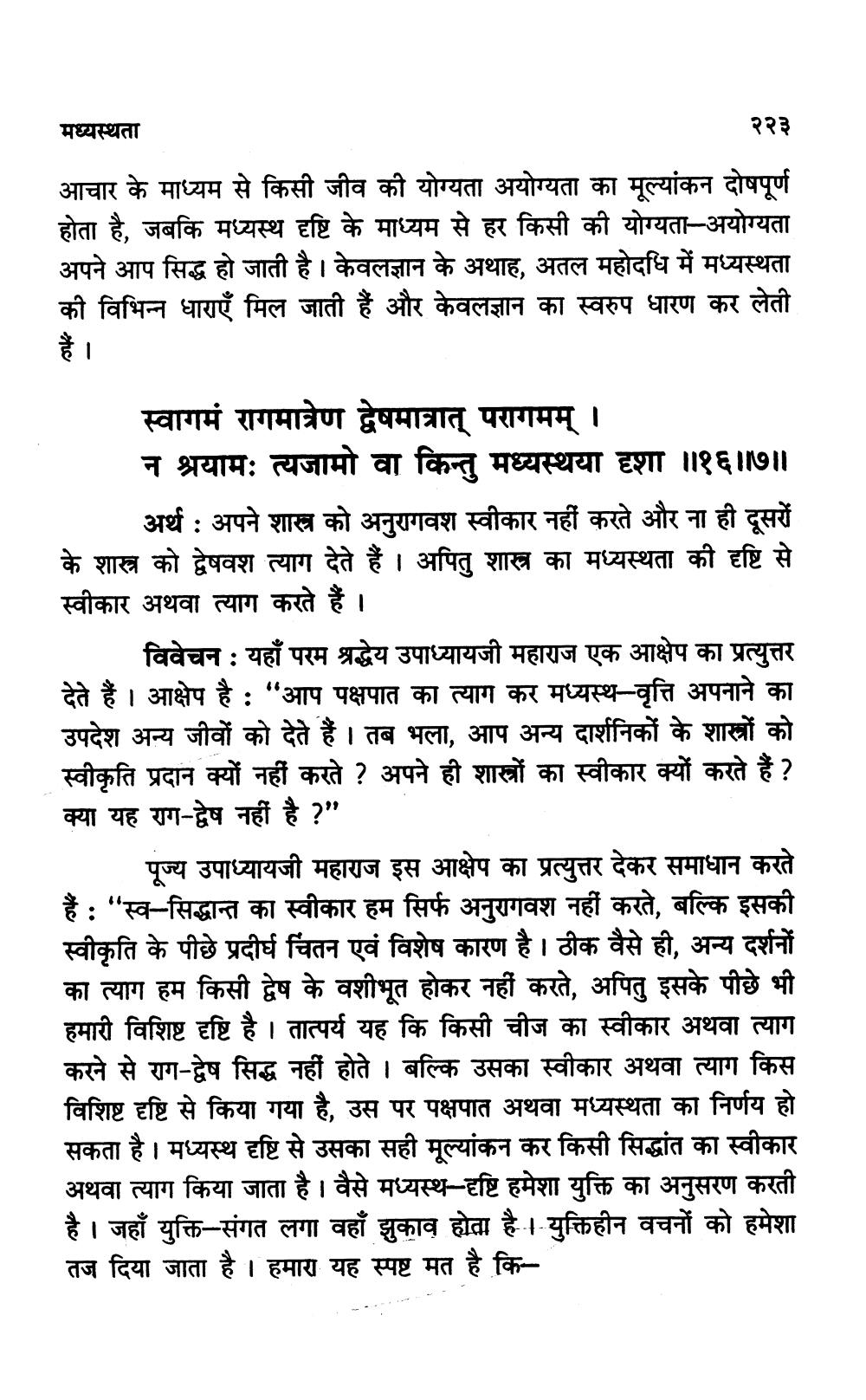________________
मध्यस्थता
२२३
आचार के माध्यम से किसी जीव की योग्यता अयोग्यता का मूल्यांकन दोषपूर्ण होता है, जबकि मध्यस्थ दृष्टि के माध्यम से हर किसी की योग्यता-अयोग्यता अपने आप सिद्ध हो जाती है। केवलज्ञान के अथाह, अतल महोदधि में मध्यस्थता की विभिन्न धाराएँ मिल जाती हैं और केवलज्ञान का स्वरुप धारण कर लेती
हैं।
स्वागमं रागमात्रेण द्वेषमात्रात् परागमम् । न श्रयामः त्यजामो वा किन्तु मध्यस्थया दृशा ॥१६॥७॥
अर्थ : अपने शास्त्र को अनुरागवश स्वीकार नहीं करते और ना ही दूसरों के शास्त्र को द्वेषवश त्याग देते हैं । अपितु शास्त्र का मध्यस्थता की दृष्टि से स्वीकार अथवा त्याग करते हैं।
विवेचन : यहाँ परम श्रद्धेय उपाध्यायजी महाराज एक आक्षेप का प्रत्युत्तर देते हैं । आक्षेप है : "आप पक्षपात का त्याग कर मध्यस्थ-वृत्ति अपनाने का उपदेश अन्य जीवों को देते हैं । तब भला, आप अन्य दार्शनिकों के शास्त्रों को स्वीकृति प्रदान क्यों नहीं करते ? अपने ही शास्त्रों का स्वीकार क्यों करते हैं? क्या यह राग-द्वेष नहीं है ?"
पूज्य उपाध्यायजी महाराज इस आक्षेप का प्रत्युत्तर देकर समाधान करते हैं : "स्व-सिद्धान्त का स्वीकार हम सिर्फ अनुरागवश नहीं करते, बल्कि इसकी स्वीकृति के पीछे प्रदीर्घ चिंतन एवं विशेष कारण है। ठीक वैसे ही, अन्य दर्शनों का त्याग हम किसी द्वेष के वशीभूत होकर नहीं करते, अपितु इसके पीछे भी हमारी विशिष्ट दृष्टि है । तात्पर्य यह कि किसी चीज का स्वीकार अथवा त्याग करने से राग-द्वेष सिद्ध नहीं होते । बल्कि उसका स्वीकार अथवा त्याग किस विशिष्ट दृष्टि से किया गया है, उस पर पक्षपात अथवा मध्यस्थता का निर्णय हो सकता है। मध्यस्थ दृष्टि से उसका सही मूल्यांकन कर किसी सिद्धांत का स्वीकार अथवा त्याग किया जाता है। वैसे मध्यस्थ-दृष्टि हमेशा युक्ति का अनुसरण करती है । जहाँ युक्ति-संगत लगा वहाँ झुकाव होता है । युक्तिहीन वचनों को हमेशा तज दिया जाता है। हमारा यह स्पष्ट मत है कि