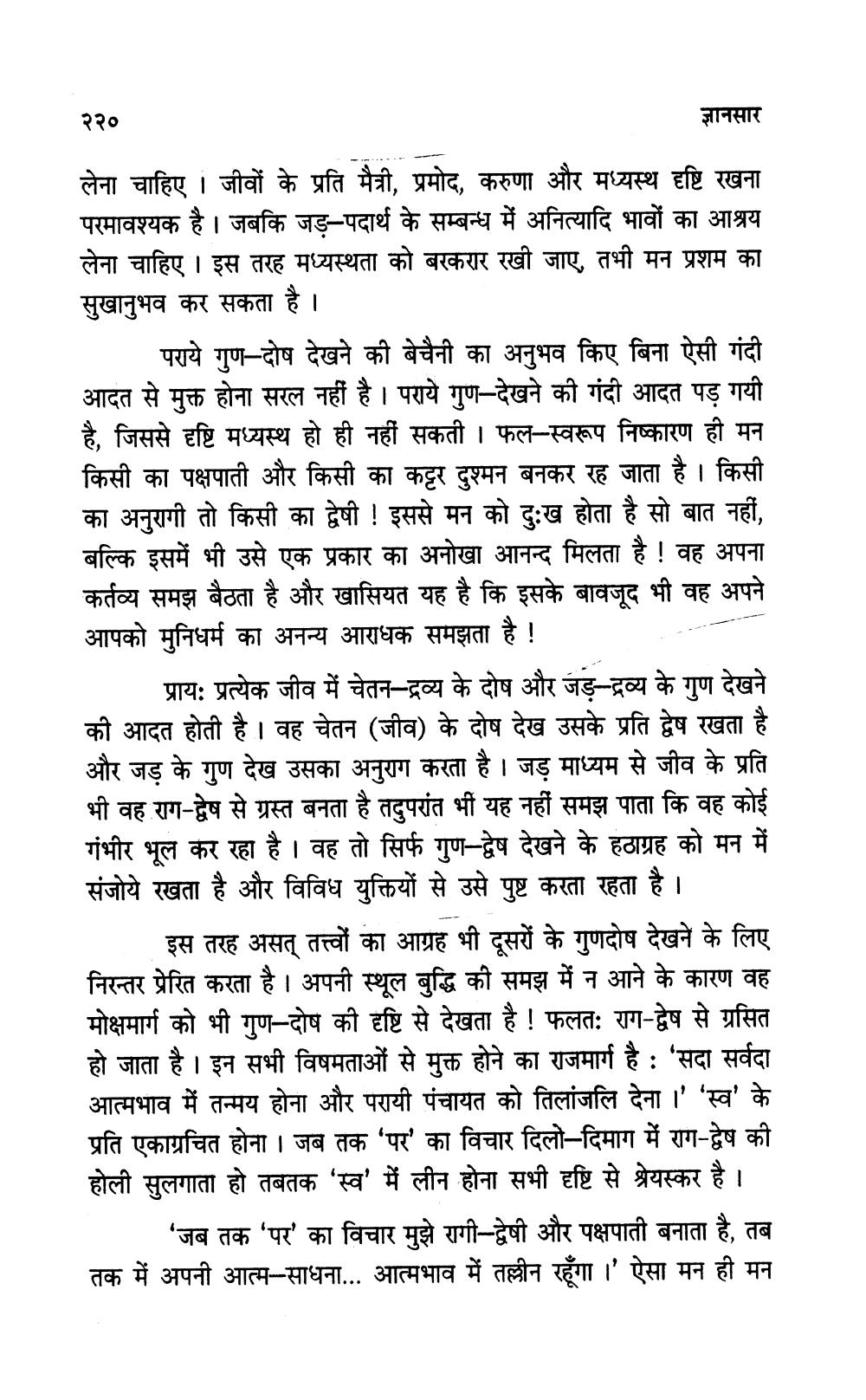________________
२२०
ज्ञानसार
लेना चाहिए । जीवों के प्रति मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ दृष्टि रखना परमावश्यक है। जबकि जड़-पदार्थ के सम्बन्ध में अनित्यादि भावों का आश्रय लेना चाहिए । इस तरह मध्यस्थता को बरकरार रखी जाए, तभी मन प्रशम का सुखानुभव कर सकता है।
पराये गुण-दोष देखने की बेचैनी का अनुभव किए बिना ऐसी गंदी आदत से मुक्त होना सरल नहीं है । पराये गुण-देखने की गंदी आदत पड़ गयी है, जिससे दृष्टि मध्यस्थ हो ही नहीं सकती । फल-स्वरूप निष्कारण ही मन किसी का पक्षपाती और किसी का कट्टर दुश्मन बनकर रह जाता है । किसी का अनुरागी तो किसी का द्वेषी ! इससे मन को दुःख होता है सो बात नहीं, बल्कि इसमें भी उसे एक प्रकार का अनोखा आनन्द मिलता है ! वह अपना कर्तव्य समझ बैठता है और खासियत यह है कि इसके बावजूद भी वह अपने आपको मुनिधर्म का अनन्य आराधक समझता है !
प्रायः प्रत्येक जीव में चेतन-द्रव्य के दोष और जड़-द्रव्य के गुण देखने की आदत होती है । वह चेतन (जीव) के दोष देख उसके प्रति द्वेष रखता है और जड़ के गुण देख उसका अनुराग करता है। जड़ माध्यम से जीव के प्रति भी वह राग-द्वेष से ग्रस्त बनता है तदुपरांत भी यह नहीं समझ पाता कि वह कोई गंभीर भूल कर रहा है । वह तो सिर्फ गुण-द्वेष देखने के हठाग्रह को मन में संजोये रखता है और विविध युक्तियों से उसे पुष्ट करता रहता है ।
___ इस तरह असत् तत्त्वों का आग्रह भी दूसरों के गुणदोष देखने के लिए निरन्तर प्रेरित करता है। अपनी स्थूल बुद्धि की समझ में न आने के कारण वह मोक्षमार्ग को भी गुण-दोष की दृष्टि से देखता है ! फलतः राग-द्वेष से ग्रसित हो जाता है । इन सभी विषमताओं से मुक्त होने का राजमार्ग है : 'सदा सर्वदा आत्मभाव में तन्मय होना और परायी पंचायत को तिलांजलि देना ।' 'स्व' के प्रति एकाग्रचित होना । जब तक 'पर' का विचार दिलो-दिमाग में राग-द्वेष की होली सुलगाता हो तबतक 'स्व' में लीन होना सभी दृष्टि से श्रेयस्कर है।
'जब तक 'पर' का विचार मुझे रागी-द्वेषी और पक्षपाती बनाता है, तब तक में अपनी आत्म-साधना... आत्मभाव में तल्लीन रहूँगा।' ऐसा मन ही मन