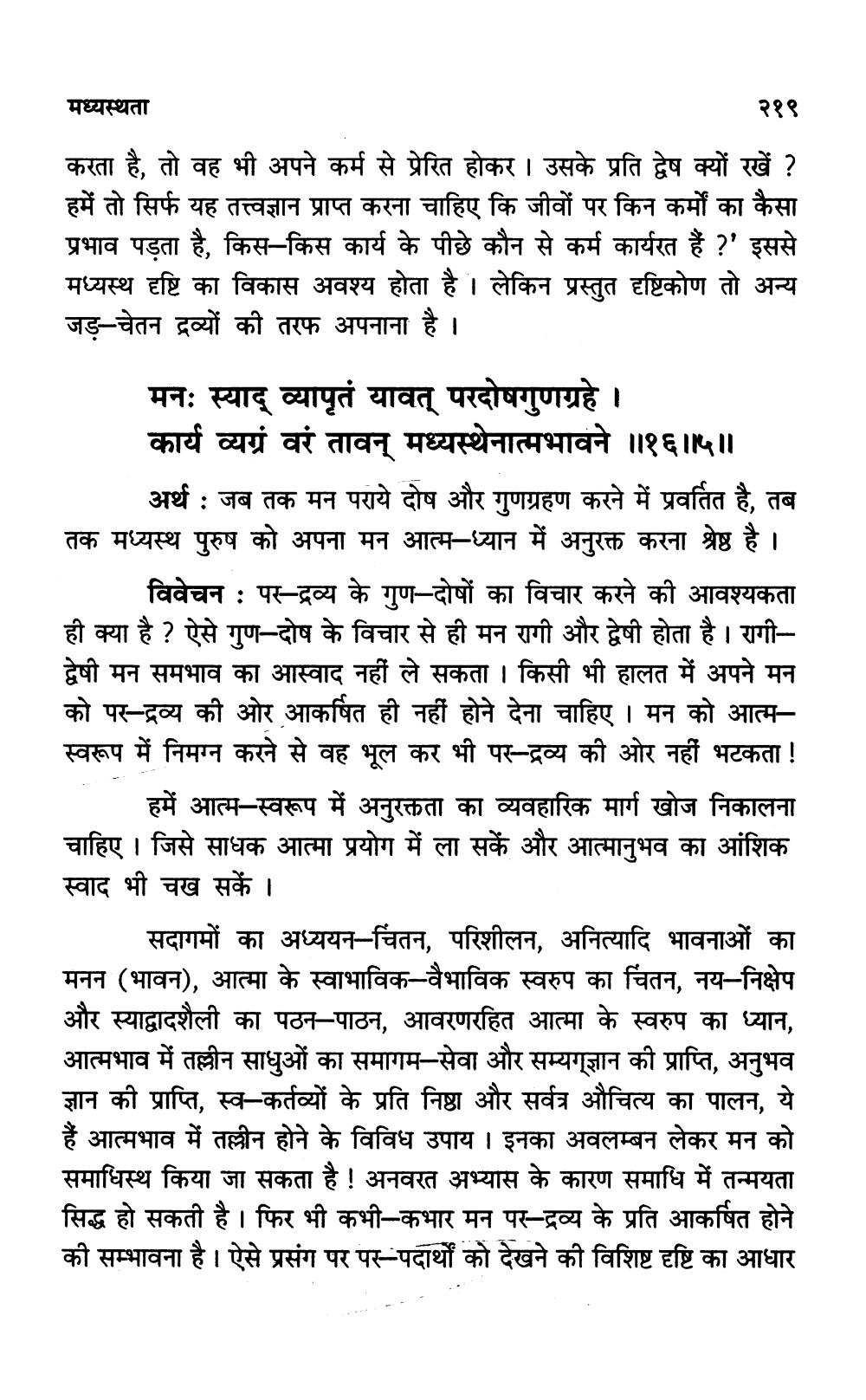________________
मध्यस्थता
२१९
करता है, तो वह भी अपने कर्म से प्रेरित होकर । उसके प्रति द्वेष क्यों रखें ? हमें तो सिर्फ यह तत्त्वज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि जीवों पर किन कर्मों का कैसा प्रभाव पड़ता है, किस-किस कार्य के पीछे कौन से कर्म कार्यरत हैं ?' इससे मध्यस्थ दृष्टि का विकास अवश्य होता है। लेकिन प्रस्तुत दृष्टिकोण तो अन्य जङ-चेतन द्रव्यों की तरफ अपनाना है।
मनः स्याद् व्यापृतं यावत् परदोषगुणग्रहे । कार्य व्यग्रं वरं तावन् मध्यस्थेनात्मभावने ॥१६॥५॥
अर्थ : जब तक मन पराये दोष और गुणग्रहण करने में प्रवर्तित है, तब तक मध्यस्थ पुरुष को अपना मन आत्म-ध्यान में अनुरक्त करना श्रेष्ठ है ।
विवेचन : पस्-द्रव्य के गुण-दोषों का विचार करने की आवश्यकता ही क्या है ? ऐसे गुण-दोष के विचार से ही मन रागी और द्वेषी होता है। रागीद्वेषी मन समभाव का आस्वाद नहीं ले सकता । किसी भी हालत में अपने मन को पर-द्रव्य की ओर आकर्षित ही नहीं होने देना चाहिए । मन को आत्मस्वरूप में निमग्न करने से वह भूल कर भी पर-द्रव्य की ओर नहीं भटकता!
हमें आत्म-स्वरूप में अनुरक्तता का व्यवहारिक मार्ग खोज निकालना चाहिए । जिसे साधक आत्मा प्रयोग में ला सकें और आत्मानुभव का आंशिक स्वाद भी चख सकें।
सदागमों का अध्ययन-चिंतन, परिशीलन, अनित्यादि भावनाओं का मनन (भावन), आत्मा के स्वाभाविक-वैभाविक स्वरुप का चिंतन, नय-निक्षेप और स्याद्वादशैली का पठन-पाठन, आवरणरहित आत्मा के स्वरुप का ध्यान, आत्मभाव में तल्लीन साधुओं का समागम-सेवा और सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति, अनुभव ज्ञान की प्राप्ति, स्व-कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और सर्वत्र औचित्य का पालन, ये हैं आत्मभाव में तल्लीन होने के विविध उपाय । इनका अवलम्बन लेकर मन को समाधिस्थ किया जा सकता है ! अनवरत अभ्यास के कारण समाधि में तन्मयता सिद्ध हो सकती है। फिर भी कभी-कभार मन पर-द्रव्य के प्रति आकर्षित होने की सम्भावना है। ऐसे प्रसंग पर पर-पदार्थों को देखने की विशिष्ट दृष्टि का आधार