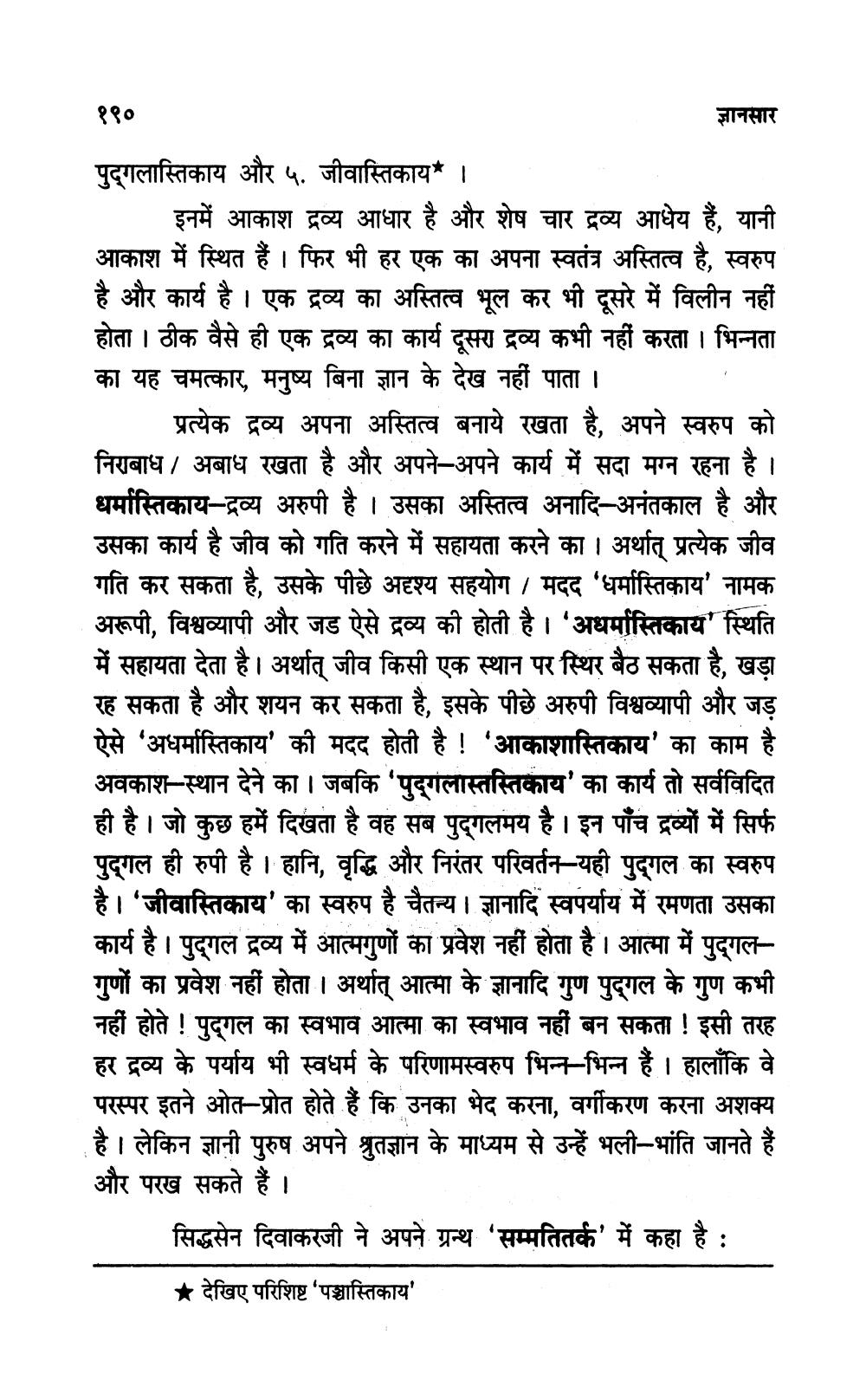________________
ज्ञानसार
१९० पुद्गलास्तिकाय और ५. जीवास्तिकाय* ।
इनमें आकाश द्रव्य आधार है और शेष चार द्रव्य आधेय हैं, यानी आकाश में स्थित हैं। फिर भी हर एक का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वरुप है और कार्य है । एक द्रव्य का अस्तित्व भूल कर भी दूसरे में विलीन नहीं होता । ठीक वैसे ही एक द्रव्य का कार्य दूसरा द्रव्य कभी नहीं करता । भिन्नता का यह चमत्कार, मनुष्य बिना ज्ञान के देख नहीं पाता ।
_प्रत्येक द्रव्य अपना अस्तित्व बनाये रखता है, अपने स्वरुप को निराबाध / अबाध रखता है और अपने-अपने कार्य में सदा मग्न रहना है । धर्मास्तिकाय-द्रव्य अरुपी है । उसका अस्तित्व अनादि-अनंतकाल है और उसका कार्य है जीव को गति करने में सहायता करने का । अर्थात् प्रत्येक जीव गति कर सकता है, उसके पीछे अदृश्य सहयोग / मदद 'धर्मास्तिकाय' नामक अरूपी, विश्वव्यापी और जड ऐसे द्रव्य की होती है। 'अधर्मास्तिकाय' स्थिति में सहायता देता है। अर्थात् जीव किसी एक स्थान पर स्थिर बैठ सकता है, खड़ा रह सकता है और शयन कर सकता है, इसके पीछे अरुपी विश्वव्यापी और जड़ ऐसे 'अधर्मास्तिकाय' की मदद होती है ! 'आकाशास्तिकाय' का काम है अवकाश-स्थान देने का । जबकि 'पुद्गलास्तस्तिकाय' का कार्य तो सर्वविदित ही है। जो कुछ हमें दिखता है वह सब पुद्गलमय है । इन पाँच द्रव्यों में सिर्फ पुद्गल ही रुपी है । हानि, वृद्धि और निरंतर परिवर्तन यही पुद्गल का स्वरुप है। 'जीवास्तिकाय' का स्वरुप है चैतन्य । ज्ञानादि स्वपर्याय में रमणता उसका कार्य है। पुद्गल द्रव्य में आत्मगुणों का प्रवेश नहीं होता है। आत्मा में पुद्गलगुणों का प्रवेश नहीं होता । अर्थात् आत्मा के ज्ञानादि गुण पुद्गल के गुण कभी नहीं होते ! पुद्गल का स्वभाव आत्मा का स्वभाव नहीं बन सकता ! इसी तरह हर द्रव्य के पर्याय भी स्वधर्म के परिणामस्वरुप भिन्न-भिन्न है । हालाँकि वे परस्पर इतने ओत-प्रोत होते हैं कि उनका भेद करना, वर्गीकरण करना अशक्य है। लेकिन ज्ञानी पुरुष अपने श्रुतज्ञान के माध्यम से उन्हें भली-भांति जानते हैं और परख सकते हैं।
सिद्धसेन दिवाकरजी ने अपने ग्रन्थ 'सम्मतितर्क' में कहा है : ★ देखिए परिशिष्ट 'पञ्चास्तिकाय'