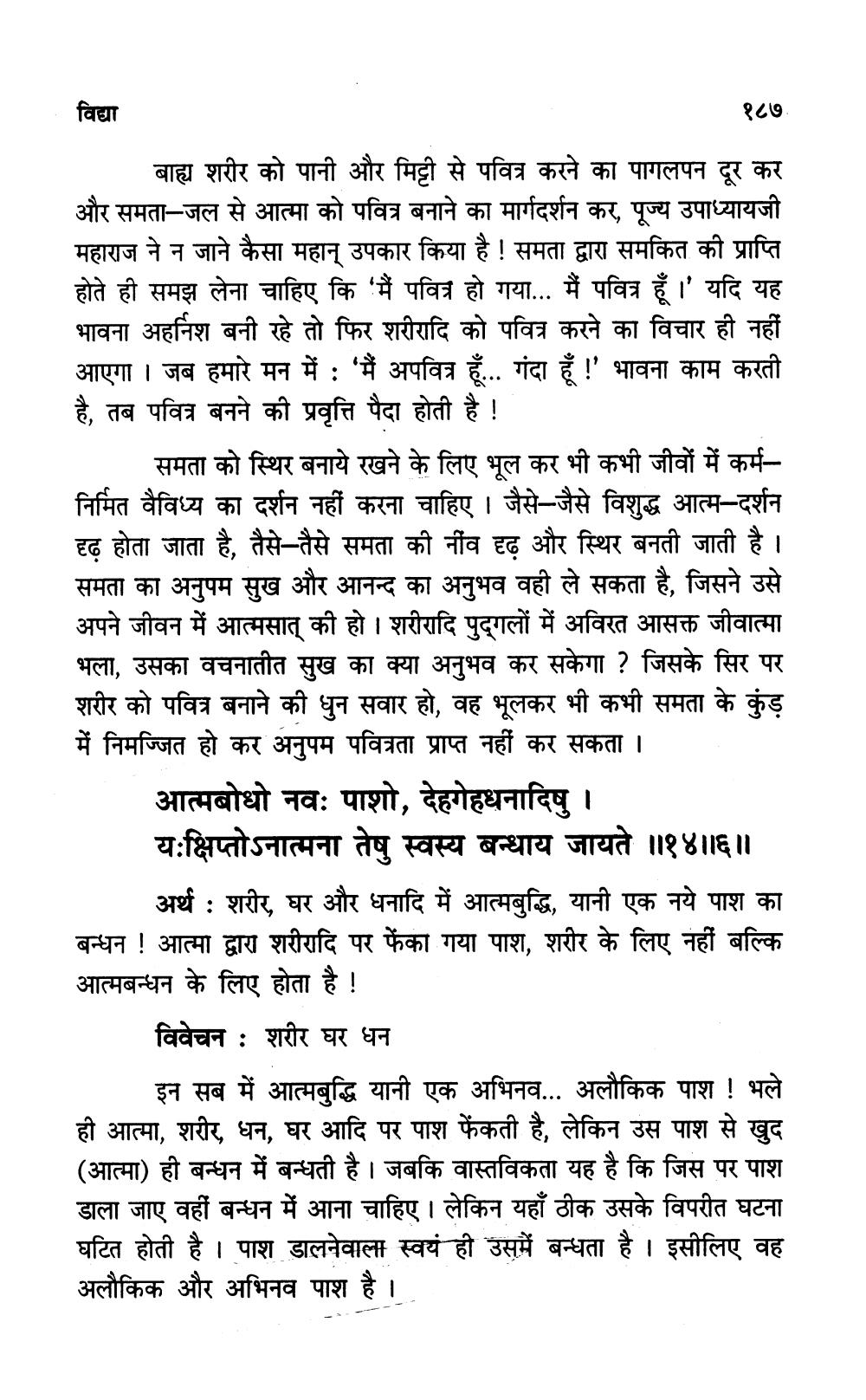________________
विद्या
१८७
बाह्य शरीर को पानी और मिट्टी से पवित्र करने का पागलपन दूर कर और समता-जल से आत्मा को पवित्र बनाने का मार्गदर्शन कर, पूज्य उपाध्यायजी महाराज ने न जाने कैसा महान् उपकार किया है ! समता द्वारा समकित की प्राप्ति होते ही समझ लेना चाहिए कि 'मैं पवित्र हो गया... मैं पवित्र हूँ ।' यदि यह भावना अहर्निश बनी रहे तो फिर शरीरादि को पवित्र करने का विचार ही नहीं आएगा । जब हमारे मन में : 'मैं अपवित्र हूँ... गंदा हूँ !' भावना काम करती है, तब पवित्र बनने की प्रवृत्ति पैदा होती है !
समता को स्थिर बनाये रखने के लिए भूल कर भी कभी जीवों में कर्मनिर्मित वैविध्य का दर्शन नहीं करना चाहिए । जैसे-जैसे विशुद्ध आत्म-दर्शन दृढ होता जाता है, तैसे-तैसे समता की नींव दृढ और स्थिर बनती जाती है। समता का अनुपम सुख और आनन्द का अनुभव वही ले सकता है, जिसने उसे अपने जीवन में आत्मसात् की हो । शरीरादि पुदगलों में अविरत आसक्त जीवात्मा भला, उसका वचनातीत सुख का क्या अनुभव कर सकेगा ? जिसके सिर पर शरीर को पवित्र बनाने की धुन सवार हो, वह भूलकर भी कभी समता के कुंड़ में निमज्जित हो कर अनुपम पवित्रता प्राप्त नहीं कर सकता ।
आत्मबोधो नवः पाशो, देहगेहधनादिषु । यःक्षिप्तोऽनात्मना तेषु स्वस्य बन्धाय जायते ॥१४॥६॥
अर्थ : शरीर, घर और धनादि में आत्मबुद्धि, यानी एक नये पाश का बन्धन ! आत्मा द्वारा शरीरादि पर फेंका गया पाश, शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मबन्धन के लिए होता है !
विवेचन : शरीर घर धन
इन सब में आत्मबुद्धि यानी एक अभिनव... अलौकिक पाश ! भले ही आत्मा, शरीर, धन, घर आदि पर पाश फेंकती है, लेकिन उस पाश से खद (आत्मा) ही बन्धन में बन्धती है। जबकि वास्तविकता यह है कि जिस पर पाश डाला जाए वहीं बन्धन में आना चाहिए । लेकिन यहाँ ठीक उसके विपरीत घटना घटित होती है । पाश डालनेवाला स्वयं ही उसमें बन्धता है । इसीलिए वह अलौकिक और अभिनव पाश है।