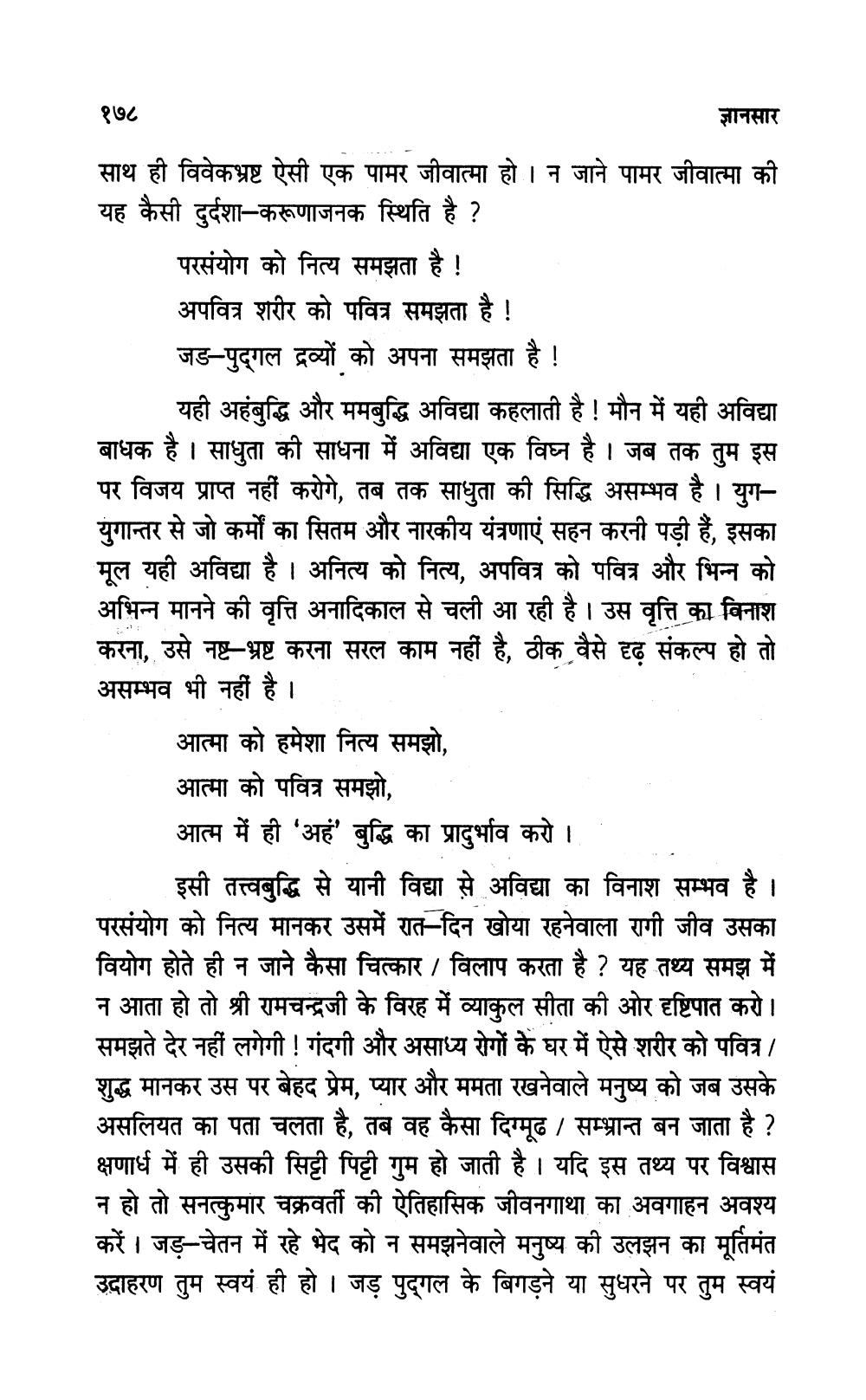________________
१७८
ज्ञानसार
साथ ही विवेकभ्रष्ट ऐसी एक पामर जीवात्मा हो । न जाने पामर जीवात्मा की यह कैसी दुर्दशा – करूणाजनक स्थिति है ?
परसंयोग को नित्य समझता है !
अपवित्र शरीर को पवित्र समझता है !
जड- पुद्गल द्रव्यों को अपना समझता है !
यही अहंबुद्धि और ममबुद्धि अविद्या कहलाती है ! मौन में यही अविद्या बाधक है । साधुता की साधना में अविद्या एक विघ्न है । जब तक तुम इस पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, तब तक साधुता की सिद्धि असम्भव है । युगयुगान्तर से जो कर्मों का सितम और नारकीय यंत्रणाएं सहन करनी पड़ी हैं, इसका मूल यही अविद्या है । अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र और भिन्न को अभिन्न मानने की वृत्ति अनादिकाल से चली आ रही है । उस वृत्ति का विनाश करना, उसे नष्ट-भ्रष्ट करना सरल काम नहीं है, ठीक वैसे दृढ़ संकल्प हो तो असम्भव भी नहीं है ।
आत्मा को हमेशा नित्य समझो,
आत्मा को पवित्र समझो,
आत्म में ही 'अहं' बुद्धि का प्रादुर्भाव करो ।
इसी तत्त्वबुद्धि से यानी विद्या से अविद्या का विनाश सम्भव है । परसंयोग को नित्य मानकर उसमें रात-दिन खोया रहनेवाला रागी जीव उसका वियोग होते ही न जाने कैसा चित्कार / विलाप करता है ? यह तथ्य समझ में न आता हो तो श्री रामचन्द्रजी के विरह में व्याकुल सीता की ओर दृष्टिपात करो । समझते देर नहीं लगेगी ! गंदगी और असाध्य रोगों के घर में ऐसे शरीर को पवित्र / शुद्ध मानकर उस पर बेहद प्रेम, प्यार और ममता रखनेवाले मनुष्य को जब उसके असलियत का पता चलता है, तब वह कैसा दिग्मूढ / सम्भ्रान्त बन जाता है ? क्षणार्ध में ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है । यदि इस तथ्य पर विश्वास न हो तो सनत्कुमार चक्रवर्ती की ऐतिहासिक जीवनगाथा का अवगाहन अवश्य करें | जड़-चेतन में रहे भेद को न समझनेवाले मनुष्य की उलझन का मूर्तिमंत उदाहरण तुम स्वयं ही हो । जड़ पुद्गल के बिगड़ने या सुधरने पर तुम स्वयं
1