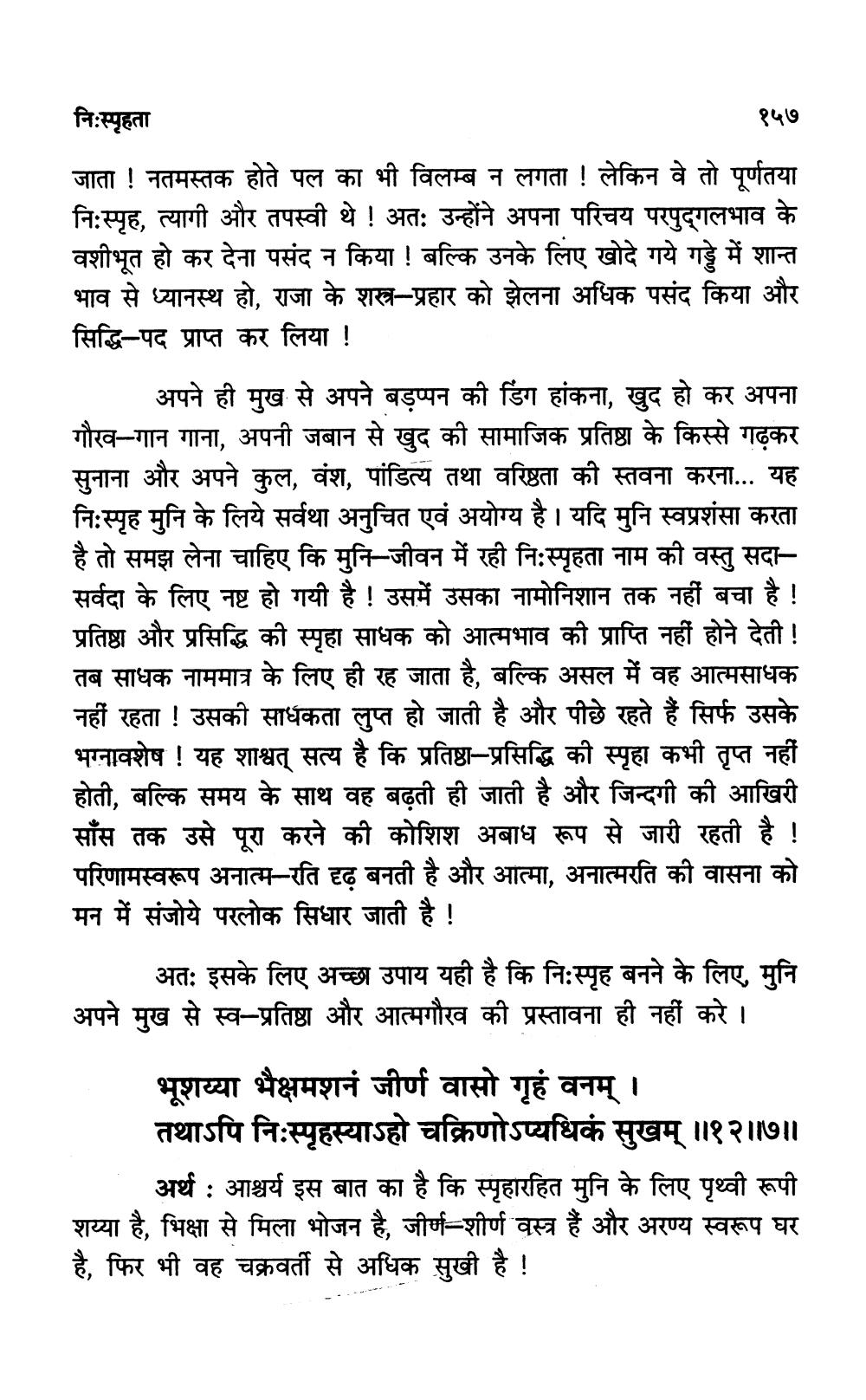________________
निःस्पृहता
१५७
जाता ! नतमस्तक होते पल का भी विलम्ब न लगता ! लेकिन वे तो पूर्णतया नि:स्पृह, त्यागी और तपस्वी थे ! अत: उन्होंने अपना परिचय परपुद्गलभाव के वशीभूत हो कर देना पसंद न किया ! बल्कि उनके लिए खोदे गये गड्डे में शान्त भाव से ध्यानस्थ हो, राजा के शस्त्र प्रहार को झेलना अधिक पसंद किया और सिद्धि-पद प्राप्त कर लिया !
अपने ही मुख से अपने बड़प्पन की डिंग हांकना, खुद हो कर अपना गौरव-गान गाना, अपनी जबान से खुद की सामाजिक प्रतिष्ठा के किस्से गढ़कर सुनाना और अपने कुल, वंश, पांडित्य तथा वरिष्ठता की स्तवना करना... यह निःस्पृह मुनि के लिये सर्वथा अनुचित एवं अयोग्य है । यदि मुनि स्वप्रशंसा करता है तो समझ लेना चाहिए कि मुनि-जीवन में रही निःस्पृहता नाम की वस्तु सदासर्वदा के लिए नष्ट हो गयी है ! उसमें उसका नामोनिशान तक नहीं बचा है ! प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की स्पृहा साधक को आत्मभाव की प्राप्ति नहीं होने देती ! तब साधक नाममात्र के लिए ही रह जाता है, बल्कि असल में वह आत्मसाधक नहीं रहता ! उसकी साधकता लुप्त हो जाती है और पीछे रहते हैं सिर्फ उसके भग्नावशेष ! यह शाश्वत् सत्य है कि प्रतिष्ठा-प्रसिद्धि की स्पृहा कभी तृप्त नहीं होती, बल्कि समय के साथ वह बढ़ती ही जाती है और जिन्दगी की आखिरी साँस तक उसे पूरा करने की कोशिश अबाध रूप से जारी रहती है ! परिणामस्वरूप अनात्म-रति दृढ़ बनती है और आत्मा, अनात्मरति की वासना को मन में संजोये परलोक सिधार जाती है !
___ अतः इसके लिए अच्छा उपाय यही है कि नि:स्पृह बनने के लिए, मुनि अपने मुख से स्व-प्रतिष्ठा और आत्मगौरव की प्रस्तावना ही नहीं करे ।
भूशय्या भैक्षमशनं जीर्ण वासो गृहं वनम् । तथाऽपि निःस्पृहस्याऽहो चक्रिणोऽप्यधिकं सुखम् ॥१२॥७॥
अर्थ : आश्चर्य इस बात का है कि स्पृहारहित मुनि के लिए पृथ्वी रूपी शय्या है, भिक्षा से मिला भोजन है, जीर्ण-शीर्ण वस्त्र हैं और अरण्य स्वरूप घर है, फिर भी वह चक्रवर्ती से अधिक सुखी है !