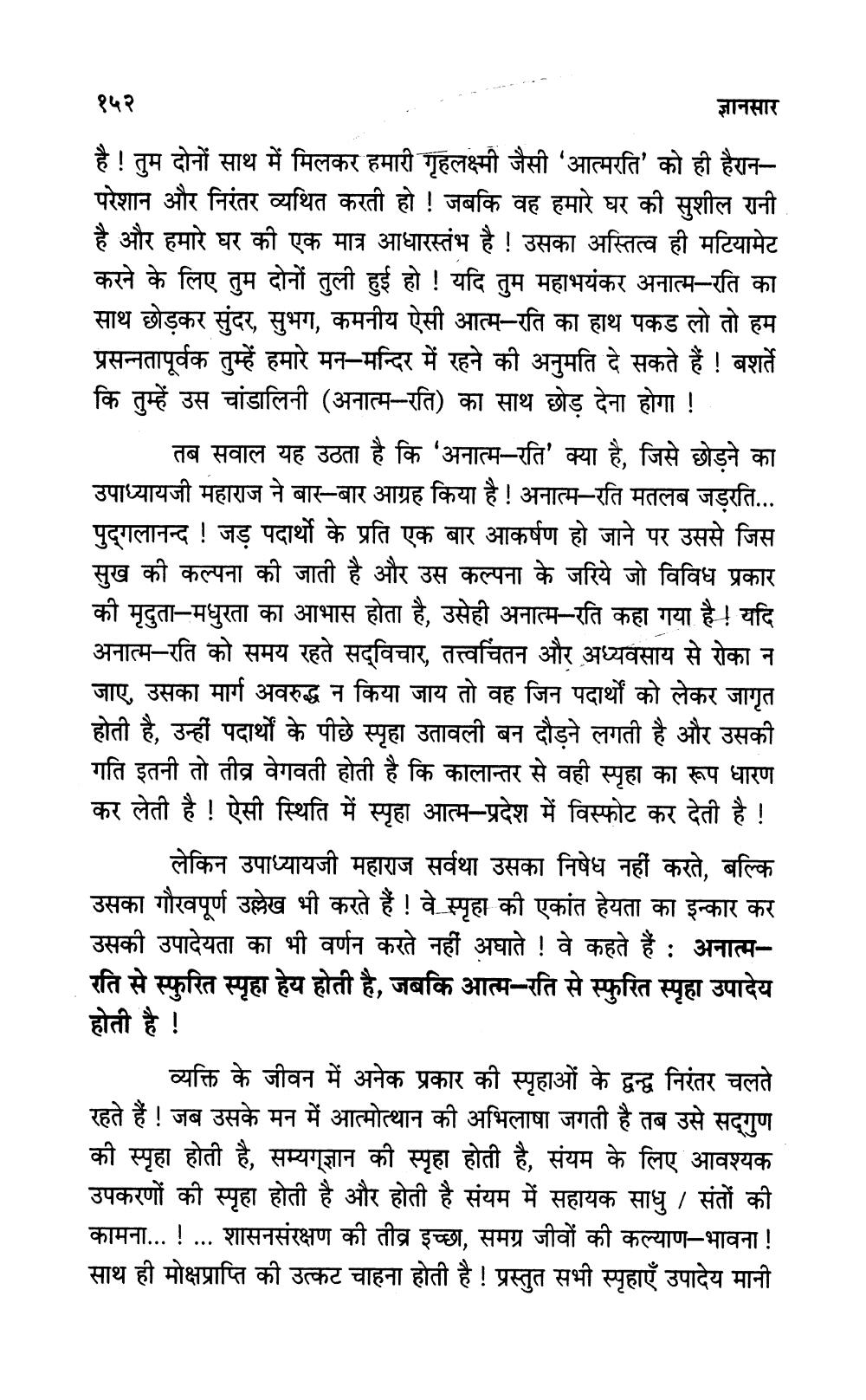________________
ज्ञानसार
१५२ है ! तुम दोनों साथ में मिलकर हमारी गृहलक्ष्मी जैसी 'आत्मरति' को ही हैरानपरेशान और निरंतर व्यथित करती हो ! जबकि वह हमारे घर की सुशील रानी है और हमारे घर की एक मात्र आधारस्तंभ है ! उसका अस्तित्व ही मटियामेट करने के लिए तुम दोनों तुली हुई हो ! यदि तुम महाभयंकर अनात्म–रति का साथ छोड़कर सुंदर, सुभग, कमनीय ऐसी आत्म-रति का हाथ पकड लो तो हम प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें हमारे मन-मन्दिर में रहने की अनुमति दे सकते हैं ! बशर्ते कि तुम्हें उस चांडालिनी (अनात्म-रति) का साथ छोड़ देना होगा !
तब सवाल यह उठता है कि 'अनात्म-रति' क्या है, जिसे छोड़ने का उपाध्यायजी महाराज ने बार-बार आग्रह किया है ! अनात्म–रति मतलब जड़रति... पुद्गलानन्द ! जड़ पदार्थो के प्रति एक बार आकर्षण हो जाने पर उससे जिस सुख की कल्पना की जाती है और उस कल्पना के जरिये जो विविध प्रकार की मृदुता-मधुरता का आभास होता है, उसेही अनात्म-रति कहा गया है। यदि अनात्म-रति को समय रहते सद्विचार, तत्त्वचिंतन और अध्यवसाय से रोका न जाए, उसका मार्ग अवरुद्ध न किया जाय तो वह जिन पदार्थों को लेकर जागृत होती है, उन्हीं पदार्थों के पीछे स्पृहा उतावली बन दौड़ने लगती है और उसकी गति इतनी तो तीव्र वेगवती होती है कि कालान्तर से वही स्पृहा का रूप धारण कर लेती है ! ऐसी स्थिति में स्पृहा आत्म-प्रदेश में विस्फोट कर देती है !
लेकिन उपाध्यायजी महाराज सर्वथा उसका निषेध नहीं करते, बल्कि उसका गौरवपूर्ण उल्लेख भी करते हैं ! वे स्पृहा की एकांत हेयता का इन्कार कर उसकी उपादेयता का भी वर्णन करते नहीं अघाते ! वे कहते हैं : अनात्मरति से स्फुरित स्पृहा हेय होती है, जबकि आत्म-रति से स्फुरित स्पृहा उपादेय होती है !
व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की स्पृहाओं के द्वन्द्व निरंतर चलते रहते हैं ! जब उसके मन में आत्मोत्थान की अभिलाषा जगती है तब उसे सद्गुण की स्पृहा होती है, सम्यगज्ञान की स्पृहा होती है, संयम के लिए आवश्यक उपकरणों की स्पृहा होती है और होती है संयम में सहायक साधु / संतों की कामना... ! ... शासनसंरक्षण की तीव्र इच्छा, समग्र जीवों की कल्याण-भावना ! साथ ही मोक्षप्राप्ति की उत्कट चाहना होती है ! प्रस्तुत सभी स्पृहाएँ उपादेय मानी