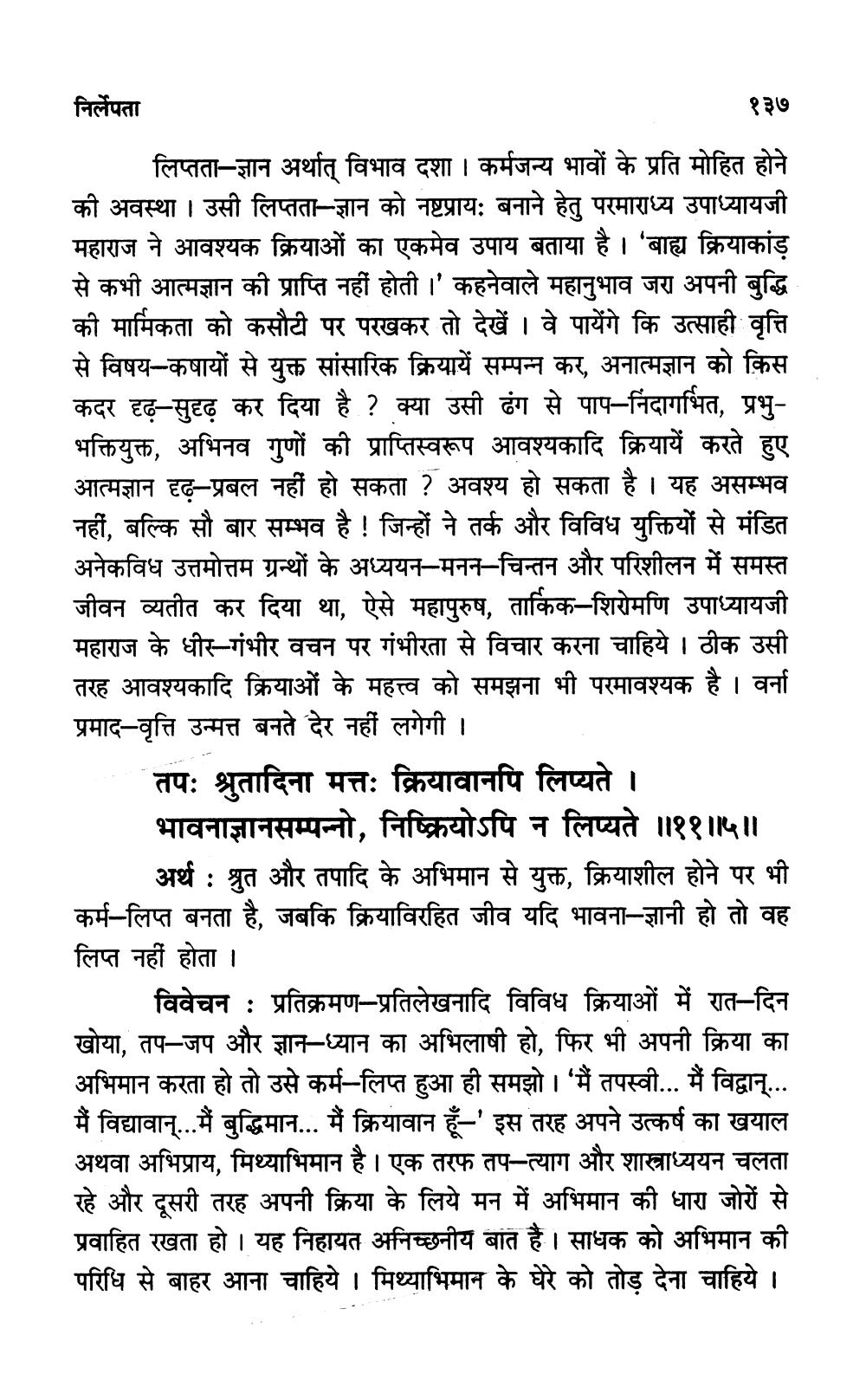________________
निर्लेपता
१३७
लिप्तता-ज्ञान अर्थात् विभाव दशा । कर्मजन्य भावों के प्रति मोहित होने की अवस्था । उसी लिप्तता-ज्ञान को नष्टप्रायः बनाने हेतु परमाराध्य उपाध्यायजी महाराज ने आवश्यक क्रियाओं का एकमेव उपाय बताया है। 'बाह्य क्रियाकांड से कभी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती।' कहनेवाले महानुभाव जरा अपनी बुद्धि की मार्मिकता को कसौटी पर परखकर तो देखें । वे पायेंगे कि उत्साही वृत्ति से विषय-कषायों से युक्त सांसारिक क्रियायें सम्पन्न कर, अनात्मज्ञान को किस कदर दृढ़-सुदृढ़ कर दिया है ? क्या उसी ढंग से पाप-निंदागर्भित, प्रभुभक्तियुक्त, अभिनव गुणों की प्राप्तिस्वरूप आवश्यकादि क्रियायें करते हुए आत्मज्ञान दृढ़-प्रबल नहीं हो सकता ? अवश्य हो सकता है । यह असम्भव नहीं, बल्कि सौ बार सम्भव है ! जिन्हों ने तर्क और विविध युक्तियों से मंडित अनेकविध उत्तमोत्तम ग्रन्थों के अध्ययन-मनन-चिन्तन और परिशीलन में समस्त जीवन व्यतीत कर दिया था, ऐसे महापुरुष, तार्किक-शिरोमणि उपाध्यायजी महाराज के धीर-गंभीर वचन पर गंभीरता से विचार करना चाहिये । ठीक उसी तरह आवश्यकादि क्रियाओं के महत्त्व को समझना भी परमावश्यक है । वर्ना प्रमाद-वृत्ति उन्मत्त बनते देर नहीं लगेगी ।
तपः श्रुतादिना मत्तः क्रियावानपि लिप्यते । भावनाज्ञानसम्पन्नो, निष्क्रियोऽपि न लिप्यते ॥११॥५॥
अर्थ : श्रुत और तपादि के अभिमान से युक्त, क्रियाशील होने पर भी कर्म-लिप्त बनता है, जबकि क्रियाविरहित जीव यदि भावना-ज्ञानी हो तो वह लिप्त नहीं होता।
विवेचन : प्रतिक्रमण-प्रतिलेखनादि विविध क्रियाओं में रात-दिन खोया, तप-जप और ज्ञान-ध्यान का अभिलाषी हो, फिर भी अपनी क्रिया का अभिमान करता हो तो उसे कर्म-लिप्त हुआ ही समझो। 'मैं तपस्वी... मैं विद्वान्... मैं विद्यावान्...मैं बुद्धिमान... मैं क्रियावान हूँ-' इस तरह अपने उत्कर्ष का खयाल अथवा अभिप्राय, मिथ्याभिमान है। एक तरफ तप-त्याग और शास्त्राध्ययन चलता रहे और दूसरी तरह अपनी क्रिया के लिये मन में अभिमान की धारा जोरों से प्रवाहित रखता हो । यह निहायत अनिच्छनीय बात है। साधक को अभिमान की परिधि से बाहर आना चाहिये । मिथ्याभिमान के घेरे को तोड़ देना चाहिये ।