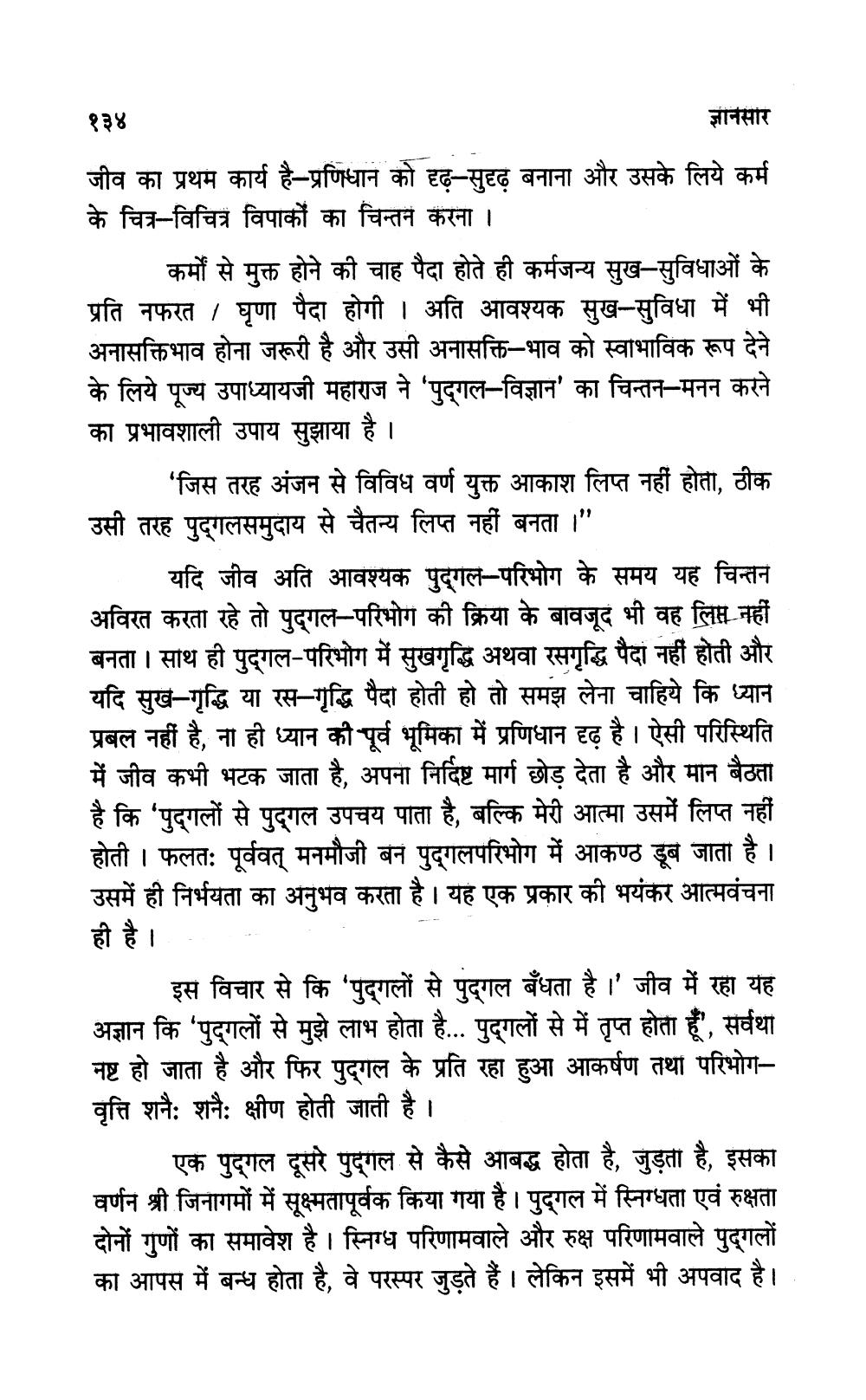________________
ज्ञानसार
जीव का प्रथम कार्य है-प्रणिधान को दृढ़-सुदृढ़ बनाना और उसके लिये कर्म के चित्र-विचित्र विपाकों का चिन्तन करना ।
कर्मों से मुक्त होने की चाह पैदा होते ही कर्मजन्य सुख-सुविधाओं के प्रति नफरत । घृणा पैदा होगी । अति आवश्यक सुख-सुविधा में भी अनासक्तिभाव होना जरूरी है और उसी अनासक्ति-भाव को स्वाभाविक रूप देने के लिये पूज्य उपाध्यायजी महाराज ने 'पुद्गल-विज्ञान' का चिन्तन-मनन करने का प्रभावशाली उपाय सुझाया है।
"जिस तरह अंजन से विविध वर्ण युक्त आकाश लिप्त नहीं होता, ठीक उसी तरह पुद्गलसमुदाय से चैतन्य लिप्त नहीं बनता ।"
__ यदि जीव अति आवश्यक पुद्गल-परिभोग के समय यह चिन्तन अविरत करता रहे तो पुद्गल-परिभोग की क्रिया के बावजूद भी वह लिप्त नहीं बनता । साथ ही पुद्गल-परिभोग में सुखगृद्धि अथवा रसगृद्धि पैदा नहीं होती और यदि सुख-गृद्धि या रस-गृद्धि पैदा होती हो तो समझ लेना चाहिये कि ध्यान प्रबल नहीं है, ना ही ध्यान की पूर्व भूमिका में प्रणिधान दृढ़ है । ऐसी परिस्थिति में जीव कभी भटक जाता है, अपना निर्दिष्ट मार्ग छोड़ देता है और मान बैठता है कि 'पुद्गलों से पुद्गल उपचय पाता है, बल्कि मेरी आत्मा उसमें लिप्त नहीं होती । फलत: पूर्ववत् मनमौजी बन पुद्गलपरिभोग में आकण्ठ डूब जाता है । उसमें ही निर्भयता का अनुभव करता है। यह एक प्रकार की भयंकर आत्मवंचना ही है।
इस विचार से कि 'पुद्गलों से पुद्गल बँधता है ।' जीव में रहा यह अज्ञान कि 'पुद्गलों से मुझे लाभ होता है... पुद्गलों से में तृप्त होता हूँ', सर्वथा नष्ट हो जाता है और फिर पुद्गल के प्रति रहा हुआ आकर्षण तथा परिभोगवृत्ति शनैः शनैः क्षीण होती जाती है।
एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से कैसे आबद्ध होता है, जुड़ता है, इसका वर्णन श्री जिनागमों में सूक्ष्मतापूर्वक किया गया है। पुद्गल में स्निग्धता एवं रुक्षता दोनों गुणों का समावेश है । स्निग्ध परिणामवाले और रुक्ष परिणामवाले पुद्गलों का आपस में बन्ध होता है, वे परस्पर जुड़ते हैं । लेकिन इसमें भी अपवाद है।