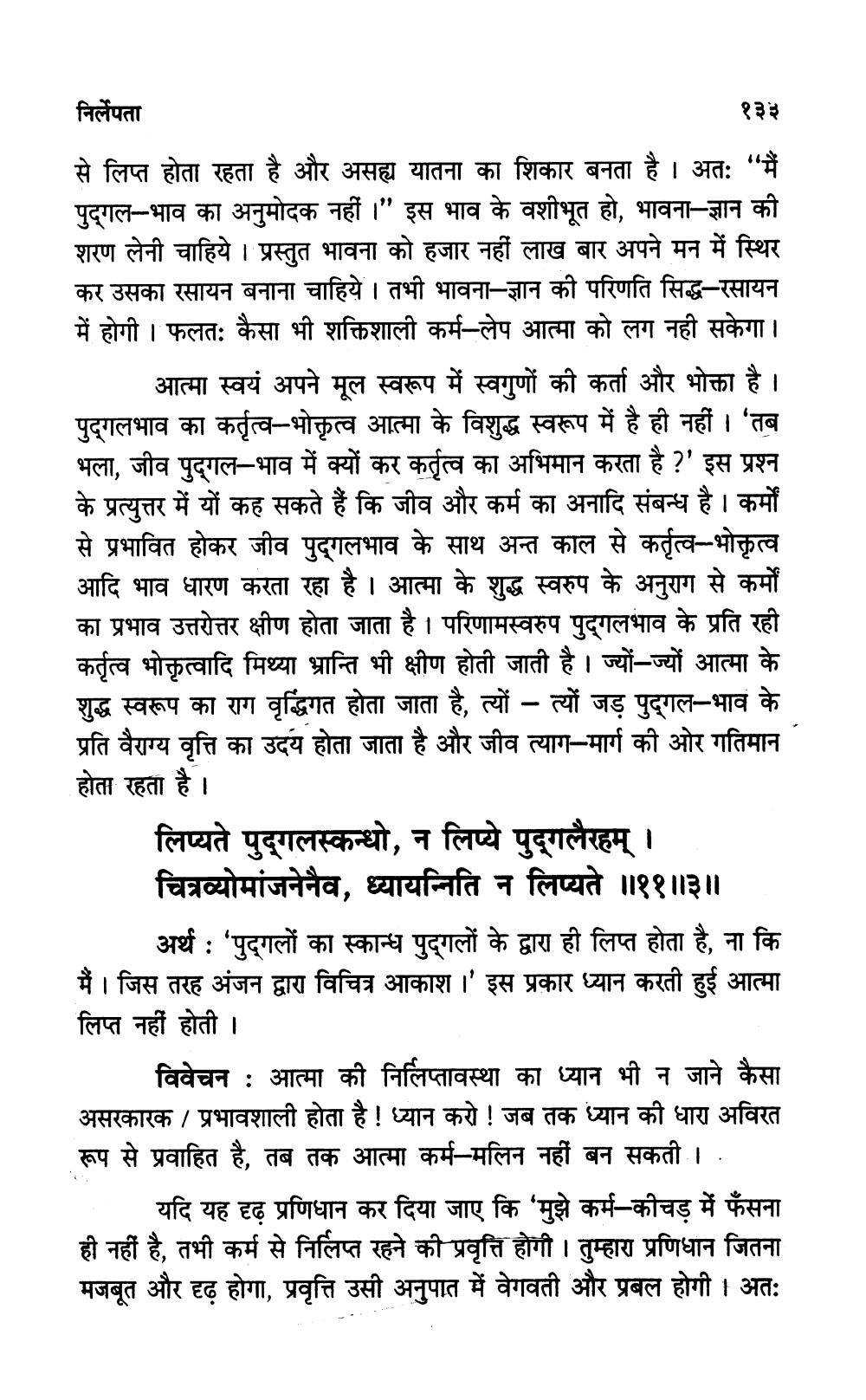________________
निर्लेपता
१३३
से लिप्त होता रहता है और असह्य यातना का शिकार बनता है । अतः "मैं पुद्गल-भाव का अनुमोदक नहीं ।" इस भाव के वशीभूत हो, भावना - ज्ञान की शरण लेनी चाहिये । प्रस्तुत भावना को हजार नहीं लाख बार अपने मन में स्थिर कर उसका रसायन बनाना चाहिये। तभी भावना - ज्ञान की परिणति सिद्ध-रसायन में होगी । फलतः कैसा भी शक्तिशाली कर्म - लेप आत्मा को लग नही सकेगा ।
आत्मा स्वयं अपने मूल स्वरूप में स्वगुणों की कर्ता और भोक्ता है । पुद्गलभाव का कर्तृत्व- भोक्तृत्व आत्मा के विशुद्ध स्वरूप में है ही नहीं । 'तब भला, जीव पुद्गल-भाव में क्यों कर कर्तृत्व का अभिमान करता है ?' इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में यों कह सकते हैं कि जीव और कर्म का अनादि संबन्ध है । कर्मों से प्रभावित होकर जीव पुद्गलभाव के साथ अन्त काल से कर्तृत्व - भोक्तृत्व आदि भाव धारण करता रहा है । आत्मा के शुद्ध स्वरुप के अनुराग से कर्मों का प्रभाव उत्तरोत्तर क्षीण होता जाता है । परिणामस्वरुप पुद्गलभाव के प्रति रही कर्तृत्व भोक्तृत्वादि मिथ्या भ्रान्ति भी क्षीण होती जाती है । ज्यों-ज्यों आत्मा के शुद्ध स्वरूप का राग वृद्धिंगत होता जाता है, त्यों-त्यों जड़ पुद्गल - भाव के प्रति वैराग्य वृत्ति का उदय होता जाता है और जीव त्याग - मार्ग की ओर गतिमान होता रहता है ।
1
लिप्यते पुद्गलस्कन्धो, न लिप्ये पुद्गलैरहम् । चित्रव्योमांजनेनैव ध्यायन्निति न लिप्यते ॥ ११ ॥३॥
अर्थ : 'पुद्गलों का स्कान्ध पुद्गलों के द्वारा ही लिप्त होता है, ना कि मैं । जिस तरह अंजन द्वारा विचित्र आकाश ।' इस प्रकार ध्यान करती हुई आत्मा लिप्त नहीं होती ।
1
विवेचन : आत्मा की निर्लिप्तावस्था का ध्यान भी न जाने कैसा असरकारक / प्रभावशाली होता है ! ध्यान करो ! जब तक ध्यान की धारा अविरत रूप से प्रवाहित है, तब तक आत्मा कर्म - मलिन नहीं बन सकती ।
यदि यह दृढ़ प्रणिधान कर दिया जाए कि 'मुझे कर्म-कीचड़ में फँसना ही नहीं है, तभी कर्म से निर्लिप्त रहने की प्रवृत्ति होगी । तुम्हारा प्रणिधान जितना मजबूत और दृढ़ होगा, प्रवृत्ति उसी अनुपात में वेगवती और प्रबल होगी । अतः