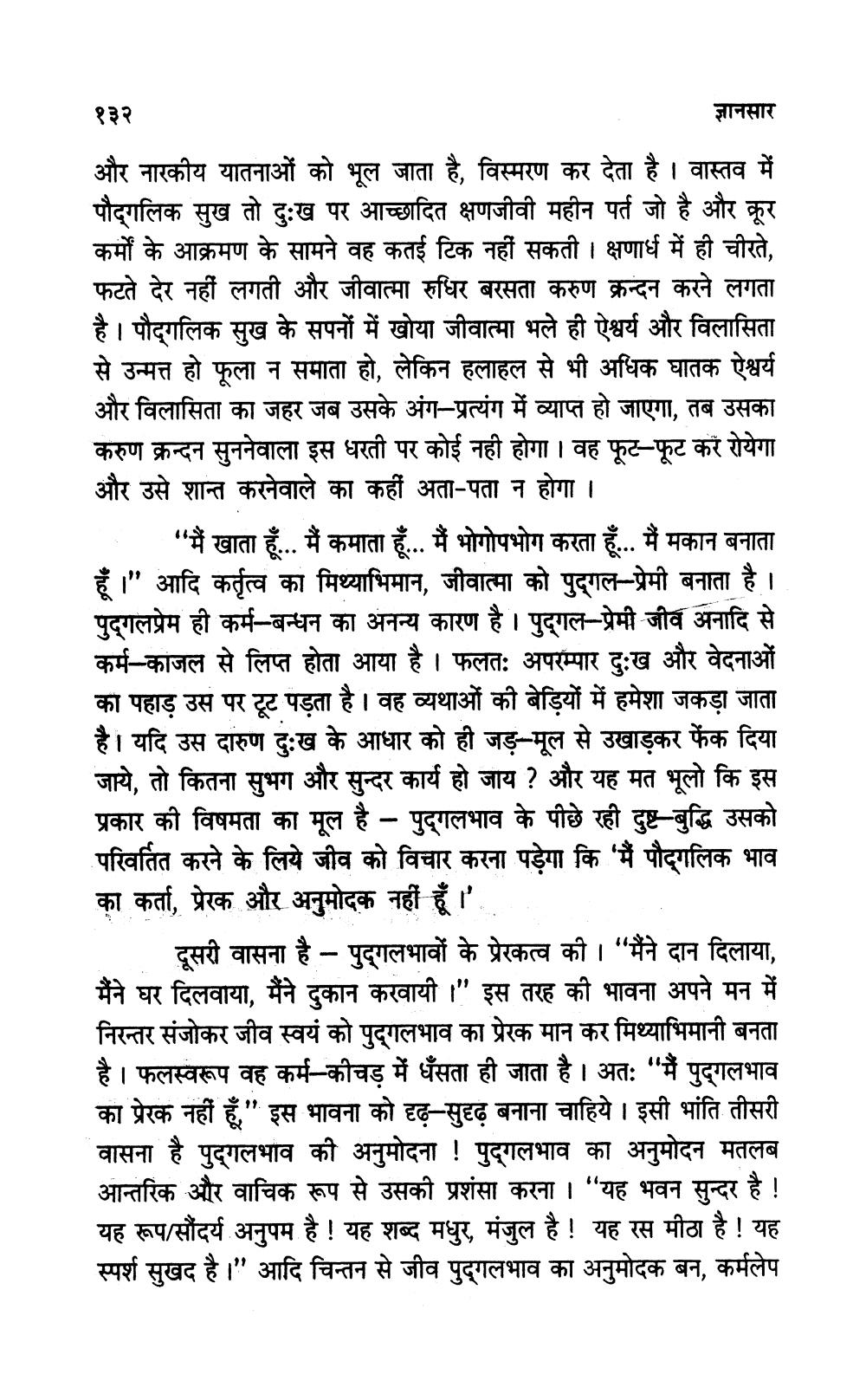________________
१३२
ज्ञानसार
और नारकीय यातनाओं को भूल जाता है, विस्मरण कर देता है । वास्तव में पौद्गलिक सुख तो दुःख पर आच्छादित क्षणजीवी महीन पर्त जो है और क्रूर कर्मों के आक्रमण के सामने वह कतई टिक नहीं सकती । क्षणार्ध में ही चीरते, फटते देर नहीं लगती और जीवात्मा रुधिर बरसता करुण क्रन्दन करने लगता है। पौद्गलिक सुख के सपनों में खोया जीवात्मा भले ही ऐश्वर्य और विलासिता से उन्मत्त हो फूला न समाता हो, लेकिन हलाहल से भी अधिक घातक ऐश्वर्य
और विलासिता का जहर जब उसके अंग-प्रत्यंग में व्याप्त हो जाएगा, तब उसका करुण क्रन्दन सुननेवाला इस धरती पर कोई नही होगा। वह फूट-फूट कर रोयेगा और उसे शान्त करनेवाले का कहीं अता-पता न होगा ।
"मैं खाता हूँ... मैं कमाता हूँ... मैं भोगोपभोग करता हूँ... मैं मकान बनाता हूँ ।" आदि कर्तृत्व का मिथ्याभिमान, जीवात्मा को पुद्गल-प्रेमी बनाता है । पुद्गलप्रेम ही कर्म-बन्धन का अनन्य कारण है। पुद्गल-प्रेमी जीव अनादि से कर्म-काजल से लिप्त होता आया है । फलतः अपरम्पार दु:ख और वेदनाओं का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है। वह व्यथाओं की बेड़ियों में हमेशा जकड़ा जाता है। यदि उस दारुण दु:ख के आधार को ही जड़-मूल से उखाड़कर फेंक दिया जाये, तो कितना सुभग और सुन्दर कार्य हो जाय ? और यह मत भूलो कि इस प्रकार की विषमता का मूल है - पुद्गलभाव के पीछे रही दुष्ट-बुद्धि उसको परिवर्तित करने के लिये जीव को विचार करना पड़ेगा कि 'मैं पौद्गलिक भाव का कर्ता, प्रेरक और अनुमोदक नहीं हूँ।'...
दूसरी वासना है - पुद्गलभावों के प्रेरकत्व की । “मैंने दान दिलाया, मैंने घर दिलवाया, मैंने दुकान करवायी।" इस तरह की भावना अपने मन में निरन्तर संजोकर जीव स्वयं को पुद्गलभाव का प्रेरक मान कर मिथ्याभिमानी बनता है । फलस्वरूप वह कर्म-कीचड़ में फँसता ही जाता है। अत: "मैं पुद्गलभाव का प्रेरक नहीं हूँ," इस भावना को दृढ़-सुदृढ़ बनाना चाहिये । इसी भांति तीसरी वासना है पुद्गलभाव की अनुमोदना ! पुद्गलभाव का अनुमोदन मतलब आन्तरिक और वाचिक रूप से उसकी प्रशंसा करना । "यह भवन सुन्दर है ! यह रूप/सौंदर्य अनुपम है ! यह शब्द मधुर, मंजुल है ! यह रस मीठा है ! यह स्पर्श सुखद है।" आदि चिन्तन से जीव पुद्गलभाव का अनुमोदक बन, कर्मलेप